CBSE 12th Term-2 Exam 2022 : Hindi Important Questions with Solution
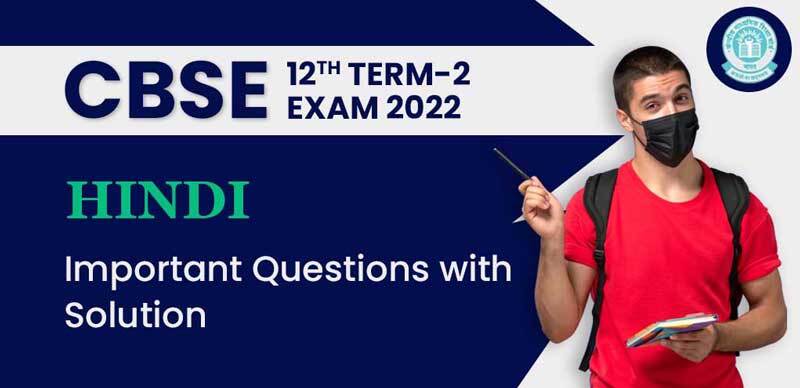
SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
CBSE 12th Term-2 Exam 2022 : Hindi Important Questions with Solution
The Central Board of Secondary Education is all set to conduct CBSE Term 2 exam for Hindi on the 2nd of May 2022, Friday. As the exam date is approaching the candidates must solve all the CBSE Class 12 Term 2 Hindi Important Questions given on this page to get good marks in Hindi. We have also given the answers to the CBSE Class 12 Term 2 Hindi Important Questions so students can learn answer writing to fetch maximum marks in the Term 2 Examination.
कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन
फ़ीचर लेखन
प्रश्नः 1. फ़ीचर की आवश्यकता क्यों होती है?
उत्तरः
फ़ीचर पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा है। भले ही समाचार पत्रों में समाचार की प्रमुखता अधिक होती है लेकिन एक समाचार-पत्र की प्रसिद्धि और उत्कृष्टता का आधार समाचार नहीं होता बल्कि उसमें प्रकाशित ऐसी सामग्री से होता है जिसका संबंध न केवल जीवन की परिस्थितियों और परिवेश से संबंधित होता है प्रत्युत् वह जीवन की विवेचना भी करती है। समाचारों के अतिरिक्त समाचार-पत्रों में मुख्य रूप से जीवन की नैतिक व्याख्या के लिए ‘संपादकीय’ एवं जीवनगत् यथार्थ की भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए ‘फ़ीचर’ लेखों की उपयोगिता असंदिग्ध है।
समाचार एवं संपादकीय में सूचनाओं को सम्प्रेषित करते समय उसमें घटना विशेष का विचार बिंदु चिंतन के केंद्र में रहता है लेकिन समाचार-पत्रों की प्रतिष्ठा और उसे पाठकों की ओर आकर्षित करने के लिए लिखे गए ‘फ़ीचर’ लेखों में वैचारिक चिंतन के साथ-साथ भावात्मक संवेदना का पुट भी उसमें विद्यमान रहता है। इसी कारण समाचार-पत्रों में उत्कृष्ट फ़ीचर लेखों के लिए विशिष्ट लेखकों तक से इनका लेखन करवाया जाता है। इसलिए किसी भी समाचार-पत्र की लोकप्रियता का मुख्य आधार यही फ़ीचर होते हैं। इनके द्वारा ही पाठकों की रुचि उस समाचार-पत्र की ओर अधिक होती है जिसमें अधिक उत्कृष्ट, रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक फ़ीचर प्रकाशित किए जाते हैं।
‘फ़ीचर’ का स्वरूप कुछ सीमा तक निबंध एवं लेख से निकटता रखता है, लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से इनमें भेद होने के कारण इनमें पर्याप्त भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। जहाँ ‘निबंध एवं लेख’ विचार और चिंतन के कारण अधिक बोझिल और नीरस बन जाते हैं वहीं ‘फ़ीचर’ अपनी सरस भाषा और आकर्षण शैली में पाठकों को इस प्रकार अभिभूत कर देते
हैं कि वे लेखक को अभिप्रेत विचारों को सरलता से समझ पाते हैं।
प्रश्नः 2. फ़ीचर का स्वरूप बताइए।
उत्तरः
‘फ़ीचर’ (Feature) अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैक्ट्रा (Fectura) शब्द से हुई है। विभिन्न
शब्दकोशों के अनुसार इसके लिए अनेक अर्थ हैं, मुख्य रूप से इसके लिए स्वरूप, आकृति, रूपरेखा, लक्षण, व्यक्तित्व आदि अर्थ प्रचलन में हैं। ये अर्थ प्रसंग और संदर्भ के अनुसार ही प्रयोग में आते हैं। अंग्रेज़ी के फ़ीचर शब्द के आधार पर ही हिंदी में भी ‘फ़ीचर’ शब्द को ही स्वीकार लिया गया है। हिंदी के कुछ विद्वान इसके लिए ‘रूपक’ शब्द का प्रयोग भी करते हैं लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्तमान में ‘फ़ीचर’ शब्द ही प्रचलन में है।
विभिन्न विदवानों ने ‘फ़ीचर’ शब्द को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, लेकिन उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। फिर भी कतिपय विद्वानों की परिभाषाओं में कुछ एक शब्दों में फेरबदल कर देने मात्र से सभी किसी-न-किसी सीमा तक एक समान अर्थ की अभिव्यंजना ही करते हैं। विदेशी पत्रकार डेनियल आर० विलियमसन ने अपनी पुस्तक ‘फ़ीचर राइटिंग फॉर न्यूजपेपर्स’ में फ़ीचर शब्द पर प्रकाश डालते हुए अपना मत दिया है कि-“फ़ीचर ऐसा रचनात्मक तथा कुछ-कुछ स्वानुभूतिमूलक लेख है, जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया गया हो।” इसी तरह डॉ० सजीव भानावत का कहना है-“फ़ीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस, मधुर और अनुभूतिपूर्ण वर्णन है।
फ़ीचर लेखक गौण है, वह एक माध्यम है जो फ़ीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा, उत्सुकता और उत्कंठा को शांत करता हुआ समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का आकलन करता है। इस प्रकार फ़ीचर में सामयिक तथ्यों का यथेष्ट समावेश होता ही है, साथ ही अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की संभावनाओं से भी वह जुड़ा रहता है। समय की धड़कनें इसमें गूंजती हैं।” इस विषय पर हिंदी और अन्य भाषाओं के अनेक विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं और मतों को दृष्टिगत रखने के उपरांत कहा जा सकता है कि किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध रूप, जो भावात्मक संवेदना से परिपूर्ण, कल्पनाशीलता से युक्त हो तथा जिसे मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, फ़ीचर कहा जाता है।
‘फ़ीचर’ पाठक की चेतना को नहीं जगाता बल्कि वह उसकी भावनाओं और संवेदनाओं को उत्प्रेरित करता है। यह यथार्थ की वैयक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इसमें लेखक पाठक को अपने अनुभव से समाज के सत्य का भावात्मक रूप में परिचय कराता है। इसमें समाचार दृश्यात्मक रूप में पाठक के सामने उभरकर आ जाता है। यह सूचनाओं को सम्प्रेषित करने का ऐसा साहित्यिक रूप है जो भाव और कल्पना के रस से आप्त होकर पाठक को भी इसमें भिगो देता है।
प्रश्नः 3. फ़ीचर का महत्त्व लिखिए।
उत्तरः
प्रत्येक समाचार-पत्र एवं पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित होने के कारण फ़ीचर की उपयोगिता स्वतः स्पष्ट है। समाचार की तरह यह भी सत्य का साक्षात्कार तो कराता ही है लेकिन साथ ही पाठक को विचारों के जंगल में भी मनोरंजन और औत्सुक्य के रंग बिरंगे फूलों के उपवन का भान भी करा देता है। फ़ीचर समाज के विविध विषयों पर अपनी सटीक टिप्पणियाँ देते हैं। इन टिप्पणियों में लेखक का चिंतन और उसकी सामाजिक उपादेयता प्रमुख होती है।
लेखक फ़ीचर के माध्यम से प्रतिदिन घटने वाली विशिष्ट घटनाओं और सूचनाओं को अपने केंद्र में रखकर उस पर गंभीर चिंतन करता है। उस गंभीर चिंतन की अभिव्यक्ति इस तरह से की जाती है कि पाठक उस सूचना को न केवल प्राप्त कर लेता है बल्कि उसमें केंद्रित समस्या का समाधान खोजने के लिए स्वयं ही बाध्य हो जाता है। फ़ीचर का महत्त्व केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज के सामने अनेक प्रश्न उठाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में अनेक वैचारिक बिंदुओं को भी समाज के सामने रखते हैं।
वर्तमान समय में फ़ीचर की महत्ता इतनी अधिक बढ़ गयी है कि विविध विषयों पर फ़ीचर लिखने के लिए समाचार-पत्र उन विषयों के विशेषज्ञ लेखकों से अपने पत्र के लिए फ़ीचर लिखवाते हैं जिसके लिए वह लेखक को अधिक पारिश्रमिक भी देते हैं। आजकल अनेक विषयों में अपने-अपने क्षेत्र में लेखक क्षेत्र से जुड़े लेखकों की माँग इस क्षेत्र में अधिक है लेकिन इसमें साहित्यिक प्रतिबद्धता के कारण वही फ़ीचर लेखक ही सफलता की ऊँचाईयों को छू सकता है जिसकी संवेदनात्मक अनुभूति की प्रबलता और कल्पना की मुखरता दूसरों की अपेक्षा अधिक हो।
प्रश्नः 4. फ़ीचर कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तरः
फ़ीचर विषय, वर्ग, प्रकाशन, प्रकृति, शैली, माध्यम आदि विविध आधारों पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पत्रकारिता के
क्षेत्र में जीवन के किसी भी क्षेत्र की कोई भी छोटी-से-छोटी घटना आदि समाचार बन जाते हैं। इस क्षेत्र में जितने विषयों के आधार पर समाचार बनते हैं उससे कहीं अधिक विषयों पर फ़ीचर लेखन किया जा सकता है। विषय-वैविध्य के कारण इसे कई भागों-उपभागों में बाँटा जा सकता है। विवेकी राय, डॉ० हरिमोहन, डॉ० पूरनचंद टंडन आदि कतिपय विद्वानों ने फ़ीचर के अनेक रूपों पर प्रकाश डाला है। उनके आधार पर फ़ीचर के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं –
- सामाजिक सांस्कृतिक फ़ीचर – इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधी जीवन के अंतर्गत रीति-रिवाज, पर परंपराओं, त्योहारों, मेलों, कला, खेल-कूद, शैक्षिक, तीर्थ, धर्म संबंधी, सांस्कृतिक विरासतों आदि विषयों को रखा जा सकता है।
- घटनापरक फ़ीचर – इसके अंतर्गत युद्ध, अकाल, दंगे, दुर्घटनायें, बीमारियाँ, आंदोलन आदि से संबंधित विषयों को रखा जा सकता है। प्राकृतिक फ़ीचर-इसके अंतर्गत प्रकृति संबंधी विषयों जैसे पर्वतारोहण, यात्राओं, प्रकृति की विभिन्न छटाओं, पर्यटन स्थलों आदि को रखा जा सकता है।
- राजनीतिक फ़ीचर – इसके अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों, घटनाओं, विचारों, व्यक्तियों आदि से संबंधित विषयों को रखा जा सकता है।
- साहित्यिक फ़ीचर – इसके अंतर्गत साहित्य से संबंधित गतिविधियों, पुस्तकों, साहित्यकारों आदि विषयों को रखा जा सकता है।
- प्रकीर्ण फ़ीचर – जिन विषयों को ऊपर दिए गए किसी भी वर्ग में स्थान नहीं मिला ऐसे विषयों को प्रकीर्ण फ़ीचर के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन उपर्युक्त विषयों के विभाजन और विषय वैविध्य को दृष्टिगत रखा जाए तो फ़ीचर को अधिकांश विद्वानों ने दो भागों में बाँटा है जिसके अंतर्गत उपर्युक्त सभी विषयों का समावेश हो जाता है –
- समाचार फ़ीचर अथवा तात्कालिक फ़ीचर – तात्कालिक घटने वाली किसी घटना पर तैयार किए गए समाचार पर आधारित फ़ीचर को समाचारी या तात्कालिक फ़ीचर कहा जाता है। इसके अंतर्गत तथ्य अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में एक बच्चे के 60 फुट गहरे गड्ढे में गिरने की घटना एक समाचार है लेकिन उस बच्चे द्वारा लगातार 50 घंटे की संघर्ष गाथा का भावात्मक वर्णन उसका समाचारी-फ़ीचर है।
- विशिष्ट फ़ीचर – जहाँ समाचारी फ़ीचर में तत्काल घटने वाली घटनाओं आदि का महत्त्व अधिक होता है वहीं विशिष्टफ़ीचर में घटनाओं को बीते भले ही समय क्यों न हो गया हो लेकिन उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। जैसे प्रकृति की छटाओं या ऋतुओं, ऐतिहासिक स्थलों, महापुरुषों एवं लम्बे समय तक याद रहने वाली घटनाओं आदि पर लिखे गए लेखक किसी भी समय प्रकाशित किए जा सकते हैं। इन विषयों के लिए लेखक विभिन्न प्रयासों से सामग्री का संचयन कर उन पर लेख लिख सकता है। ऐसे फ़ीचर समाचार पत्रों के लिए प्राण-तत्त्व के रूप में होते हैं। इनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है इसलिए बहुत से पाठक इनका संग्रहण भी करते हैं। इस तरह के फ़ीचर किसी दिन या सप्ताह विशेष में अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं; जैसे-दीपावली या होली पर्व पर इन त्यौहारों से संबंधित पौराणिक या ऐतिहासिक संदर्भो को लेकर लिखे फ़ीचर, महात्मा गांधी जयंती या सुभाषचंद्र बोस जयंती पर गांधी जी अथवा सुभाषचंद्र बोस के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालने वाले फ़ीचर आदि।
प्रश्नः 5. फ़ीचर की विशेषताएँ बताइए।
उत्तरः
फ़ीचर लेखन के विविध पक्षों एवं लेखक की रचना-प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालने से पहले फ़ीचर की विशेषताओं के बारे में जान लेना आवश्यक है। अपनी विशेषताओं के कारण ही एक फ़ीचर समाचार, निबंध या लेख जैसी विधाओं से भिन्न अपनी पहचान बनाता है। एक अच्छे फ़ीचर में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए –
सत्यता या तथ्यात्मकता – किसी भी फ़ीचर लेख के लिए सत्यता या तथ्यात्मकता का गुण अनिवार्य है। तथ्यों से रहित किसी अविश्वनीय सूत्र को आधार बनाकर लिखे गए लेख फ़ीचर के अंतर्गत नहीं आते हैं। कल्पना से युक्त होने के बावजूद भी फ़ीचर में विश्वसनीय सूत्रों को लेख का माध्यम बनाया जाता है। यदि वे तथ्य सत्य से परे हैं या उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है तो ऐसे तथ्यों पर फ़ीचर नहीं लिखा जाना चाहिए।
गंभीरता एवं रोचकता–फ़ीचर में भावों और कल्पना के आगमन से उसमें रोचकता तो आ जाती है किंतु ऐसा नहीं कि वह विषय के प्रति गंभीर न हो। समाज की सामान्य जनता के सामने किसी भी सूचना को आधार बनाकर या विषय को लक्ष्य में रखकर फ़ीचर प्रस्तुत किया जाता है तो वह फ़ीचर लेखक विषय-वस्तु को केंद्र में रखकर उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। उसके गंभीर चिंतन के परिणामों को ही फ़ीचर द्वारा रोचक शैली में संप्रेषित किया जाता है।
मौलिकता-सामान्यतः एक ही विषय को आधार बनाकर अनेक लेखक उस पर फ़ीचर लिखते हैं। उनमें से जो फ़ीचर अपनी मौलिक पहचान बना पाने में सफल होता है वही फ़ीचर एक आदर्श फ़ीचर कहलाता है। विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों का संग्रहण और विश्लेषण करते हुए फ़ीचर लेखक की अपनी दृष्टि अधिक महत्त्वपूर्ण होती है लेकिन साथ ही वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से भी उन तथ्यों को परखता है जिससे उसकी प्रामाणिकता अधिक सशक्त हो जाती है। लेखक जितने अधिक तथ्यों को गहनता से विश्लेषित कर उसे अपनी दृष्टि और शैली से अभिव्यक्ति प्रदान करता है उतना ही उसका फ़ीचर लेख मौलिक कहलाता है।
सामाजिक दायित्व बोध-कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती। उसी तरह फ़ीचर भी किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य से युक्त होता है। फ़ीचर का उद्देश्य सामाजिक दायित्व बोध से संबद्ध होना चाहिए क्योंकि फ़ीचर समाज के लिए ही लिखा जाता है इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों पर उसका प्रभाव पड़ना अपेक्षित है। इसलिए फ़ीचर सामाजिक जीवन के जितना अधिक निकट होगा और सामाजिक जीवन की विविधता को अभिव्यंजित करेगा उतना ही अधिक वह सफल होगा।
संक्षिप्तता एवं पूर्णता–फ़ीचर लेख का आकार अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। कम-से-कम शब्दों में गागर में सागर भरने की कला ही फ़ीचर लेख की प्रमुख विशेषता है लेकिन फ़ीचर लेख इतना छोटा भी न हो कि वह विषय को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम ही न हो। विषय से संबंधित बिंदुओं में क्रमबद्धता और तारतम्यता बनाते हुए उसे आगे बढ़ाया जाए तो फ़ीचर स्वयं ही अपना आकार निश्चित कर लेता है।
चित्रात्मकता-फ़ीचर सीधी-सपाट शैली में न होकर चित्रात्मक होना चाहिए। सीधी और सपाट शैली में लिखे गए फ़ीचर पाठक पर अपेक्षित प्रभाव नहीं डालते। फ़ीचर को पढ़ते हुए पाठक के मन में उस विषय का एक ऐसा चित्र या बिम्ब उभरकर आना चाहिए जिसे आधार बनाकर लेखक ने फ़ीचर लिखा है।
लालित्ययुक्त भाषा – फ़ीचर की भाषा सहज, सरल और कलात्मक होनी चाहिए। उसमें बिम्बविधायिनी शक्ति द्वारा ही उसे रोचक बनाया जा सकता है। इसके लिए फ़ीचर की भाषा लालित्यपूर्ण होनी चाहिए। लालित्यपूर्ण भाषा द्वारा ही गंभीर से गंभीर विषय को रोचक एवं पठनीय बनाया जा सकता है। उपयुक्त शीर्षक-एक उत्कृष्ट फ़ीचर के लिए उपयुक्त शीर्षक भी होना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो फ़ीचर के विषय, भाव या संवेदना का पूर्ण बोध करा पाने में सक्षम हो। संक्षिप्तता एवं सारगर्भिता फ़ीचर के शीर्षक के अन्यतम गुण हैं। फ़ीचर को आकर्षक एवं रुचिकर बनाने के लिए काव्यात्मक, कलात्मक, आश्चर्यबोधक, भावात्मक, प्रश्नात्मक आदि शीर्षकों को रखा जाना चाहिए।
प्रश्नः 6. फ़ीचर लेखक में किन-किन गुणों का होना आवश्यक है?
उत्तरः
फ़ीचर लेखक में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है।
विशेषज्ञता-फ़ीचर लेखक जिस विषय को आधार बनाकर उस पर लेख लिख रहा है उसमें उसका विशेषाधिकार होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विषय पर न तो शोध कर सकता है और न ही उस विषय की बारीकियों को समझ सकता है। इसलिए विषय से संबंधित विशेषज्ञ व्यक्ति को अपने क्षेत्राधिकार के विषय पर लेख लिखने चाहिए।
बहुज्ञता-फ़ीचर लेखक को बहुज्ञ भी होना चाहिए। उसे धर्म, दर्शन, संस्कृति, समाज, साहित्य, इतिहास आदि विविध विषयों की समझ होनी चाहिए। उसके अंतर्गत अध्ययन की प्रवृत्ति भी प्रबल होनी चाहिए जिसके द्वारा वह अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक अपने फ़ीचर को आकर्षक, प्रभावशाली तथा तथ्यात्मकता से परिपूर्ण बना सकता है।
परिवेश की प्रति जागरूक-फ़ीचर लेखक को समसामयिक परिस्थितियों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। अपनी सजगता से ही वह जीवन की घटनाओं को सक्ष्मता से देख, समझ और महसूस कर पाता है जिसके आधार पर वह एक अच्छा फ़ीचर तैयार कर सकने योग्य विषय को ढूँढ लेता है। समाज की प्रत्येक घटना आम आदमी के लिए सामान्य घटना हो सकती है लेकिन जागरूक लेखक के लिए वह घटना अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन सकती है।
आत्मविश्वास-फ़ीचर लेखक को अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के विषय के भीतर झाँकने और उसकी प्रवृत्तियों को पकड़ने की क्षमता के लिए सबसे पहले स्वयं पर ही विश्वास करना होगा। अपने ज्ञान और अनुभव पर विश्वास करके ही वह विषय के भीतर तक झाँक सकता है।
निष्पक्ष दृष्टि-फ़ीचर लेखक के लिए आवश्यक है कि वह जिस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए फ़ीचर लेख लिख रहा है उस विषय के साथ वह पूर्ण न्याय कर सके। विभिन्न तथ्यों और सूत्रों के विश्लेषण के आधार पर वह उस पर अपना निर्णय प्रस्तुत करता है। लेकिन उसका निर्णय विषय के तथ्यों और प्रमाणों से आबद्ध होना चाहिए। उसे अपने निर्णय या दृष्टि को उस पर आरोपित नहीं करना चाहिए। उसे संकीर्ण दृष्टि से मुक्त हो किसी वाद या मत के प्रति अधिक आग्रहशील नहीं रहना चाहिए।
भाषा पर पूर्ण अधिकार-फ़ीचर लेखक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। भाषा के द्वारा ही वह फ़ीचर को लालित्यता और मधुरता से युक्त कर सकता है। उसकी भाषा माधुर्यपूर्ण और चित्रात्मक होनी चाहिए। इससे पाठक को भावात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने में लेखक को कठिनाई नहीं होती। विषय में प्रस्तुत भाव और विचार के अनुकूल सक्षम भाषा में कलात्मक प्रयोगों के सहारे लेखक अपने मंतव्य तक सहजता से पहँच सकता है।
प्रश्नः 7. फ़ीचर लेखन की तैयारी कैसे करें।
उत्तरः
फ़ीचर लेखन से पूर्व लेखक को निम्नलिखित तैयारियाँ करनी पड़ती हैं।
विषय चयन – फ़ीचर लेखन के विविध प्रकार होने के कारण इसके लिए विषय का चयन सबसे प्रथम आधार होता है। उत्कृष्ट फ़ीचर लेखन के लिए फ़ीचर लेखक को ऐसे विषय का चयन करना चाहिए. जो रोचक और ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ उसकी अपनी रुचि का भी हो। यदि लेखक की रुचि उस विषय क्षेत्र में नहीं होगी तो वह उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। रुचि के साथ उस विषय में लेखक की विशेषज्ञता भी होनी चाहिए अन्यथा वह महत्त्वपूर्ण से महत्त्वपूर्ण तथ्यों को भी छोड़ सकता है और गौण-से-गौण तथ्यों को भी फ़ीचर में स्थान दे सकता है। इससे विषय व्यवस्थित रूप से पाठक के सामने नहीं आ पाएगा।
फ़ीचर का विषय ऐसा होना चाहिए जो समय और परिस्थिति के अनुसार प्रासंगिक हो। नई से नई जानकारी देना समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं का उद्देश्य होता है। इसलिए तत्काल घटित घटनाओं को आधार बनाकर ही लेखक को विषय का चयन करना चाहिए। त्यौहारों, जयंतियों, खेलों, चुनावों, दुर्घटनाओं आदि जैसे विशिष्ट अवसरों पर लेखक को विशेष रूप से संबंधित विषयों का ही चयन करना चाहिए। लेखक को विषय का चयन करते समय पत्र-पत्रिका के स्तर, वितरण-क्षेत्र और पाठक-वर्ग की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। दैनिक समाचार-पत्रों में प्रतिदिन के जीवन से जुड़े फ़ीचर विषयों की उपयोगिता अधिक होती है। इसलिए समाचार-पत्र के प्रकाशन अवधि के विषय में भी लेखक को सोचना चाहिए।
सामग्री संकलन-फ़ीचर के विषय निर्धारण के उपरांत उस विषय से संबंधित सामग्री का संकलन करना फ़ीचर लेखक का अगला महत्त्वपूर्ण कार्य है। जिस विषय का चयन लेखक द्वारा किया गया है उस विषय के संबंध में विस्तृत शोध एवं अध्ययन के द्वारा उसे विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करना चाहिए। सामग्री संकलन के लिए वह विभिन्न माध्यमों का सहारा ले सकता है। इसके लिए उसे विषय से संबंधित व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने से फ़ीचर लेखक के लेख की शैली अत्यंत प्रभावशाली बन जाएगी।
फ़ीचर लेखक अपने लेख को अत्यधित पठनीय और प्रभावी बनाने के लिए साहित्य की प्रमुख गद्य विधाओं में से किसी का सहारा ले सकता है। आजकल कहानी, रिपोर्ताज, डायरी, पत्र, लेख, निबंध, यात्रा-वृत्त आदि आधुनिक विधाओं में अनेक फ़ीचर लेख लिखे जा रहे हैं। पाठक की रुचि और विषय की उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर फ़ीचर लेखक इनमें से किसी एक या मिश्रित रूप का प्रयोग कर सकता है।
अंत-फ़ीचर का अंतिम भाग उपसंहार या सारांश की तरह होता है। इसके अंतर्गत फ़ीचर लेखक अपने लेख के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विषय-वस्तु के आधार पर समस्या का समाधान, सुझाव या अन्य विचार-सूत्र देकर कर सकता है लेकिन लेखक के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह अपने दृष्टिकोण या सुझाव को किसी पर अनावश्यक रूप से न थोपे। अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर वह उस लेख का समापन इस तरह से करे कि वह पाठक की जिज्ञासा को शांत भी कर सके और उसे मानसिक रूप से तृप्ति भी प्रदान हो। अंत को आकर्षक बनाने के लिए फ़ीचर लेखक चाहे तो किसी कवि की उक्ति या विद्वान के विचार का भी सहारा ले सकता है। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। बस अंत ऐसा होना चाहए कि विषय-वस्तु को समझाने के लिए कुछ शेष न रहे।
फ़ीचर लेखक को अपना लेख लिखने के उपरान्त एक बार पुनः उसका अध्ययन करके यह देखना चाहिए कि कोई ऐसी बात उस लेख के अंतर्गत तो नहीं आई जो अनावश्यक या तथ्यों से परे हो। अगर ऐसा है तो ऐसे तथ्यों को तुरंत लेख से बाहर निकालकर पुनः लेख की संरचना को देखना चाहिए। अंत में अपने फ़ीचर को आकर्षक बनाने के लिए फ़ीचर लेखक उसकी विषय-वस्तु को इंगित करने वाले उपयुक्त ‘शीर्षक’ का निर्धारण करता है। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि पाठक जिसे पढ़ते ही उस फ़ीचर को पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाए। इसके लिए नाटकीय, काव्यात्मक, आश्चर्यबोधक, प्रश्नसूचक आदि विभिन्न रूपों के शीर्षकों का सहारा फ़ीचर लेखक ले सकता है।
अपने लेखक को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए फ़ीचर लेखक अपने लेख के साथ विषय से संबंधित सुंदर और उत्कृष्ट छायाचित्रों का चयन भी कर सकता है। इसके लिए चाहे तो वह स्वयं किसी चित्र को बनाकर या प्रासंगित चित्रों को स्वयं ही कैमरे से खींचकर उसे लेख के साथ छापने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। छायाचित्रों से फ़ीचर में जीवंतता और आकर्षण का भाव भर जाता है। छायाचित्रों से युक्त फ़ीचर विषय-वस्तु को प्रतिपादित करने वाले और उसे परिपूर्ण बनाने में सक्षम होने चाहिए।
नीचे फ़ीचर लेखन के तीन उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनसे आप फ़ीचर लेखन की संरचना को समझ सकते हैं।
उदाहरण
प्रश्नः 1. ‘नींद क्यूँ रात भर नहीं आती’
उत्तरः
आजकल महानगरों में अनिद्रा यानि की नींद न आने की शिकायत रोज़ बढ़ती जा रही है। अक्सर आपको आपके परिचित मित्र शिकायत करते मिल जायेंगे कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। रात भर वे या तो करवटें बदलते रहते हैं या घड़ी की ओर ताकते रहते हैं। कुछेक तो अच्छी नींद की चाह में नींद की गोली का सहारा भी लेते हैं।
नींद न आना, बीमारी कम, आदत ज़्यादा लगती है। वर्तमान युग में मनुष्य ने अपने लिए आराम की ऐसी अनेक सुविधाओं का विकास कर लिया है कि अब ये सुविधाएँ ही उसका आराम हराम करने में लगी हुई हैं। सूरज को उगते देखना तो शायद अब हमारी किस्मत में ही नहीं है। ‘जल्दी सोना’ और ‘जल्दी उठना’ का सिद्धांत अब बीते दिनों की बात हो चला है या यूँ कहिए कि समय के साथ वह भी ‘आऊटडेटेड’ हो गई है। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना अब दिनचर्या कम फ़ैशन ज्यादा हो गया है। लोग ये कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं कि रात को देर से सोया था जल्दी उठ नहीं पाया। जो बात संकोच से कही जानी चाहिए थी अब गर्व का प्रतीक हो गयी है। एक ज़माना था जब माता-पिता अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठने के संस्कार दिया करते थे। सुबह जल्दी उठकर घूमना, व्यायाम करना, दूध लाना आदि ऐसे कर्म थे जो व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा देते ही थे साथ ही उससे मेहनतकश बनने की प्रेरणा भी मिलती थी। मगर धीरे-धीरे आधुनिक सुख-सुविधाओं ने व्यक्ति को काहित बना दिया और इस काहिली में उसे अपनी सार्थकता अनुभव होने लगी है।
आराम की इस मनोवृत्ति ने मनुष्य को मेहनत से बेज़ार कर दिया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य की रोग-प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगी है और वह छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी दवाईयाँ खाने की कोशिश करता है जबकि इन बीमारियों का ईलाज केवल दिनचर्या-परिवर्तन से ही हो सकता है। नींद न आना ऐसी ही एक बीमारी है जो आधुनिक जीवन की एक समस्या है। हमारी आराम तलबी ने हमें इतना बेकार कर दिया है कि हम सोने में भी कष्ट का अनुभव करते हैं। रात भर करवटें बदलते हैं और दिन-भर ऊँघते रहते हैं। नींद न आने के लिए मुख्य रूप से हमारी मेहनत न करने की मनोवृत्ति जिम्मेदार है।
हम पचास गज की दूरी भी मोटर कार या स्कूटर से तय करने की इच्छा रखते हैं। सुबह घूमना हमें पसंद नहीं है, सीधे बैठकर लिखना या पढ़ना हमारे लिए कष्ट साध्य है। केवल एक मंजिल चढ़ने के लिए हमें लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारी आरामतलबी की इंतहा है। इसी आराम ने हमें सुखद नींद से कोसों दूर कर दिया है। नींद एक सपना होती जा रही है। अच्छी नींद लेने के लिए हमें विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता पड़ने लगी है जबकि इसका आसान-सा नुस्खा हमारी दादी और नानी ने ही बता दिया था कि खूब मेहनत करो, जमकर खाओ और चादर तानकर सो जाओ।
हज़ारों लाखों रुपये जोड़कर भी नींद नहीं खरीदी जा सकती। नींद तो मुफ्त मिलती है –कठोर श्रम से। शरीर जितना थकेगा, जितना काम करेगा, उतना ही अधिक आराम उसे मिलेगा। कुछ को नरम बिस्तरों और एयर कंडीश्नर कमरों में नींद नहीं आती और कुछ चिलचिलाती धूप में भी नुकीले पत्थरों पर घोड़े बेचकर सो जाते हैं। इसीलिए अच्छी नींद का एक ही नुस्खा है वो है-मेहनत-मेहनत-मेहनत। दिन-भर जी-तोड़ मेहनत करने वाले इसी नुस्खे को आजमाते हैं। नींद पाने के लिए हमें भी उन जैसा ही होना होगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है –
सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर,
मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते।
(लेखक : हरीश अरोड़ा)
प्रश्नः 2. भारतीय साहित्य की विशेषताओं पर एक फ़ीचर लिखिए।
उत्तरः
समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता, उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख है कि केवल इसके बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता का पताका फहराता रहा है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित करता रहा है। जिस तरह धर्म के क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी तरह साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रकृति समन्वय की ओर रही है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख-दुख, उत्थान-पतन, हर्ष-विषाद आदि विरोधी तथा विरपरीत भावों के सामान्यीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने से है। साहित्य के किसी भी अंग को लेकर देखिए? सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात-प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका आकर्षण बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है, जितना भविष्य उत्कर्ष से है। इसीलिए हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक दिखाई नहीं पड़ते हैं।
प्रश्नः 3. पर्यटन के महत्त्व पर एक फ़ीचर लिखिए।
उत्तरः
पर्यटन करना, घूमना, घुमक्कड़ी का ही आधुनिकतम नाम है। आज के पर्यटन के पीछे भी मनुष्य की घुमक्कड़ प्रवृत्ति ही कार्य कर रही है। आज भी जब वह देश-विदेश के प्रसिद्ध स्थानों की विशेषताओं के बारे में जब सुनता-पढ़ता है, तो उन्हें निकट से देखने, जानने के लिए उत्सुक हो उठता है। वह अपनी सुविधा और अवसर के अनुसार उस ओर निकल पड़ता है। आदिम घुमक्कड़ और आज के पर्यटक में इतना अंतर अवश्य है कि आज पर्यटन उतना कष्ट-साध्य नहीं है जितनी घुमक्कड़ी वृत्ति थी। ज्ञान-विज्ञान के आविष्कारों, अन्वेषणों की जादुई शक्ति के कारण एवं सुलभ साधनों के कारण आज पर्यटन पर निकलने के लिए अधिक सोच-विचार की आवश्यकता नहीं होती। आज तो मात्र सुविधा और संसाधन चाहिए। इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि पर्यटक बनने का जोखिम भरा आनंद तो उन पर्यटकों को ही आया होगा जिन्होंने अभावों और विषम परिस्थितियों से जूझते हुए देश-विदेश की यात्राएँ की होगी। फाह्यान, वेनसांग, अलबेरुनी, इब्नबतूता, मार्को पोलो आदि ऐसे ही यात्री थे।
पर्यटन के साधनों की सहज सुलभता के बावजूद आज भी पर्यटकों में पुराने जमाने के पर्यटकों की तरह उत्साह, धैर्य साहसिकता, जोखिम उठाने की तत्परता दिखाई देती है।
आज पर्यटन एक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। इस उद्योग के प्रसार के लिए देश-विदेश में पर्यटन मंत्रालय बनाए गए हैं। विश्वभर में पर्यटकों की सुविधा के लिए बड़े-बड़े पर्यटन केंद्र खुल चुके हैं।
प्रश्नः 4. आतंकवाद के प्रभाव पर एक फ़ीचर लिखिए।
उत्तरः
इस युग में अतिवाद की काली छाया इतनी छा गई है कि चारों ओर असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है। असंतोष की यह अभिव्यक्ति अनेक माध्यमों से होती है। आतंकवाद आज राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक अमोघ अस्त्र बन गया है। अपनी बात मनवाने के लिए आतंक उत्पन्न करने की पद्धति एक सामान्य नियम बन चुकी है। आज यदि शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करता है तो उसके प्रतिकार के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जा रहा है। उपेक्षित वर्ग भी अपना अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है।
स्वार्थबदध संकचित दृष्टि ही आतंकवाद की जननी है। क्षेत्रवाद, धर्मांधता, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारण, सांस्कृतिक टकराव, भाषाई मतभेद, आर्थिक विषमता, प्रशासनिक मशीनरी की निष्क्रियता और नैतिक ह्रास अंततः आतंकवाद के पोषण एवं प्रसार में सहायक बनते हैं। भारत को जिस प्रकार के आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है, वह भयावह और चिंतनीय है। यह चिंता इसलिए है क्योंकि उसके मूल में अलगाववादी और विघटनकारी ताकतें काम कर रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश के विभिन्न भागों में विदेशी शह पाकर आतंकवादी सक्रिय हो उठे थे। इसका दुष्परिणाम यह है कि आज कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तानी कबाइलियों और उनके देश में आए पाक सैनिकों के हाथ पहुँच गया है। आज भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है।
प्रश्नः 5. भारतीय संस्कृति की महत्ता अथवा अखंड परंपरा पर एक फ़ीचर लिखिए।
उत्तरः
सामाजिक संस्कारों का दूसरा नाम ही संस्कृति है। कोई भी समाज विरासत के रूप में इसे प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली है। संस्कृति ऐसी सामाजिक विरासत है जिसके पीछे एक लंबी परंपरा होती है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम तथा महत्त्वपूर्ण संस्कृतियों में से एक है। यह कब और कैसे विकसित हुई? यह कहना कठिन है प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। भारतीय संस्कृति के मूलरूप का परिचय हमें वेदों से ही मिलता है। वेदों की रचना ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विवरण भी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता पर पूर्णरूपेण प्रकाश डालता है। इसका इतना कालजयी और अखंड इतिहास इसे महत्त्वपूर्ण बनाता है। मिस्र, यूनान और रोम आदि देशों की संस्कृतियाँ आज केवल इतिहास बन कर सामने हैं। जबकि भारतीय संस्कृति एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा के साथ आज भी निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर है। इकबाल के शब्दों में कहा जा सकता है कि –
यूनान, मिस्र, रोम, सब मिट गए जहाँ से।
कुछ बात है, कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।।
प्रश्नः 6. नारी के संदर्भ में कही गई “नारी तू नारायणी” बात पर फ़ीचर लिखिए।
उत्तरः
प्राचीन युग में नारी केवल भोग की वस्तु थी। पुरुष नारी की आशा-आकांक्षाओं के प्रति बहुत उदासीन रहता था। अभागी नारी घर की लक्ष्मण रेखा को पार करने का दुस्साहस करने में बिलकुल असमर्थ थी। नारी को किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। नारी की स्थिति जिंदा लाश की तरह थी। वह बच्चे पैदा करने वाली मशीन के अतिरिक्त कुछ और न थी लेकिन आधुनिक युग में नारी ने अपने महत्ता को पहचाना। उसने दासता के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र वातावरण में सांस ली। आधुनिक नारी ने शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। इसीलिए आजकल किशोरों की अपेक्षा किशोरियाँ शिक्षा के क्षेत्र में कहीं आगे हैं। वह कला विषयों में ही नहीं बल्कि वाणिज्य और विज्ञान विषयों में भी अत्यंत सफलतापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।
आधुनिक नारी ने राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी महत्ता एवं प्रतिभा का परिचय दिया है। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कालजयी उदाहरण हमारे सामने है। भारत की राजनीति में ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान था। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आदि प्रदेशों की बागडोर भी महिला मुख्यमंत्रियों के हाथों में है। इंग्लैंड की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर भी एक महिला है। यूरोपीय देशों में नारियाँ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। हमारे देश की नारियाँ भी प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आज की नारी नौकरी द्वारा धन का अर्जन करती है। इस प्रकार वह आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुष को सहयोग देती है। आधुनिक नारी प्राचीन अंधविश्वास की बेड़ियों से सर्वथा मुक्त हो चुकी है। आज की नारी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को अधिक प्रश्रय देने लगी है।
आधुनिक नारियाँ नित नए क्षेत्र में कदम रख रही हैं। वे उन क्षेत्रों में मज़बूती से पाँव जमा रही हैं जिन पर कभी पुरुषों का एकाधिकार समझा जाता था। श्रीमती मधु जैन ने नारी की बढ़ती शक्ति के बारे में लिखा है कि-“आधुनिक नारी हवाई जहाज़ उड़ा रही है और कंपनी प्रबंधक पद पर पहुंच रही है।” अब तक केवल पुरुषों का क्षेत्र समझे जाने वाले शेयर बाज़ार में भी वह मौजूद है तो पत्रकारिता में भी। गैराज में वह कार दुरुस्त करती नज़र आती है तो ज़मीन-जायदाद के व्यवसाय में भी वह पीछे नहीं है। एकल परिवारों के बढ़ने से इस नई भारतीय नारी का आविर्भाव हुआ है। जो पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देती प्रतीत होती है।
आलेख लेखन
प्रश्नः 1.
आलेख के विषय में बताइए।
उत्तरः
आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं जो कि उचित भी है। लेख में सामान्यत: किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में ‘आ’ उपसर्ग लगता है जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक् और संपूर्ण होना चाहिए। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक् विचार प्रस्तुत करती है।
प्रश्नः 2.
सार्थक आलेख के गुण बताइए।
उत्तरः
सार्थक आलेख के निम्नलिखित गुण हैं –
- नवीनता एवं ताजगी।
- जिज्ञासाशील।
- विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण ।
- भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली।
- एक ही बात पुनः न लिखी जाए।
- विश्लेषण शैली का प्रयोग।
- आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्त्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए।
- आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए।
- संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख हो।
उदाहरण
1. भारतीय क्रिकेट का सरताज : सचिन तेंदुलकर
पिछले पंद्रह सालों से भारत के लोग जिन-जिन हस्तियों के दीवाने हैं-उनमें एक गौरवशाली नाम है-सचिन तेंदुलकर। जैसे अमिताभ का अभिनय में मुकाबला नहीं, वैसे सचिन का क्रिकेट में कोई सानी नहीं। संसार-भर में एक यही खिलाड़ी है जिसने टेस्ट-क्रिकेट के साथ-साथ वन-डे क्रिकेट में भी सर्वाधिक शतक बनाए हैं। अभी उसके क्रिकेट जीवन के कई वर्ष और बाकी हैं। यदि आगे आने वाला समय भी ऐसा ही गौरवशाली रहा तो उनके रिकार्ड को तोड़ने के लिए भगवान को फिर से नया अवतार लेना पड़ेगा। इसीलिए कुछ क्रिकेट-प्रेमी सचिन को क्रिकेट का भगवान तक कहते हैं। उसके प्रशंसकों ने हनुमान-चालीसा की तर्ज पर सचिन-चालीसा भी लिख दी है।
मुंबई में बांद्रा-स्थित हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला सचिन इतनी ऊँचाइयों पर पहुँचने पर भी मासूम और विनयी है। अहंकार तो उसे छू तक नहीं गया है। अब भी उसे अपने बचपन के दोस्तों के साथ वैसा ही लगाव है जैसा पहले था। सचिन अपने परिवार के साथ बिताए हुए क्षणों को सर्वाधिक प्रिय क्षण मानता है। इतना व्यस्त होने पर भी उसे अपने पुत्र का टिफिन स्कूल पहुँचाना अच्छा लगता है।
सचिन ने केवल 15 वर्ष की आयु में पाकिस्तान की धरती पर अपने क्रिकेट-जीवन का पहला शतक जमाया था जो अपने-आप में एक रिकार्ड है। उसके बाद एक-पर-एक रिकार्ड बनते चले गए। अभी वह 21 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि उसने टेस्ट क्रिकेट में 7 शतक ठोक दिए थे। उन्हें खेलता देखकर भारतीय लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर कहते थे-सचिन मेरा ही प्रतिरूप है।
2. ग्रामीण संसाधनों के बल पर आर्थिक स्वतंत्रता
समाज में सकारात्मक बदलाव के तीन ही मुख्य सूचक होते हैं। आचरण, आर्थिकी व संगठनात्मक पहल। इन तीनों से ही समाज को असली बल मिलता है और प्रगति के रास्ते भी तैयार होते हैं। इन सबको प्रभाव में लाने के लिए सामूहिक पहल ही सही दिशा दे सकती है।
हेस्को (हिमालयन एन्वायर्नमेंटल स्टडीज कन्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन) ने अपनी कार्यशैली में ये तीन मुद्दे केंद्र में रखकर सामाजिक यात्रा शुरू की। कुछ बातें स्पष्ट रूप से तय थीं कि किसी भी प्रयोग को स्थायी परिणाम तक पहुँचाना है तो स्थानीय भागीदारी, संसाधन और बाज़ार की सही समझ के बिना यह संभव नहीं होगा। वजह यह है कि बेहतर आर्थिकी गाँव समाज की पहली चिंता है और उसका स्थायी हल स्थानीय उत्पादों तथा संसाधनों से ही संभव है। सही, सरल व सस्ती तकनीक आर्थिक क्रांति का सबसे बड़ा माध्यम है। स्थानीय उत्पादों पर आधारित ब्रांडिंग गाँवों के उत्पादों पर उनका एकाधिकार भी तय कर सकती है और ये उत्पाद गुणवत्ता व पोषकता के लिए हमेशा पहचान बना सकते हैं, इसलिए बाज़ार के अवसर भी बढ़ जाते हैं।
गाँवों की बदलती आर्थिकी की दो बड़ी आवश्यकताएँ होती हैं। संगठनात्मक पहल, बराबरी व साझेदारी तय करती है। किसी • भी आर्थिक-सामाजिक पहल की बहुत-सी चुनौतियाँ संगठन के दम पर निपटाई जाती हैं। सामूहिक सामाजिक पहलुओं का अपना एक चरित्र व आचरण बन जाता है, जो आंदोलन को भटकने नहीं देता। हेस्को की इसी शैली ने हिमालय के घराटों में पनबिजली व पन उद्योगों की बड़ी क्रांति पैदा की। जहाँ ये घराट (पन चक्कियाँ) मृतप्राय हो गई थीं, अब एक बड़े आंदोलन के रूप में आटा पिसाई, धान कुटाई ही नहीं बल्कि पनबिजली पैदा कर घराटी नए सम्मान के साथ समाज में जगह बना चुके हैं।
इनके संगठन और आचरण ने मिलकर केंद्र व राज्यों में राष्ट्रीय घराट योजना के लिए सरकारों को बाध्य कर दिया। एक घराट की मासिक आय पहले 1,000 रुपए तक थी, आज वह 8,000 से 10,000 रुपए कमाता है। आज हज़ारों घराट नए अवतार में स्थानीय बिजली व डीजल चक्कियों को सीधे टक्कर दे रहे हैं। इन्होंने बाज़ार में अपना घराट आटा उतार दिया है, जो ज़्यादा पौष्टिक है।
फल-अनाज उत्पाद गाँवों को बहुत देकर नहीं जाते। विडंबना यह है कि उत्पादक या उपभोक्ता की बजाय सारा लाभ इनके बाजार या प्रसंस्करण में जुटा बीच का वर्ग ले जाता है। 1990 के दौरान हेस्को ने स्थानीय फल-फूलों को बेहतर मूल्य देने के लिए पहली प्रसंस्करण इकाई डाली और जैम-जेली जूस बनाने की शुरुआत की। देखते-देखते युवाओं-महिलाओं ने ऐसी इकाइयाँ डालनी शुरू की और आज उत्तराखंड में सैकड़ों प्रोसेसिंग इकाइयाँ काम कर रही हैं। एक-दूसरे के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संगठन भी खड़े कर दिए।
उत्तराखंड फ्रूट प्रोसेसिंग एसोसिएशन इसी का परिणाम है। ये जहाँ, अपने आपसी मुद्दों के प्रति सजग रहते हैं वहीं, सरकार को भी टोक-टोक कर रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से प्रयोगों ने आज बड़ी जगह बना ली है। उत्तराखंड में मिस्त्री, लोहार, कारपेंटर आज नए विज्ञान व तकनीक के सहारे बेहतर आय कमाने लगे हैं। पहले पत्थरों का काम, स्थानीय कृषि उपकरण व कुर्सी-मेज के काम शहरों के नए उत्पादनों के आगे फीके पड़ जाते थे। आज ये नए विज्ञान व तकनीक से लैस हैं। इनके संगठन ने इन्हें अपने हकों के लिए लड़ना भी सिखाया है।
हेस्को पिछले 30 वर्षों में ऐसे आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ, जिसमें हिमालय के ही नहीं बल्कि देश के कई संगठनों को भी दिशा दी है और ये आंदोलन मात्र आर्थिक ही नहीं था बल्कि समाज में संगठनात्मक व आचरण की मज़बूत पहल बनकर खड़ा हो गया। गाँवों की आर्थिकी का यह नया रास्ता अब राज्यों के बाद राष्ट्रीय आंदोलन होगा। जहाँ ग्रामीण संसाधनों पर आधारित गाँवों की अधिक स्वतंत्रता की पहल होगी।
3. कूड़े के ढेर हैं दुनिया की अगली चुनौती
शिक्षाविदों और पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर विश्व में अपशिष्ट के पचास महाकाय क्षेत्र हैं : 18 अफ्रीका में, 17 एशिया में, आठ दक्षिण अमेरिका में, पाँच मध्य अमेरिका और कैरिबियन में तथा दो यूरोप में। कूड़े की विशाल बस्तियाँ चीन में भी हैं, पर उनकी सही गिनती और ब्योरा पाना असंभव है। विश्व की आधी आबादी को बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट
सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनुमानतः दुनिया का लगभग चालीस फीसदी कूड़ा खुले में सड़ता है, जो निकट बस्तियों में रहनेवालों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। समृद्ध देशों में कूड़े की रीसाइकिलिंग महँगी पड़ती है। गरीब देशों के लिए कूड़ा अतिरिक्त आय का साधन बनता है, भले म अपशिष्ट को योजनाबद्ध और सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाने के लिए उनके पास धन व संसाधन का घोर अभाव हो। कारखानों, अस्पतालों से निकला विषाक्त मल ढोने वालों और उसकी री-साइकिलिंग करनेवालों के प्रशिक्षण या स्वास्थ्य सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं। वयस्क और युवा कूड़ा कर्मी नंगे हाथों काम करते हुए जख्मी होते हैं, उसमें से खाद्य सामग्री टटोलते और खाते फिरते हैं।
भीषण गरमी में बिना ढका-समेटा और सड़ता अपशिष्ट खतरनाक कीटाणु और जहरीली गैस पैदा करता है। बारिश में इसमें से रिसता पानी भूमिगत जल में समाता है और आसपास के नदी, नालों, जलाशयों को प्रदूषित करता है। जलते कूड़े की जहरीली गैस और घोर प्रदूषण के बीच जीविका कमाने वालों और निकटवर्ती बस्तियों में रहनेवाले लोगों के स्वास्थ्य को दीर्घावधि में जो हानि निश्चित है, उनका जीवन काल कितना घटा है, उसके प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन कितना चिंतित है? यह ऐसा टाइम बम है, जो फटने पर विश्व जन स्वास्थ्य में प्रलय ला सकता है। संयुक्त राष्ट्र को ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी में संसाधन प्रयोग कुशलता के लेक्चरार कॉस्टस वेलिस की चेतावनी है कि खुले कूड़े के विशालकाय ढेर मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर और पेट, त्वचा, सांस, आँख तथा जानलेवा जेनेटिक और संक्रामक रोगों के जनक हैं।
विकसित देशों की कई ज़रूरतें पिछड़े देशों से पूरी होती हैं। ज़रूरतमंद देशों की ‘स्वेटशॉप्स’ में बना सामान लागत से कई गुनी अधिक कीमत पर पश्चिमी देशों की दुकानों में सजता है। बड़ी बात नहीं कि कूड़े से ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी जर्मनी का अनुसरण करने वाले अन्य यूरोपीय देश अफ्रीका जैसे पिछड़े देशों से कूड़ा आयात करने लगें। वह कूड़ा, जो सर्वव्यापी उपभोक्तावाद के रूप में पश्चिम की देन का ही अंजाम है। यह भी निश्चित है कि तब संपूर्ण अपशिष्ट के बाकायदा ‘वेस्ट मैनेजमेंट’ के कड़े से कड़े नियम लागू किए जाने के लिए शोर भी उन्हीं की तरफ से उठेगा कि आयातित कडा पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित और आरोग्यकर हो।
मुंबई की देओनार कचरा बस्ती को ऐकरा (घाना), इबादान (नाइजीरिया), नैरोबी (केन्या), बेकैसी (इंडोनेशिया) जैसी अन्य विशाल कूड़ा बस्तियों की दादी-नानी कहा गया है। 1927 से अब तक इसमें 170 लाख टन कूड़े की आमद आंकी गई है। इससे लगभग छह मील की परिधि में रहने वाली पचास लाख आबादी के विरोध पर इसे धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है, पर अब भी 1,500 लोग यहाँ कूड़ा बीनने, छाँटने के काम से रोजी कमाते हैं। विश्व के समृद्ध देशों को भारतोन्मुख करने का सबसे सार्थक प्रयास ऊर्जा उत्पादन में हो सकता है। कूड़े से ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी यूरोपीय देशों की तकनीक भारत की कूड़ा बस्तियों को अभिशाप से वरदान में बदल सकती है।
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
एनडीए सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी है, जो इसी साल खरीफ सीजन से लागू होगी। इससे किसानों को प्राकृतिक या स्थानीय आपदा के चलते फ़सल को हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम, जैसे रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5 प्रतिशत, खरीफ फसलों के लिए दो फीसदी और वार्षिक, वाणिज्यक एवं बागवानी फसलों के लिए पाँच प्रतिशत देना होगा जबकि किसानों को बीमा राशि पूरी मिलेगी। सरकार इस पर करीब 8,800 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इससे साढ़े तेरह करोड़ किसानों को लाभ होगा।
यह कदम उठाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि विगत में शुरू की गई फ़सल बीमा योजनाएँ अब तक कारगर नहीं रही हैं। पिछली एनडीए सरकार ने 1999 में कृषि क्षेत्र में बीमा की शुरूआत कर एक अभिनव पहल की थी, पर यूपीए सरकार ने 2010 में इसमें कई ऐसे बदलाव कर दिए, जो किसानों के लिए घातक साबित हुए। मोदी सरकार की यह फ़सल बीमा योजना ‘एक राष्ट्र, एक योजना’ तथा ‘वन सीजन, वन प्रीमियम’ के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी।
यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई ‘संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना’ (एमएनएआइएस) की सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसमें प्रीमियम अधिक हो जाने पर एक अधिकतम सीमा निर्धारित रहती थी। नतीजतन किसान को मिलने वाली दावा राशि भी कम हो जाती थी।
जबकि नई बीमा योजना में कोई किसान यदि तीस हजार रुपये का बीमा कराता है, तो 22 प्रतिशत प्रीमियम होने पर भी मात्र 600 रुपये देने होंगे, जबकि बाकी के 6,000 रुपये का भुगतान सरकार करेगी। अगर किसान का शत-प्रतिशत नुकसान होता है, तो उसे 30 हजार रुपये की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी। पहले किसानों को 15 प्रतिशत तक प्रीमियम देना पड़ता था, पर अब इसे घटाकर डेढ़ से दो फीसदी कर दिया गया है। साथ ही, ओलावृष्टि, जलभराव और भूस्खलन को स्थानीय आपदा माना जाएगा। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को भी शामिल किया गया है। फ़सल कटने के 14 दिन तक फ़सल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है, तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी। पहले यह सुविधा सिर्फ तटीय क्षेत्रों को प्राप्त थी।
अब तक देखा गया है कि फ़सल बीमा होने के बावजूद किसानों को बीमित राशि लेने के लिए जगह-जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग का फैसला किया गया है। इससे फ़सल कटाई/नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सकेगा और किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सकेगी। इसके लिए सरकार रिमोट सेंसिंग तकनीक और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेगी। कुल मिलाकर, सरकार ने किसानों के हित में एक समग्र योजना की शुरूआत की है, जिसका लाभ पूरे देश के किसानों को मिलेगा।
5. नए सामाजिक बदलाव
जब भारत आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ाने के साथ सबको तरक्की का लाभ देने और शिक्षा, ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा है तो सामाजिक उद्यमशीलता (सोशल आंत्रप्रेन्योरशिप) स्थायी सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा जरिया साबित हो रहा है। सोशल आंत्रप्रेन्योर बुद्ध की करुणा और उद्योगपति की व्यावसायिक बुद्धिमानी का मिश्रण होता है। यानी वे उद्यमशीलता का माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने वाला बदलाव के वाहक हैं।
समाज की ज्वलंत समस्याओं के लिए उसके पास इनोवेटिव समाधान होते हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए किसी बाधा को आड़े नहीं आने देता। पिछले एक दशक में देश में बदलाव का यह जरिया बहुत तेजी से बढ़ा है और इसमें आईआईएम और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के युवाओं ने गहरी रुचि दिखाई है। एक उदाहरण बिहार के ऐसे पिछड़े इलाकों का दिया जा सकता है, जहाँ अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। सामाजिक उद्यमशीलता के जरिये भूसे से बिजली बनाकर ये इलाके रोशन किए गए हैं।
भारत में सामाजिक उदयमों के जरिये शिक्षा से स्वास्थ्य रक्षा, अक्षय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, ई-लर्निंग व ई-बिजनेस, आवास, झुग्गी-झोपड़ियों का विकास, जलप्रदाय व स्वच्छता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और महिलाओं, बच्चों व बुजर्गों से संबंधित कई समस्याओं को हल किया जा रहा है। इन सामाजिक उद्यमों का मुख्य उद्देश्य देश के वंचितों व हाशिये पर पड़े तबकों को टिकाऊ और गरिमामय जिंदगी मुहैया कराना है। खास बात यह है कि मुनाफे को ध्यान में रखते हुए सामाजिक बदलाव हासिल करने के स्तर में फर्क हो सकता है, लेकिन हर प्रयास में आर्थिक टिकाऊपन को आधार बनाया गया है, क्योंकि इसी से स्थायी बदलाव लाया जा सकता है।
इसका एक तरीका ऐसे बिजनेस मॉडल अपनाना है, जो सामाजिक समस्याएँ सुलझाने के लिए सस्ते उत्पादों व सेवाओं पर जोर देते हैं। लक्ष्य ऐसा सामाजिक बदलाव लाना है, जो व्यक्तिगत मुनाफे से मर्यादित नहीं है। गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की बजाय सामाजिक आंत्रप्रेन्योरशिप व्यापक पैमाने पर बदलाव लाता है। एनजीओ से वे इस मायने में अलग हैं कि उनका उद्देश्य छोटे पैमाने और निश्चित समय-अवधि से सीमित बदलाव की जगह व्यापक आधार वाले, दीर्घावधि बदलाव लाना है।
फिर एनजीओ आयोजनों, गतिविधियों और कभी-कभी प्रोडक्ट बेचकर पैसा जुटाते हैं, लेकिन पैसा इकट्ठा करने में समय और ऊर्जा लगती है, जिनका उपयोग सीधे काम करने और प्रोडक्ट की मार्केटिंग में किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सामाजिक आंत्रप्रेन्योर प्रभावित लोगों को निष्क्रिय लाभान्वितों की बजाय समाधान का हिस्सा मानता है। मसलन, माइक्रो फाइनेंस को लें। कई संगठन कमज़ोर तबकों खासतौर पर महिलाओं को कम राशि के लोन देकर उनकी जिंदगी बदल रहे हैं। लोन के जरिये वे कोई काम शुरू करते हैं और उन्हें आजीविका का स्थायी जरिया मिलता है। देश में काम कर रहे कुछ माइक्रो फाइनेंस को लें।
कई संगठन कमज़ोर तबकों खासतौर पर महिलाओं को कम राशि के लोन देकर उनकी जिंदगी बदल रहे हैं। लोन के जरिये वे कोई काम शुरू करते हैं और उन्हें आजीविका का स्थायी जरिया मिलता है। देश में काम कर रहे कुछ माइक्रो फाइनेंस संगठन दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते ऐसे संगठन हैं। सामाजिक उदयमशीलता.के जरिये जिन क्षेत्रों में बदलाव लाया जा रहा है उनमें सबसे पहले हैं सस्ती स्वास्थ्य-रक्षा सुविधाएँ। देश में 60 फीसदी आबादी गाँवों व छोटे कस्बों में रहती हैं, जबकि 70 फीसदी मध्यम व बड़े अस्पताल बड़े शहरों व महानगरों में है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 80 फीसदी माँग प्राथमिक व द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए हैं और केवल 30 फीसदी अस्पताल से सुविधाएं मुहैया कराते हैं। स्वास्थ्य रक्षा की बड़ी खामी सामाजिक उद्यमों के द्वारा दूर की जा रही है।
इसी तरह शहरी आवास बाजार में 1.88 आवासीय इकाइयों की कमी है। सामाजिक उद्यमशीलता से निर्माण लागत व समय में कमी लाकर बदलाव लाया जा रहा है। पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में भी इस तरह का बदलाव देखा जा रहा है। जलदोहन और संग्रहण, सप्लाई और वितरण और कचना प्रबंधन। इसमें खासतौर पर वर्षा के पानी के उपयोग पर काम हो रहा है। स्वच्छता में खास मॉडल में घरों में टॉयलेट का निर्माण, भुगतान पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले टॉयलेट और ‘इकोसन टॉयलेट’ के जरिये बायो फ्यूल बनाया जा रहा है। देश में 70 फीसदी से अधिक ग्रामीण आबादी को खेती से आजीविका मिलती है। इसकी खामियों को दूर कर आर्थिक व सामाजिक बदलाव लाया जा रहा है। इसमें फ़सल आने के पहले की सुविधाओं और फ़सल को बाजार तक पहुँचाने की श्रृंखला पर काम करके बदलाव लाया जा रहा है।
अपठित काव्यांश
1. शांति नहीं तब तक, जब तक
सुख-भाग न सबका सम हो।
नहीं किसी को बहुत अधिक हो
नहीं किसी को कम हो।
स्वत्व माँगने से न मिले,
संघात पाप हो जाएँ।
बोलो धर्मराज, शोषित वे
जिएँ या कि मिट जाएँ?
न्यायोचित अधिकार माँगने
से न मिले, तो लड़ के
तेजस्वी छीनते समय को,
जीत, या कि खुद मर के।
किसने कहा पाप है? अनुचित
स्वत्व-प्राप्ति-हित लड़ना?
उठा न्याय का खड्ग समर में
अभय मारना-मरना?
प्रश्नः
(क) कवि के अनुसार शांति के लिए क्या आवश्यक शर्त है?
(ख) तेजस्वी किस प्रकार समय को छीन लेते हैं ?
(ग) न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए?
(घ) कृष्ण युधिष्ठिर को युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं ?
उत्तरः
(क) कवि के अनुसार, शांति के लिए आवश्यक है कि संसार में संसाधनों का वितरण समान हो।
(ख) अपने अनुकूल समय को तेजस्वी जीतकर छीन लेते हैं।
(ग) न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। अपना हक माँगना पाप नहीं है।
(घ) कृष्ण युधिष्ठिर को युद्ध के लिए इसलिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि वे अपने हक को पा सकें, अपने प्रति अन्याय को खत्म कर सकें।
2. नीड़ का निर्माण फिर-फिर
नेह का आह्वान फिर-फिर
वह उठी आँधी कि नभ में
छा गया सहसा अँधेरा
धूलि-धूसर बादलों ने
भूमि को इस भाँति घेरा,
रात-सा दिन हो गया फिर
रात आई और काली,
लग रहा था अब न होगा,
इस निशा का फिर सवेरा,
रात के उत्पात-भय से
भीत जन-जन, भीत कण-कण
किंतु प्राची से उषा की
मोहिनी मुसकान फिर-फिर
नीड़ का निर्माण फिर-फिर
नेह का आह्वान फिर-फिर
प्रश्नः
(क) आँधी तथा बादल किसके प्रतीक हैं ? इनके क्या परिणाम होते हैं ?
(ख) कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है?
(ग) कवि किस बात से भयभीत है और क्यों?
(घ) उषा की मुसकान मानव-मन को क्या प्रेरणा देती है?
उत्तरः
(क) आँधी और बादल विपदाओं के प्रतीक हैं। जब विपदाएँ आती हैं तो उससे जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। मानव मन का उत्साह नष्ट हो जाता है।
(ख) कवि निर्माण का आह्वान इसलिए करता है ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। निर्माण ही जीवन की गति है।
(ग) विपदाओं के कारण चारों तरफ निराशा का माहौल था। कवि को लगता था कि निराशा के कारण निर्माण कार्य रुक जाएगा।
(घ) उषा की मुसकान मानव में कार्य करने की इच्छा जगाती है। वह मानव को निराशा के अंधकार से बाहर निकालती है।
3. पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे,
और प्रज्वलित प्राण देश कया कभी मरेगा मारे?
लहू गर्म करने को रक्खो मन में ज्वलित विचार,
हिंसक जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार ।
एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर-नारी
कलम उगलती आग, जहाँ अक्षर बनते चिंगारी
जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले,
बातों में बिजली होती, होते दिमाग में गोले।
जहाँ लोग पालते लहू में हालाहल की धार
क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार?
प्रश्नः
(क) कलम किस बात की प्रतीक है?
(ख) तलवार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है?
(ग) लहू को गरम करने से कवि का क्या आशय है?
(घ) कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती?
उत्तरः
(क) कलम क्रांति पैदा करने का प्रतीक है। वह वैचारिक क्रांति लाती है।
(ख) तलवार की आवश्यकता हिंसक पशुओं से बचने के लिए होती है अर्थात् अन्यायी को समाप्त करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है।
(ग) इसका अर्थ है-क्रांतिकारी विचारों से मन में जोश व उत्साह का बनाए रखना।
(घ) वे व्यक्ति जिनमें अंदर जोश है, वैचारिक शक्ति है, उन्हें तलवार की ज़रूरत नहीं होती।
4. यह लघु सरिता का बहता जल
कितना शीतल, कितना निर्मल
हिमगिरि के हिम से निकल-निकल,
यह विमल दूध-सा हिम का जल,
कर-कर निनाद कल-कल, छल-छल,
तन का चंचल मन का विह्वल
यह लघु सरिता का बहता जल।
ऊँचे शिखरों से उतर-उतर
गिर-गिर, गिरि की चट्टानों पर,
कंकड़-कंकड़ पैदल चलकर
दिनभर, रजनी-भर, जीवन-भर
धोता वसुधा का अंतस्तल
यह लघु सरिता का बहता जल।
हिम के पत्थर वो पिघल-पिघल,
बन गए धरा का वारि विमल,
सुख पाता जिससे पथिक विकल
पी-पी कर अंजलि भर मृदुजल
नित जलकर भी कितना शीतल
यह लघु सरिता का बहता जल।
कितना कोमल कितना वत्सल
रे जननी का वह अंतस्तल,
जिसका यह शीतल करुणाजल
बहता रहता युग-युग अविरल
गंगा, यमुना, सरयू निर्मल
यह लघु सरिता का बहता जल।
प्रश्नः
(क) वसुधा का अंतस्तल धोने में जल को क्या-क्या करना पडता है?
(ख) जल की तुलना दूध से क्यों की गई है?
(ग) आशय स्पष्ट कीजिए-‘तन का चंचल मन का विह्वल’
(घ) ‘रे जननी का वह अंतस्तल’ में जननी किसे कहा गया है?
उत्तरः
(क) वसुधा का अंतस्तल धोने के लिए जल ऊँचे पर्वतों से उतरकर पर्वतों की चट्टानों पर गिरकर कंकड़-कंकड़ों पर पैदल चलते हुए दिन-रात जीवन पर्यंत कार्य करता है।
(ख) हिम के पिघलने से जल बनता है जो शुद्ध व पवित्र होता है। दूध को भी पवित्र व शुद्ध माना जाता है। अतः जल की तुलना दूध से की गई है।
(ग) इसका मतलब है कि जिस प्रकार शरीर में मन चंचल अपने भावों के कारण हर वक्त गतिशील रहता है, उसी तरह छोटी नदी का जल भी हर समय गतिमान रहता है।
(घ) इसमें भारत माता को जननी कहा गया है।
5. यह जीवन क्या है ? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है।
सुख-दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है।
कब फूटा गिरि के अंतर से? किस अंचल से उतरा नीचे।
किस घाटी से बह कर आया समतल में अपने को खींचे।
निर्झर में गति है जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है।
धुन एक सिर्फ़ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है।
बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता,
बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता।
लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है,
तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है।
निर्झर कहता है बढ़े चलो! देखो मत पीछे मुड़कर,
यौवन कहता है बढ़े चलो! सोचो मत क्या होगा चल कर।
चलना है केवल चलना है! जीवन चलता ही रहता है,
रुक जाना है मर जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है।
प्रश्नः
(क) जीवन की तुलना निर्झर से क्यों की गई है?
(ख) जीवन और निर्झर में क्या समानता है ?
(ग) जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
(घ) ‘तब यौवन बढ़ता है आगे!’ से क्या आशय है?
उत्तरः
(क) जीवन व निर्झर में समानता है क्योंकि दोनों में मस्ती होती है तथा दोनों ही सुख-दुख के किनारों के बीच चलते हैं।
(ख) जीवन की तुलना निर्झर से की गई है क्योंकि जिस तरह निर्झर विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे चलता रहता है, उसी प्रकार जीवन भी बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता है।
(ग) जीवन का उद्देश्य सिर्फ चलना है। रुक जाना उसके लिए मृत्यु के समान है।
(घ) इसका आशय है कि जब जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो आम व्यक्ति रुक जाता है, परंतु युवा शक्ति आगे बढ़ती है। वह परिणाम की परवाह नहीं करती।
6. आँसू से भाग्य पसीजा है, हे मित्र कहाँ इस जग में?
नित यहाँ शक्ति के आगे, दीपक जलते मग-मग में।
कुछ तनिक ध्यान से सोचो, धरती किसती हो पाई ?
बोलो युग-युग तक किसने, किसकी विरुदावलि गाई ?
मधुमास मधुर रुचिकर है, पर पतझर भी आता है।
जग रंगमंच का अभिनय, जो आता सो जाता है।
सचमुच वह ही जीवित है, जिसमें कुछ बल-विक्रम है।
पल-पल घुड़दौड़ यहाँ है, बल-पौरुष का संगम है।
दुर्बल को सहज मिटाकर, चुपचाप समय खा जाता,
वीरों के ही गीतों को, इतिहास सदा दोहराता।
फिर क्या विषाद, भय चिंता जो होगा सब सह लेंगे,
परिवर्तन की लहरों में जैसे होगा बह लेंगे।
प्रश्नः
(क) ‘रोने से दुर्भाग्य सौभाग्य में नहीं बदल जाता’ के भाव की पंक्तियाँ छाँटकर लिखिए।
(ख) समय किसे नष्ट कर देता है और कैसे?
(ग) इतिहास किसे याद रखता है और क्यों?
(घ) ‘मधुमास मधुर रुचिकर है, पर पतझर भी आता है’ पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तरः
(क) ये पंक्तिया हैं आँसू से भाग्य पसीजा है, हे मित्र, कहाँ इस जग में नित यहाँ शक्ति के आगे, दीपक जलते मग-मग में।
(ख) समय हमेशा कमजोर व्यवस्था को चुपचाप नष्ट कर देता है। दुर्बल तब समय के अनुसार स्वयं को बदल नहीं पाता तथा प्रेरणापरक कार्य नहीं करता।
(ग) इतिहास उन्हें याद रखता है जो अपने बल व पुरुषार्थ के आधार पर समाज के लिए कार्य करते हैं। प्रेरक कार्य करने वालों को जनता याद रखती है।
(घ) इसका अर्थ है कि अच्छे दिन सदैव नहीं रहते। मानव के जीवन में पतझर जैसे दुख भी आते हैं।
7. तरुणाई है नाम सिंधु की उठती लहरों के गर्जन का,
चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने जिनके जीवन का।
विफल प्रयासों से भी दूना वेग भुजाओं में भर जाता,
जोड़ा करता जिनकी गति से नव उत्साह निरंतर नाता।
पर्वत के विशाल शिखरों-सा यौवन उसका ही है अक्षय,
जिनके चरणों पर सागर के होते अनगिन ज्वार साथ लय।
अचल खड़े रहते जो ऊँचा, शीश उठाए तूफ़ानों में,
सहनशीलता दृढ़ता हँसती जिनके यौवन के प्राणों में।
वही पंथ बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हों निर्झर,
प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर।
प्रश्नः
(क) कवि ने किसका आह्वान किया है और क्यों?
(ख) तरुणाई की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है?
(ग) मार्ग की रुकावटों को कौन तोड़ते हैं और कैसे?
(घ) आशय स्पष्ट कीजिए-‘जिनके चरणों पर सागर के होते अनगिन ज्वार साथ लय।’
उत्तरः
(क) कवि ने युवाओं का आह्वान किया है क्योंकि उनमें उत्साह होता है और वे संघर्ष क्षमता से युक्त होते हैं।
(ख) तरुणाई की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है-उत्साह, कठिन परिस्थितियों का सामना करना, हार से निराश न होना, दृढ़ता, सहनशीलता आदि।
(ग) मार्ग की रुकावटों को युवा शक्ति तोड़ती है। जिस प्रकार झरने चट्टानों को तोड़ते हैं, उसी प्रकार युवा शक्ति अपने पंथ की रुकावटों को खत्म कर देती है।
(घ) इसका अर्थ है कि युवा शक्ति जनसामान्य में उत्साह का संचार कर देती है।
8. अचल खड़े रहते जो ऊँचा शीश उठाए तूफानों में,
सहनशीलता, दृढ़ता हँसती जिनके यौवन के प्राणों में।
वही पंथ बाधा तो तोड़े बहते हैं जैसे हों निर्झर,
प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर।
आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई,
नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जगकर है लहराई।
आज विगत युग के पतझर पर तुमको नव मधुमास खिलाना,
नवयुग के पृष्ठों पर तुमको है नूतन इतिहास लिखाना।
उठो राष्ट्र के नवयौवन तुम दिशा-दिशा का सुन आमंत्रण,
जागो, देश के प्राण जगा दो नए प्रात का नया जागरण।
आज विश्व को यह दिखला दो हममें भी जागी तरुणाई,
नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई।
प्रश्नः
(क) मार्ग की रुकावटों को कौन तोड़ता है और कैसे?
(ख) नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं ?
(ग) “विगत युग के पतझर’ से क्या आशय है?
(घ) कवि देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है?
उत्तरः
(क) मार्ग की रुकावटों को वीर तोड़ता है। वे अपने उत्साह, संघर्ष, सहनशीलता व वीरता से पथ की बाधाओं को दूर करते हैं।
(ख) नवयुवक प्रगति के नाम को दुर्गम रास्तों पर चलकर सार्थक करते हैं।
(ग) इसका आशय है कि पिछले कुछ समय से देश में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पा रहा है।
(घ) कवि देश के नवयुवकों का आह्वान इसलिए कर रहा है क्योंकि उनमें नए, कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। वे नए इतिहास को लिख सकते हैं। उन्हें देश में नया उत्साह जगाना है।
9. मैंने गढ़े
ताकत और उत्साह से
भरे-भरे
कुछ शब्द
जिन्हें छीन लिया मठाधीशों ने
दे दिया उन्हें धर्म का झंडा
उन्मादी हो गए
मेरे शब्द
तलवार लेकर
बोऊँगी उन्हें मिटाने लगे
अपना ही वजूद
फिर रचे मैंने
इंसानियत से लबरेज
ढेर सारे शब्द
नहीं छीन पाएगा उन्हें
छीनने की कोशिश में भी
गिर ही जाएँगे कुछ दाने
और समय आने पर
फिर उगेंगे वे
अबकी उन्हें अगवा कर लिया
सफ़ेदपोश लुटेरों ने
और दबा दिया उन्हें
कुर्सी के पाये तले
असहनीय दर्द से चीख रहे हैं
मेरे शब्द और वे
कर रहे हैं अट्टहास
अब मैं गर्दैगी
निराई गुड़ाई और
खाद-पानी से
लहलहा उठेगी फ़सल
तब कोई मठाधीश
कोई लुटेरा
एक बार
दो बार
बार-बार
लगातार उगेंगे
मेरे शब्द
प्रश्नः
(क) ‘मठाधीशों’ ने उत्साह भरे शब्दों को क्यों छीना होगा?
(ख) आशय समझाइए-कुर्सी के पाये तले दर्द से चीख रहे हैं
(ग) कवयित्री किस उम्मीद से शब्दों को बो रही है?
(घ) ‘और वे कर रहे हैं अट्टहास’ में ‘वे’ शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है?
उत्तरः
(क) मठाधीशों ने उत्साह भरे शब्दों को छीन लिया ताकि वे धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सके।
(ख) इसका आशय है कि सत्ता ने इंसानियत के शब्दों को कैद कर लिया। वे मुक्ति चाहते हैं, परंतु सत्ता उन्हें अपने हितों के लिए इस्तेमाल करती है।
(ग) कवयित्री अपने शब्दों को बो रही है ताकि इन शब्दों को कोई लूट या कब्जा न कर सके। जब इनकी फ़सल उग जाएगी तो ये चिरस्थायी हो जाएँगे।
(घ) ‘वे’ शब्द सफ़ेदपोश लुटेरों के लिए है।
10. खुल कर चलते डर लगता है
बातें करते डर लगता है
क्योंकि शहर बेहद छोटा है।
ऊँचे हैं, लेकिन खजूर से
मुँह है इसीलिए कहते हैं,
जहाँ बुराई फूले-पनपे-
वहाँ तटस्थ बने रहते हैं,
नियम और सिद्धांत बहुत
दंगों से परिभाषित होते हैं-
जो कहने की बात नहीं है,
वही यहाँ दुहराई जाती,
जिनके उजले हाथ नहीं हैं,
उनकी महिमा गाई जाती
यहाँ ज्ञान पर, प्रतिभा पर,
अवसर का अंकुश बहुत कड़ा है-
सब अपने धंधे में रत हैं
यहाँ न्याय की बात गलत है
क्योंकि शहर बेहद छोटा है।
बुद्धि यहाँ पानी भरती है,
सीधापन भूखों मरता है-
उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है,
जो सारे काम गलत करता है।
यहाँ मान के नाप-तौल की,
इकाई कंचन है, धन है-
कोई सच के नहीं साथ है
यहाँ भलाई बुरी बात है।
क्योंकि शहर बेहद छोटा है।
प्रश्नः
(क) कवि शहर को छोटा कहकर किस ‘छोटेपन’ को अभिव्यक्त करना चाहता है ?
(ख) इस शहर के लोगों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?
(ग) आशय समझाइए
‘बुद्धि यहाँ पानी भरती है,
सीधापन भूखों मरता है’
(घ) इस शहर में असामाजिक तत्व और धनिक क्या-क्या प्राप्त करते हैं ?
उत्तरः
(क) कवि ने शहर को छोटा कहा है क्योंकि यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्तियों के स्वार्थ में डूबे होने के कारण हर जगह अन्याय स्थापित हो रहा है।
(ख) इस शहर के लोग संवेदनहीन, स्वार्थी, डरपोक, अन्यायी का गुणगान करने वाले व निरर्थक प्रलाप करने वाले हैं।
(ग) इस पंक्ति का आशय है कि यहाँ विद्वान व समझदार लोगों को महत्त्व नहीं दिया जाता। सरल स्वभाव का व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता।
(घ) इस शहर में असामाजिक तत्व दंगों से अपना शासन स्थापित करते हैं तथा नियम बनाते हैं। धनिक अवैध कार्य करके धन कमाते हैं।
11. जाग रहे हम वीर जवान,
जियो, जियो ऐ हिंदुस्तान!
हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल,
हम नवीन भारत के सैनिक, धीर, वीर, गंभीर, अचल।
हम प्रहरी ऊँचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं,
हम हैं शांति-दूत धरणी के, छाँह सभी को देते हैं।
वीरप्रसू माँ की आँखों के, हम नवीन उजियाले हैं,
गंगा, यमुना, हिंद महासागर के हम ही रखवाले हैं।
तन, मन, धन, तुम पर कुर्बान,
जियो, जियो ऐ हिंदुस्तान!
हम सपूत उनके, जो नर थे, अनल और मधु के मिश्रण,
जिनमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन।
एक नयन संजीवन जिनका, एक नयन था हालाहल,
जितना कठिन खड्ग था कर में, उतना ही अंतर कोमल।
थर-थर तीनों लोक काँपते थे जिनकी ललकारों पर,
स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर।
हम उन वीरों की संतान,
जियो, जियो ऐ हिंदुस्तान!
प्रश्नः
(क) ‘नवीन भारत’ से क्या तात्पर्य है?
(ख) उस पंक्ति को उद्धृत कीजिए जिसका आशय है कि भारतीय बाहर से चाहे कठोर दिखाई पड़ें, उनका हृदय कोमल होता है।
(ग) ‘हम उन वीरों की संतान’-उन पूर्वज वीरों की कुछ विशेषताएँ लिखिए।
(घ) ‘वीरप्रसू माँ’ किसे कहा गया है? क्यों?
उत्तरः
(क) ‘नवीन भारत’ से तात्पर्य है-आज़ादी के पश्चात् निरंतर विकसित होता भारत।
(ख) उक्त भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है-जितना कठिन खड्ग था कर में, उतना ही अंतर कोमल।
(ग) कवि ने पूर्वज वीरों की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं
- इनकी वीरता से संसार भयभीत था।
- वीरों में आग व मधु का मेल था।
- वीरों में तेज था, परंतु वे कोमल भावनाओं से युक्त थे।
(घ) ‘वीरप्रसू माँ’ से तात्पर्य भारतमाता से है। भारतमाता ने देश का मान बढ़ाने वाले अनेक वीर दिए हैं।
अपठित गद्यांश
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए
1. संवाद में दोनों पक्ष बोलें यह आवश्यक नहीं। प्रायः एक व्यक्ति की संवाद में मौन भागीदारी अधिक लाभकर होती है। यह स्थिति संवादहीनता से भिन्न है। मन से हारे दुखी व्यक्ति के लिए दूसरा पक्ष अच्छे वक्ता के रूप में नहीं अच्छे श्रोता के रूप में अधिक लाभकर होता है। बोलने वाले के हावभाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक-सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। संवाद से संबंध बेहतर भी होते हैं और अशिष्ट संवाद संबंध बिगाड़ने का कारण भी बनता है। बात करने से बड़े-बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ तक हल हो जाती हैं।
पर संवाद की सबसे बड़ी शर्त है एक-दूसरे की बातें पूरे मनोयोग से, संपूर्ण धैर्य से सुनी जाएँ। श्रोता उन्हें कान से सुनें और मन से अनुभव करें तभी उनका लाभ है, तभी समस्याएँ सुलझने की संभावना बढ़ती है और कम-से-कम यह समझ में आता है कि अगले के मन की परतों के भीतर है क्या? सच तो यह है कि सुनना एक कौशल है जिसमें हम प्रायः अकुशल होते हैं। दूसरे की बात काटने के लिए, उसे समाधान सुझाने के लिए हम उतावले होते हैं और यह उतावलापन संवाद की आत्मा तक हमें पहुँचने नहीं देता।
हम तो बस अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। तब दूसरे पक्ष को झुंझलाहट होती है। वह सोचता है व्यर्थ ही इसके सामने मुँह खोला। रहीम ने ठीक ही कहा था-“सुनि अठिलैहैं लोग सब, बाँटि न लैहैं कोय।” ध्यान और धैर्य से सुनना पवित्र आध्यात्मिक कार्य है और संवाद की सफलता का मूल मंत्र है। लोग तो पेड़-पौधों से, नदी-पर्वतों से, पशु-पक्षियों तक से संवाद करते हैं। राम ने इन सबसे पूछा था क्या आपने सीता को देखा?’ और उन्हें एक पक्षी ने ही पहली सूचना दी थी। इसलिए संवाद की अनंत संभावनाओं को समझा जाना चाहिए।
प्रश्नः 1.
उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
उत्तरः
शीर्षक-संवाद : एक कौशल।
प्रश्नः 2.
‘संवादहीनता’ से क्या तात्पर्य है ? यह स्थिति मौन भागीदारी से कैसे भिन्न है?
उत्तरः
संवादहीनता से तात्पर्य है-बातचीत न होना। यह स्थिति मौन भागीदारी से बिलकुल अलग है। मौन भागीदारी में एक बोलने वाला होता है। संवादहीनता में कोई भी पक्ष अपनी बात नहीं कहता।
प्रश्नः 3.
भाव स्पष्ट कीजिए- “यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुँचने देता।”
उत्तरः
इसका भाव यह है कि बातचीत के समय हम दूसरे की बात नहीं सुनते। हम अपने सुझाव उस पर थोपने की कोशिश करते हैं। इससे दूसरा पक्ष अपनी बात को समझा नहीं पाता और हम संवाद की मूल भावना को खत्म कर देते हैं।
प्रश्नः 4.
दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष कब अधिक लाभकर होता है? क्यों?
उत्तरः
दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष तब अधिक लाभकर होता है जब वह अच्छा श्रोता बने। दुखी व्यक्ति अपने मन की बात कहकर अपने दुख को कम करना चाहता है। वह दूसरे की नहीं सुनना चाहता।
प्रश्नः 5.
सुनना कौशल की कुछ विशेषताएँ लिखिए।
उत्तरः
सुनना कौशल की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(क) एक-दूसरे की बात पूरे मनोयोग से सुननी चाहिए।
(ख) श्रोता उन्हें सुनकर मनन करें।
(ग) सही ढंग से सुनने से ही समस्या सुलझ सकती है। .
प्रश्नः 6.
हम संवाद की आत्मा तक प्रायः क्यों नहीं पहुँच पाते?
उत्तरः
हम संवाद की आत्मा तक प्रायः इसलिए पहुँच नहीं पाते क्योंकि हम अपने समाधान देने के लिए उतावले होते हैं। इससे हम दूसरे की बात को समझ नहीं पाते।
प्रश्नः 7.
रहीम के कथन का आशय समझाइए।
उत्तरः
रहीम का कहना है कि लोग बात सुन लेते हैं, पर उन्हें बाँटता कोई नहीं। कहने का तात्पर्य है कि आम व्यक्ति अपनी ही बात कहना चाहता है।
2. जब समाचार-पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। यह सूचना नौकरियों से संबंधित हो सकती है, खाली मकान को किराये पर उठाने के संबंध में हो सकती है या किसी औषधि के प्रचार से संबंधित हो सकती है। कुछ लोग विज्ञापन के आलोचक हैं। वे इसे निरर्थक मानते हैं। उनका मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी जबकि खराब वस्तुएँ विज्ञापन की सहायता पाकर भी भंडाफोड़ होने पर बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएँगी, परंतु लोगों कि यह सोच ग़लत है।
आज के युग में मानव का प्रचार-प्रसार का दायरा व्यापक हो चुका है। अत: विज्ञापनों का होना अनिवार्य हो जाता है। किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। विज्ञापन ही वह शक्तिशाली माध्यम है जो हमारी ज़रूरत की वस्तुएँ प्रस्तुत करता है, उनकी माँग बढ़ाता है और अंततः हम उन्हें जुटाने चल पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करती है, उसे उत्पादक कहा जाता है। उन वस्तुओं और सेवाओं को ख़रीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य विज्ञापन करता है।
वह उत्पादक को उपभोक्ता के संपर्क में लाता है तथा माँग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। पुराने ज़माने में किसी वस्तु की अच्छाई का विज्ञापन मौखिक तरीके से होता था। काबुल का मेवा, कश्मीर की ज़री का काम, दक्षिण भारत के मसाले आदि वस्तुओं की प्रसिद्धि मौखिक रूप से होती थी। उस समय आवश्यकता भी कम होती थी तथा लोग किसी वस्तु के अभाव की तीव्रता का अनुभव नहीं करते थे। आज समय तेज़ी का है। संचार-क्रांति ने जिंदगी को गति दे दी है। मनुष्य की. आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं। इसलिए विज्ञापन मानव-जीवन की अनिवार्यता बन गया है।
प्रश्नः 1.
गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
उत्तरः
शीर्षक-विज्ञापन का महत्त्व।
प्रश्नः 2.
विज्ञापन किसे कहते हैं ? वह मानव जीवन का अनिवार्य अंग क्यों माना जाता है?
उत्तरः
समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित सूचना विज्ञापन कहलाती है। विज्ञापन के जरिए लोगों की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं तथा मानव का प्रचार-प्रसार का दायरा व्यापक हो चुका है। इसलिए वह मानव जीवन का अनिवार्य अंग माना जाता है।
प्रश्नः 3.
उत्पादक किसे कहते हैं ? उत्पादक-उपभोक्ता संबंधों को विज्ञापन कैसे प्रभावित करता है?
उत्तरः
वस्तु का निर्माण करने वाला व्यक्ति या कंपनी को उत्पादक कहा जाता है। विज्ञापन उत्पादक व उपभोक्ता को संपर्क में लाकर माँग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है।
प्रश्नः 4.
किसी विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? जीवन में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
उत्तरः
विज्ञापन का उद्देश्य वस्तुओं को प्रस्तुत करके माँग बढ़ाना है। इसके कारण ही हम खरीददारी करते हैं।
प्रश्नः 5.
पुराने समय में विज्ञापन का तरीका क्या था? वर्तमान तकनीकी युग ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया है?
उत्तरः
पुराने ज़माने में विज्ञापन का तरीका मौखिक था। उस समय आवश्यकता कम होती थी तथा वस्तु के अभाव की तीव्रता भी कम थी। आज तेज़ संचार का युग है। इसने मानव की ज़रूरत बढ़ा दी है।
प्रश्नः 6.
विज्ञापन के आलोचकों के विज्ञापन के संदर्भ में क्या विचार हैं?
उत्तरः
विज्ञापन के आलोचक इसे निरर्थक मानते हैं। उनका कहना है कि अच्छी चीज़ स्वयं ही लोकप्रिय हो जाती हैं जबकि खराब वस्तुएँ विज्ञापन का सहारा पाकर भी लंबे समय नहीं चलती।
प्रश्नः 7.
आज की भाग-दौड़ की ज़िन्दगी में विज्ञापन का महत्त्व उदाहरण देकर समझाइए।
उत्तरः
आज मानव का दायरा व्यापक हो गया है। उसके पास अधिक संसाधन है। विज्ञापन ही अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है।
3. राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और साँस लेते हैं-हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है।
जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है-देश को प्राथमिकता, भले ही हमें ‘स्व’ को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाषचन्द्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए तभी उसकी नीतियाँ-रीतियाँ राष्ट्रीय कही जा सकती हैं।
जब-जब भारत में फूट पड़ी, तब-तब विदेशियों ने शासन किया। चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत-तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहं में सिमटता जा रहा है। फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है।
प्रश्नः 1.
गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।
उत्तरः
शीर्षक-राष्ट्र और राष्ट्रीयता।
प्रश्नः 2.
‘स्व’ से क्या तात्पर्य है, उसे मिटाना क्यों आवश्यक है?
उत्तरः
‘स्व’ से तात्पर्य है-अपना। केवल अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति की दृष्टि संकुचित होती है। वह राष्ट्र का विकास नहीं कर सकता। अतः ‘स्व’ को मिटाना आवश्यक है।
प्रश्नः 3.
आशय स्पष्ट कीजिए-“राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है।”
उत्तरः
इसका अर्थ है कि राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। वह व्यक्तियों से बसा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर संस्कृति है, विचार है। वहाँ जीवनमूल्य स्थापित हो चुके होते हैं।
प्रश्नः 4.
राष्ट्रीयता से लेखक का क्या आशय है ? गद्यांश में चर्चित दो राष्ट्रभक्तों के नाम लिखिए।
उत्तरः
राष्ट्रीयता से लेखक का आशय है कि देश के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता व विकास के लिए काम करने की भवना होना। लेखक ने महात्मा गांधी व सुभाषचन्द्र बोस का नाम लिया है।
प्रश्नः 5.
राष्ट्रीय बोध को अभाव किन-किन रूपों में दिखाई देता है?
उत्तरः
आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भाषा के नाम पर तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर। इसके कारण व्यक्ति अपने अहं में सिमटता जा रहा है। अतः राष्ट्रीय बोध का अभाव दिखाई दे रहा है।
प्रश्नः 6.
राष्ट्र के उत्थान में व्यक्ति का क्या स्थान है? उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तरः
राष्ट्र के उत्थान में व्यक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जब व्यक्ति अपने अहं को त्याग कर देश के विकास के लिए कार्य करता है तो देश की प्रगति होती है। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाषचन्द्र बोस आदि के कार्यों से देश आजाद हुआ।
प्रश्नः 7.
व्यक्तिगत स्वार्थ एवं राष्ट्रीय भावना परस्पर विरोधी तत्व हैं। कैसे? तर्क सहित उत्तर लिखिए।
उत्तरः
व्यक्तिगत स्वार्थ एवं राष्ट्रीय भावना परस्पर विरोधी तत्व हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण मनुष्य अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के बारे में सोचता है, देश के बारे में नहीं। राष्ट्रीय भावना में ‘स्व’ का त्याग करना पड़ता है। ये दोनों प्रवृत्तियाँ एक साथ नहीं हो सकतीं।
4. भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है। यहाँ दान पुण्य को जीवनमुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान लेने वाले भी होंगे। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की ज़िम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु व सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व दान देना-दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। कुछ भिखारी खानदानी होते हैं क्योंकि पुश्तों से उनके पूर्वज धर्म स्थानों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं।
कुछ भिखारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जो देश में छोटी-सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा अनेक श्रेणी के और भी भिखारी होते हैं। कुछ भिखारी परिस्थिति से बनते हैं तो कुछ बना दिए जाते हैं। कुछ शौकिया भी। इस व्यवसाय में आ गए हैं। जन्मजात भिखारी अपने स्थान निश्चित रखते हैं। कुछ भिखारी अपनी आमदनी वाली जगह दूसरे भिखारी को किराए पर देते हैं। आधुनिकता के कारण अनेक वृद्ध मज़बूरीवश भिखारी बनते हैं।
गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख माँगने लगते हैं। काम न मिलना भी भिक्षावृत्ति को जन्म देता है। कुछ अपराधी बच्चों को उठा ले जाते हैं तथा उनसे भीख मँगवाते हैं। वे इतने हैवान हैं कि भीख माँगने के लिए बच्चों का अंग-भंग भी कर देते हैं। भारत में भिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। देवराज इंद्र व विष्णु श्रेष्ठ भिक्षुकों में थे। इंद्र ने कर्ण से अर्जुन की रक्षा के लिए उनके कवच व कुंडल ही भीख में माँग लिए। विष्णु ने वामन अवतार लेकर भीख माँगी।
धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई। पूजा-स्थल, तीर्थ, रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, गली-मुहल्ले आदि हर जगह भिखारी दिखाई देते हैं। इस कार्य में हर आयु का व्यक्ति शामिल है। साल-दो साल के दुध मुँहे बच्चे से लेकर अस्सी-नब्बे वर्ष के बूढ़े तक को भीख माँगते देखा जा सकता है। भीख माँगना भी एक कला है, जो अभ्यास या सूक्ष्म निरीक्षण से सीखी जा सकती है।
अपराधी बाकायदा इस काम की ट्रेनिंग देते हैं। भीख रोकर, गाकर, आँखें दिखाकर या हँसकर भी माँगी जाती है। भीख माँगने के लिए इतना आवश्यक है कि दाता के मन में करुणा जगे। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर दाता करुणामय होकर परंपरानिर्वाह कर पुण्य प्राप्त करता है।
प्रश्नः 1.
गद्यांश का समुचित शीर्षक दीजिए।
उत्तरः
शीर्षक-भिक्षावृत्ति एक व्यवसाय।
प्रश्नः 2.
“भारत में भिक्षा का इतिहास प्राचीन है”-सप्रमाण सिद्ध कीजिए।
उत्तरः
भारत में भिक्षावृत्ति का इतिहास पुराना है। देवराज इंद्र व विष्णु श्रेष्ठ भिक्षुकों में हैं। इंद्र ने अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से कवच व कुंडल की भिक्षा माँगी जबकि विष्णु ने वामन अवतार में भीख माँगी। धर्मशास्त्रों से भिक्षावृत्ति को धार्मिक मान्यता मिली।
प्रश्नः 3.
“भीख माँगना एक कला है”-इस कला के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए।
उत्तरः
भीख माँगना एक कला है जो अभ्यास व सूक्ष्म निरीक्षण से सीखी जाती है। रोकर, गाकर, आँखें दिखाकर या हँसकर, अपंगता, अशक्तता आदि के जरिए दूसरे के मन में करुणा जगाकर भीख माँगी जाती है।
प्रश्नः 4.
समाज में भिक्षावृत्ति बढ़ाने में हमारी मान्यताएँ किस प्रकार सहायक होती हैं ?
उत्तरः
भिक्षावृत्ति बढ़ाने में हमारी धार्मिक मान्यताएँ सहायक हैं। भारत में दान देना व लेना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। दान-पुण्य को जीवनमुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। अतः भिक्षुकों का होना लाजिमी है।
प्रश्नः 5.
भिखारी व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख कीजिए।
उत्तरः
भिखारी व्यवसाय में कुछ भिखारी खानदानी हैं जो कई पीढियों से धर्मस्थानों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय भिखारी हैं जो देश में छोटी-सी विपत्ति आने पर भीख माँगने विदेश चले जाते हैं। कुछ परिस्थितिवश तथा कुछ अपराधियों द्वारा बना दिए जाते हैं। कुछ शौकिया भिखारी भी होते हैं।
प्रश्नः 6.
भिखारी दाता के मन में किस भाव को जगाते हैं और क्यों?
उत्तरः
भिखारी अपनी अशक्तता, कुरूपता, अपंगता, वृद्धावस्था आदि के जरिए दाता के मन में करुणाभाव जगाते हैं ताकि वे दान देकर अपनी परंपरा का निर्वाह कर सकें।
प्रश्नः 7.
आपके विचार से भिक्षावृत्ति से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है?
उत्तरः
मेरे विचार से भिक्षावृत्ति से छुटकारा तभी मिल सकता है जब उसे धर्म के प्रभाव से अलग किया जाएगा। कानून व सामाजिक आंदोलन भी सहायक हो सकते हैं।
5. सभी मनुष्य स्वभाव से ही साहित्य-स्रष्टा नहीं होते, पर साहित्य-प्रेमी होते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही है सुंदर देखने का। घी का लड्डू टेढ़ा भी मीठा ही होता है, पर मनुष्य गोल बनाकर उसे सुंदर कर लेता है। मूर्ख-से-मूर्ख हलवाई के यहाँ भी गोल लड्डू ही प्राप्त होता है; लेकिन सुंदरता को सदा-सर्वदा तलाश करने की शक्ति साधना के द्वारा प्राप्त होती है। उच्छृखलता और सौंदर्य-बोध में अंतर है। बिगड़े दिमाग का युवक परायी बहू-बेटियों के घूरने को भी सौंदर्य-प्रेम कहा करता है, हालाँकि यह संसार की सर्वाधिक असुंदर बात है।
जैसा कि पहले ही बताया गया है, सुंदरता सामंजस्य में होती है और सामंजस्य का अर्थ होता है, किसी चीज़ का बहुत अधिक और किसी का बहुत कम न होना। इसमें संयम की बड़ी ज़रूरत है। इसलिए सौंदर्य-प्रेम में संयम होता है, उच्छृखलता नहीं। इस विषय में भी साहित्य ही हमारा मार्ग-दर्शक हो सकता है। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उसे दूसरे से भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य कुछ ऐसी जटिलताओं में आ फँसा है कि उसके भावों को ठीक-ठीक पहचानना हर समय सुकर नहीं होता।
ऐसी अवस्था में हमें मनीषियों के चिंतन का सहारा लेना पड़ता है। इस दिशा में साहित्य के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है और उसे मनुष्य पद का अधिकारी बने रहने के लिए साहित्य ही एकमात्र सहारा है। यहाँ साहित्य से हमारा मतलब उसकी सब तरह ही सात्त्विक चिंतन-धारा से है।
प्रश्नः 1.
गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
उत्तरः
शीर्षक-साहित्य और सौंदर्य-बोध। .
प्रश्नः 2.
साहित्य स्रष्टा और साहित्य प्रेमी से क्या तात्पर्य है?
उत्तरः
साहित्य स्रष्टा वे व्यक्ति होते हैं जो साहित्य का सृजन करते हैं। साहित्य प्रेमी साहित्य का आस्वादन करते हैं।
प्रश्नः 3.
लड्डू का उदाहरण क्यों दिया गया है?
उत्तरः
लेखक ने लड्डू का उदाहरण मनुष्य के सौंदर्य प्रेम के संदर्भ में दिया है। लड्डू की तासीर मीठी होती है चाहे वह गोल हो या टेढ़ा-मेढ़ा परंतु मनुष्य उन्हें गोल बनाकर उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है।
प्रश्नः 4.
उच्छृखलता और सौंदर्य-बोध में क्या अंतर है?
उत्तरः
उच्छंखलता में नियमों का पालन नहीं होता, जबकि सौंदर्य बोध में संयम होता है।
प्रश्नः 5.
लेखक ने संसार की सबसे बुरी बात किसे माना है और क्यों?
उत्तरः
लेखक ने संसार की सबसे बुरी बात परायी बहू-बेटियों को घूरना बताया है क्योंकि यह सौंदर्य बोध के नाम पर उच्छृखलता है।
प्रश्नः 6.
जीवन में संयम की ज़रूरत क्यों है?
उत्तरः
जीवन में संयम की ज़रूरत है क्योंकि संयम से ही सामंजस्य का भाव उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य दूसरों की भावना का आदर कर सकता है।
प्रश्नः 7.
हमें विद्वानों के चिंतन की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
उत्तरः
हमें विद्वानों के चिंतन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जीवन की जटिलताओं में फँसने के कारण हम दूसरे के भावों को सही से नहीं समझ पाते। साहित्य ही इस समस्या का समाधान है।
6. बड़ी कठिन समस्या है। झूठी बातों को सुनकर चुप हो कर रहना ही भले आदमी की चाल है, परंतु इस स्वार्थ और लिप्सा के जगत में जिन लोगों ने करोड़ों के जीवन-मरण का भार कंधे पर लिया है वे उपेक्षा भी नहीं कर सकते। ज़रा सी गफलत हुई कि सारे संसार में आपके विरुद्ध ज़हरीला वातावरण तैयार हो जाएगा। आधुनिक युग का यह एक बड़ा भारी अभिशाप है कि गलत बातें बड़ी तेजी से फैल जाती हैं।
समाचारों के शीघ्र आदान-प्रदान के साधन इस युग में बड़े प्रबल हैं, जबकि धैर्य और शांति से मनुष्य की भलाई के लिए सोचने के साधन अब भी बहुत दुर्बल हैं। सो, जहाँ हमें चुप होना चाहिए, वहाँ चुप रह जाना खतरनाक हो गया है। हमारा सारा साहित्य नीति और सच्चाई का साहित्य है। भारतवर्ष की आत्मा कभी दंगा-फसाद और टंटे को पसंद नहीं करती परंतु इतनी तेज़ी से कूटनीति और मिथ्या का चक्र चलाया जा रहा है कि हम चुप नहीं बैठ सकते।
अगर लाखों-करोड़ों की हत्या से बचना है तो हमें टंटे में पड़ना ही होगा। हम किसी को मारना नहीं चाहते पर कोई हम पर अन्याय से टूट पड़े तो हमें ज़रूर कुछ करना पड़ेगा। हमारे अंदर हया है और अन्याय करके पछताने की जो आदत है उसे कोई हमारी दुर्बलता समझे और हमें सारी दुनिया के सामने बदनाम करे यह हमसे नहीं सहा जाएगा। सहा जाना भी नहीं चाहिए। सो, हालत यह है कि हम सच्चाई और भद्रता पर दृढ़ रहते हैं और ओछे वाद-विवाद और दंगे-फसादों में नहीं पड़ते। राजनीति कोई अजपा-जाप तो है नहीं।
यह स्वार्थों का संघर्ष है। करोड़ों मनुष्यों की इज्जत और जीवन-मरण का भार जिन्होंने उठाया है वे समाधि नहीं लगा सकते। उन्हें स्वार्थों के संघर्ष में पड़ना ही पड़ेगा और फिर भी हमें स्वार्थी नहीं बनना है।
प्रश्नः 1.
गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
उत्तरः
शीर्षक-अन्याय का प्रतिकार।
प्रश्नः 2.
लेखक ने किसे कठिन समस्या माना है और क्यों?
उत्तरः
लेखक ने बताया है कि अफवाहों के दौर में शांत रहना बहुत कठिन है क्योंकि राजनीति अफवाहों के जरिए दंगे करवाती है। ऐसी स्थिति में संघर्ष अनिवार्य है।
प्रश्नः 3.
आधुनिक युग का अभिशाप किसे माना गया है और क्यों?
उत्तरः
आधुनिक युग का अभिशाप गलत बातों का तेजी से फैलना है क्योंकि गलत बात का प्रचार संचार साधन तेज़ी से करते हैं और भलाई के साधन सीमित है।
प्रश्नः 4.
चुप रहना कब खतरनाक होता है, कैसे?
उत्तरः
लेखक का मानना है कि गलत प्रचार पर चुप रहना खतरनाक होता है क्योंकि दंगा-फसाद आदि से लाखों की हत्या हो सकती है। अतः उनका विरोध करना अनिवार्य हो जाता है।
प्रश्नः 5.
भारतवर्ष की कोई एक विशेषता गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
उत्तरः
भारतवर्ष की विशेषता है कि वह दंगा-फसाद व टंटे को पसंद नहीं करता। वह स्वार्थ को दूर रखता है, परंतु अन्यायी को नष्ट करता है।
प्रश्नः 6.
लेखक ने संघर्ष करना क्यों आवश्यक माना है?
उत्तरः
लेखक ने संघर्ष को आवश्यक माना है, क्योंकि जन की हानि से बचने के लिए दुष्टों का अंत करना अनिवार्य है।
प्रश्नः 7.
आशय स्पष्ट कीजिए :
‘राजनीति कोई अजपा-जाप तो है नहीं।’
उत्तरः
इसका अर्थ है कि राजनीति सब कुछ नहीं है। यह स्वार्थों का संघर्ष है।
आरोह भाग 2 उषा
प्रश्न 1.
कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? (CBSE-2009, 2011, 2013, 2014)
अथवा
‘शमशेर की कविता गाँव की सुबह का जीवंत चित्रण है।’-पुष्टि कीजिए। (CBSE-2016)
उत्तर:
कवि ने गाँव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब-योजना की है। भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लिपे चौके के समान बताया गया है जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल-सा लगता है। कवि दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें गतिशीलता है।
प्रश्न 2.
भोर का नभ
राख से लीपा हुआ चौका
(अभी गीला पड़ा है)
नई कविता में कोष्ठक, विराम चिह्नों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है? समझाइए।
उत्तर:
नई कविता के लगभग सभी कवियों ने सदा कुछ विशेष कहना चाहा है अथवा कविता की विषयवस्तु को नए ढंग से प्रस्तुत करना चाहा है। उन्होंने इसके लिए कोष्ठक, विराम चिह्नों और पंक्तियों के बीच स्थान छोड़ दिया है। जो कुछ उन्होंने इसके माध्यम से कहा है, कविता उससे नए अर्थ देती है। उपरोक्त पंक्तियों में यद्यपि सुबह के आकाश को चौका जैसा माना है और यदि इसके कोष्ठक में दी गई पंक्ति को देखा जाए तो तब चौका जो अभी-अभी राख से लीपा है, उसका रंग मटमैला है। इसी तरह सुबह का आकाश भी दिखाई देता है।
अपनी रचना
अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्दचित्र खींचिए।
उत्तर:
सूर्योदय सूर्यास्त
सुबह का आकाश गोधूलि की वेला में
बहुत कुछ समुद्री जल जैसा सब कुछ धुंधला-सा हो जाता है।
सुबह आकाश कुछ कुछ ऐसा जैसे कि
मानो नए बोर्ड पर तवे का उत्तरार्ध
लिखे नए शब्दों जैसा बहुत कुछ ऐसा
और… जैसा कि काले अच्छर
धीरे-धीरे यह आवरण हट रहा है। धीरे-धीरे सारा परिवेश
तवे की तरह सुर्ख लाल गहन अंधेरे में जा रहा है।
सूर्य उदय होने को है। अब सूर्यास्त होगा।
आपसदारी
सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। प्रसाद की कविता ‘बीती विभावरी जाग री’ और अज्ञेय की ‘बावरा अहेरी’ की पंक्तियाँ आगे बॉक्स में दी जा रही हैं। ‘उषा’ कविता के समानांतर इन कविताओं को पढ़ते हुए नीचे दिए गए बिंदुओं पर तीनों कविताओं का विश्लेषण कीजिए और यह भी बताइए कि कौन-सी कविता आपको ज्यादा अच्छी लगी और क्यों?
शब्द चयन
| उपमान | परिवेश |
| बीती विभावरी जाग री! अंबर पनघट में डुबो रही तारा-घट ऊषा नागरी। खग-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई |
मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है आली} आँखों में भरे विहाग री – जयशंकर प्रसाद |
| भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल-लाल कनियाँ पर जब खींचता है जाल को बाँध लेता है सभी को साथः छोटी-छोटी चिड़ियाँ, मॅझोले परेवे, बड़े-बड़े पंखी डैनों वाले डील वाले डौल के बेडौल उड़ने जहाज़, |
कलस-तिसूल वाले मंदिर-शिखर से ले तारघर की नाटी मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली उपयोग-सुंदरी बेपनाह काया कोः गोधूली की धूल को, मोटरों के धुएँ को भी पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक-खची तन्वि रूप-रेखा को और दूर कचरा जलानेवाली कल की उदंड चिमनियों को, जो धुआँ यों उगलती हैं मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी। – सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ |
उत्तर:
सभी कविताओं को कवियों ने नए उपमान के द्वारा प्रस्तुत किया है। यदि प्रसाद जी ने पनघट, नागरी, खग, लतिका, नवल रस विहाग आदि उपमानों के माध्यम से प्रात:काल का वर्णन किया है तो अज्ञेय ने भोर को बावरा अहेरी, मंदिर, नाटी मोटी और चपटी गोल धूसे, गोधूली आदि उपमानों के द्वारा प्रस्तुत किया है। शमशेर बहादुर सिंह ने प्रात:काल के लिए नीले शंख, काला सिल, चौका, स्लेट, युवती आदि उपमानों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। उपमानों की तरह तीनों कवियों की शब्द योजना बिलकुल सटीक और सार्थक है।
तीनों ही कवियों ने साधारण बोलचाल के शब्दों का सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। तीनों कवियों ने सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया है। हमें शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ‘उषा’ शीर्षक की कविता सबसे अच्छी लगती है। कारण यही है कि ‘बावरी अहेरी’ और ‘बीती विभावरी जाग री’ शीर्षक कविताएँ उपमानों, शब्द योजना की दृष्टि से ‘उषा’ कविता की अपेक्षा कठिन प्रतीत होती है। ‘उषा’ कविता आम पाठक की समझ में शीघ्र आ जाती है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है?
उत्तर:
कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है। जिस प्रकार गीला चौका मटमैला और साफ़ होता है।
प्रश्न 2.
कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है?
उत्तर:
कवि ने नए-नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। ये उपमान सूर्य के उदय होने में सहायक हैं। कवि ने इनका प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते ही यह जादू टूट जाता है।
प्रश्न 3.
निम्नलिखित काव्यांश का भाव-सौंदर्य बताइए –
बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से
कि जैसे धुल गई हो।
उत्तर:
कवि कहता है कि जिस प्रकार ज्यादा काली सिर अर्थात् पत्थर पर थोड़ा-सा केसर डाल देने से वह धुल जाती है अर्थात् उसका कालापन खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार काली सिर को किरण रूपी केसर धो देता है अर्थात् सूर्योदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है।
प्रश्न 4.
‘उषा’ कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए।
उत्तर:
कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लीपा गया हो तथा वह अभी गीला हो। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ होता है, उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता।
प्रश्न 5.
‘उषा’ कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों ?
उत्तर:
‘उषा’ कविता में प्रात:कालीन नभ की तुलना राख से लीपे गए गीले चौके से की है। इस समय आकाश नम तथ धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूखकर साफ़ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है।
कवितावली (उत्तर कांड से), लक्ष्मण-मूच्छ और राम का विलाप
प्रश्न 1.
कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। (CBSE-2010, 2015)
अथवा
‘कवितावली’ के आधार पर पुष्टि कीजिए कि तुलसी को अपने समय की आर्थिक-सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। (CBSE-2016)
उत्तर:
‘कवितावली’ में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वगों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसी दास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत-सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था।
प्रश्न 2.
पेट की आग का शमन ईश्वर ( राम ) भक्ति का मेघ ही कर सकता है—तुलसी का यह काव्य-सत्य क्या इस समय का भी युग-सत्य है? तुर्क संगत उत्तर दीजिए।
उत्तर:
जब पेट में आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उलटा अथवा बुरा कार्य करता है, किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का शमन हो सकता है क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकने की क्षमता रखता है।
प्रश्न 3.
तुलसी ने यह कहने की ज़रूरत क्यों समझी? धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूतु कहौ, जोलहा कहौ कोऊ/काहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सोऊ। इस सवैया में काहू के बेटासों बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आती?
उत्तर:
तुलसीदास के युग में जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो गए थे। तुलसी के संबंध में भी समाज ने उनके कुल व जाति पर प्रश्नचिहन लगाए थे। कवि भक्त था तथा उसे सांसारिक संबंधों में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना। इससे किसी की जाति खराब नहीं होगी क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के वर ढूँढ़ता है। पुरुष-प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल जाती है। तुलसी इस सवैये में अगर अपनी बेटी की शादी की बात करते तो संदर्भ में बहुत अंतर आ जाता। इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती। दूसरे, समाज में लड़की का विवाह न करना गलत समझा जाता है। तीसरे, तुलसी बिना जाँच के अपनी लड़की की शादी करते तो समाज में जाति-प्रथा पर कठोर आघात होता। इससे सामाजिक संघर्ष भी बढ़ सकता था।
प्रश्न 4.
धूत कहौ ….. वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? (CBSE-2013, 2014, 2017)
उत्तर:
तुलसीदास का जीवन सदा अभावों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जगाए रखा। इसी प्रकार के भाव उनकी भक्ति में भी आए हैं। वे राम के सामने गिड़गिड़ाते नहीं बल्कि जो कुछ उनसे प्राप्त करना चाहते हैं वह भक्त के अधिकार की दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्वाभिमानी भक्ति का परिचय देते हुए राम से यही कहा है कि मुझ पर कृपा करो तो भक्त समझकर न कि कोई याचक या भिखारी समझकर।।
प्रश्न 5.
व्याख्या करें
(क) मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता।
जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पितु बचन मनतेउँ नहिं ओहू॥
(ख) जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिबर कर हीना।
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जौं जड़ दैव जिआवै मोही॥
(ग) माँग के खैबो, मसीत को सोइबो, लैबोको एकु ने दैबको दोऊ॥
(घ) ऊँचे नीचे करम, धरम-अधरम करि, पेट को ही पचत, बेचत बेटा-बेटकी॥
उत्तर:
(क) लक्ष्मण के मूर्चिछत होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे हित के लिए माता-पिता का त्याग कर दिया और वनवास स्वीकार किया। तुमने वन में रहते हुए सर्दी, धूप, आँधी आदि सहन किया। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊँगा तो मैं पिता की बात नहीं मानता और न ही तुम्हें अपने साथ लेकर वन आता। राम लक्ष्मण की नि:स्वार्थ सेवा को याद कर रहे हैं।
(ख) मूर्चिछत लक्ष्मण को गोद में लेकर राम विलाप कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे पंखों के बिना पक्षी की, मणि के बिना साँप की और सँड़ के बिना हाथी की स्थिति दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में मैं अक्षम व असहाय हो गया हूँ। यदि भाग्य ने तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन इसी तरह शक्तिहीन रहेगा। दूसरे शब्दों में, मेरे तेज व पराक्रम के पीछे तुम्हारी ही शक्ति कार्य करती रही है।
(ग) तुलसीदास ने समाज से अपनी तटस्थता की बात कही है। वे कहते हैं कि समाज की बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे किसी पर आश्रित नहीं हैं वे मात्र राम के सेवक हैं। जीवन-निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति करते हैं तथा मस्जिद में सोते हैं। उन्हें संसार से कोई लेना-देना नहीं है।
(घ) तुलसीदास ने अपने समय की आर्थिक दशा का यथार्थपरक चित्रण किया है। इस समय लोग छोटे-बड़े, गलतसही सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भूख मिटानी है। वे कर्म की प्रवृत्ति व तरीके की परवाह नहीं करते। पेट की आग को शांत करने के लिए वे अपने बेटा-बेटी अर्थात संतानों को भी बेचने के लिए विवश हैं अर्थात पेट भरने के लिए व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है।
प्रश्न 6.
भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।
उत्तर:
जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम एकदम विह्वल हो उठे। वे ऐसे रोए जैसे कोई बालक पिता से बिछुड़कर होता है। सारी मानवीय संवेदनाएँ उन्होंने प्रकट कर दीं। जिस प्रकार मानव-मानव के लिए रोता है ठीक वैसा ही राम ने किया। राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मानव में अपेक्षित सारी अनुभूतियाँ इस शोक सभा में दिखाई देती हैं।
प्रश्न 7.
शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है?
उत्तर:
हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में देर हो रही थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर थी। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार कर के लक्ष्मण को पिलाई तथा लक्ष्मण ठीक हो गए। लक्ष्मण के उठने से राम का शोक समाप्त हो गया और सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण स्वयं उत्साही वीर थे। उनके आ जाने से सेना का खोया पराक्रम प्रगाढ़ होकर वापस आ गया। इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठाकर लाने से शोक-ग्रस्त माहौल में वीर रस का आविर्भाव हो गया था।
प्रश्न 8.
“जैहउँ अवध कवन मुहुँ लाई । नारि हेतु प्रिय भाइ गॅवाई॥
बरु अपजस सहतेउँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं॥
भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप-वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है?
उत्तर:
इस वचन में नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। राम ने अपनी पत्नी के खो जाने से बढ़कर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने को महत्त्व दिया है। उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि नारी के लिए मैंने भाई खो दिया है यह सबसे बड़ा कलंक है। यदि नारी खो जाए तो उसके खो जाने से कोई बड़ी हानि नहीं होती। नारी से बढ़कर तो भाई-बंधु हैं जिनके कारण व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, यदि वही खो जाए तो माथे पर जीवनभर के लिए कलंक लग जाता है।
पाठ के आसपास
प्रश्न 1.
कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी (इंदुमती) के मृत्यु-शोक पर ‘अज’ तथा निराला की ‘सरोज-स्मृति’ में पुत्री (सरोज) के मृत्यु-शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। उनसे भ्रातृशोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें।
उत्तर:
‘सरोज-स्मृति’ में कवि निराला ने अपनी पुत्री की मृत्यु पर उद्गार व्यक्त किए थे। ये एक असहाय पिता के उद्गार थे जो अपनी पुत्री की आकस्मिक मृत्यु के कारण उपजे थे। भ्रातृशोक में डूबे राम का विलाप निराला की तुलना में कम है। लक्ष्मण अभी सिर्फ़ मूर्चिछत ही हुए थे। उनके जीवित होने की आशा बची हुई थी। दूसरे, सरोज की मृत्यु के लिए निराला की कमजोर आर्थिक दशा जिम्मेदार थी। वे उसकी देखभाल नहीं कर पाए थे, जबकि राम के साथ ऐसी समस्या नहीं थी।
प्रश्न 2.
‘पेट ही को पचत, बेचते बेटा-बेटकी’ तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों (खासकर बेटियों) को भी बेच डालने की हृदयविदारक घटनाएँ हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। (CBSE-2013)
उत्तर:
भुखमरी की स्थिति बहुत दयनीय होती है। व्यक्ति भुखमरी की इस दयनीय स्थिति में हर प्रकार का नीच कार्य करता है। कर्ज लेता है, बेटा-बेटी तक को बेच देता है। जब कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है तो आत्महत्या तक कर लेता है। तुलसी का समाज भी लगभग वैसा ही था जैसा कि आज का भारतीय मध्यवर्गीय समाज। उस समय की परिस्थिति भी बहुत भयानक थी। लोगों के पास कमाने का कोई साधन न था ऊपर से अकाल ने लोगों को भुखमरी के किनारे तक पहुँचा दिया। इस स्थिति से तंग आकर व्यक्ति वे सभी अनैतिक कार्य करने लगे। बेटा-बेटी का सौदा करने लगे। यदि साहूकार का ऋण नहीं उतरता है तो स्वयं मर जाते थे। ठीक यही परिस्थिति हमारे समाज की है। किसान कर्ज न चुकाने की स्थिति में आत्महत्याएँ कर रहे हैं। कह सकते हैं कि तुलसी का युग और आज का युग एक ही है। आर्थिक दृष्टि से दोनों युगों में विषमताएँ रहीं।
प्रश्न 3.
तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं? आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचर्चा करें।
उत्तर:
तुलसी के युग में बेकारी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं-
- खेती के लिए पानी उपलब्ध न होना।
- बार-बार अकाल पडना।
- अराजकता।
- व्यापार व वाणिज्य में गिरावट।
आज बेकारी के कारण पहले की अपेक्षा भिन्न हैं-
- भ्रष्टाचार।
- शारीरिक श्रम से नफ़रत करना।
- कृषि-कार्य के प्रति अरुचि।
- जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा तथा अकुशलता।
नमक
प्रश्न 1.
सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? (CBSE-2009, 2013)
उत्तर:
नमक की पुड़िया को लेकर सफ़िया के मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए या चोरी से छिपाकर। सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंधित था। यह गैर-कानूनी था। दूसरे, कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान की भी चिंदी-चिंदी बिखेर देंगे। इससे बदनामी भी होगी। तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक है।
प्रश्न 2.
नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था? (CBSE-2012, 2015, 2017)
उत्तर:
जब भावना के बदले बुद्धि हावी होने लगी तो सफ़िया का मन द्वंद्व ग्रस्त हो गया। वह सोचने लगी कि कस्टम वाले पुड़िया ले जाने देंगे या नहीं। यदि उन्होंने उसे न जाने दिया तो उसके वायदे का क्या होगा। वही वायदा जो उसने सिख बीबी से किया। सफ़िया जोकि सैयद थी, इसलिए उसने सोचा कि यदि वह नमक न ले गई तो क्या होगा, क्योंकि सैयद लोग कभी भी वायदा नहीं तोड़ते। जान देकर भी यह वायदा पूरा करना होगा।
प्रश्न 3.
जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफ़िसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे?
उत्तर:
सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो इधर कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सिख बीवी का प्रसंग छिड़ने पर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी। वे सिख बीवी व सफ़िया की भावना से भी प्रभावित थे। उन्हें दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीजें बहुत याद आ रही थीं। राजनीतिक उद्देश्यों ने सबको एक-दूसरे से अलग कर दिया।
प्रश्न 4.
लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार. किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं?
उत्तर:
इन उद्गारों से यही स्पष्ट होता है कि चाहे राजनीति या भूगोल देश की सीमाओं को बाँट दे अथवा देश को टुकड़ों में बाँट दे लेकिन लोगों के मन को नहीं अलग किया जा सकता। लोगों का मन किसी भी तरह से इस बँटवारे को नहीं स्वीकारता । एक पाकिस्तानी को दिल्ली प्यारी है तो एक हिंदुस्तानी को लाहौर प्यारा है।
प्रश्न 5.
नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। (CBSE-2011)
उत्तर:
नमक ले जाते समय सफ़िया के मन में अनेक द्वंद्व उठे। इससे उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ उभरकर आती हैं-
(i) भावुक-सफ़िया भावुक है। वह सिख बीवी की भावनाओं को मानती है तथा उसी के आधार पर लाहौरी नमक भारत ले जाना चाहती है। यह गैर-कानूनी है, यह जानते हुए भी वह भावनाओं को बड़ा मानती है।
(ii) वायदे की पक्की-सफ़िया सैयद है। सैयद होने के नाते वह अपने वायदे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। वह नमक ले जाने के लिए हर गलत-सही तरीके पर विचार करती है।
(iii) व्यावहारिक-सफ़िया व्यावहारिक है। वह प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती। वह दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती है तथा अपने तकों से उन्हें अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है। इस तरीके से वह नमक की पुड़िया लाने में सफल होती है।
प्रश्न 6.
मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से ज़मीन और जनता बँट नहीं जाती है-उचित तर्को व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। (CBSE-2008, 2011, 2014)
उत्तर:
राजनीति और कूटनीति के चलते देश के टुकड़े हो जाते हैं। देश कई टुकड़ों में बँट जाता है। भारत भी कूटनीति का शिकार रहा है। भारत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के कारण तीन टुकड़ों में बँटा हुआ है लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि लोगों के दिलों में किसी भी प्रकार की दरार (लकीर) नहीं खिंची है। लोग आज भी एक-दूसरे से मिलते हैं। उनमें वही भाईचारा और प्यार कायम है। हिंदुस्तान में इन दोनों देशों के नागरिक आते-जाते हैं। यहाँ से नागरिक इन देशों में जाते हैं। वे एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं।
प्रश्न 7.
‘नमक’ कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मुहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है, कैसे? (CBSE-2010, 2011)
उत्तर:
नमक’ कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मुहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। उनमें प्रेम और स्नेह का स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। लेखिका का अपने भाइयों, परिचितों से स्नेह, सिख बीवी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव-ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं।
क्यों कहा गया?
प्रश्न 1.
क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मुहब्बत मुरौवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते?
उत्तर:
सफ़िया ने यह बात इसलिए कही है कि सब कानूनों से ऊपर है इंसानियत। इंसानियत से ही सारी बातें जन्म लेती हैं। कानून हुकूमत के हो सकते हैं लेकिन इंसानियत तो प्रेम और भाईचारे का कानून सिखाता है। जिस आदमी में इंसानियत नहीं है वह पशु है, जानवर है।
प्रश्न 2.
भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे-धीरे उस पर हावी हो रही थी।
उत्तर:
सफ़िया के भाई ने कानूनी पक्ष बताकर नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए मना कर दिया था। उस समय वह भाई पर बिगड़ी और इंसानियत, प्रेम आदि की दुहाई दी। पर जब गुस्सा उतर गया तो उसने पुड़िया ले जाने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अनेक विकल्प सोचे, परंतु हर बार कानून का डर सामने आया। अंत में उसने इसे टोकरी में कीनुओं के नीचे छिपाकर ले जाने का निर्णय किया।
प्रश्न 3.
मुहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुज़र जाती है कि कानून हैरान रह जाता है।
उत्तर:
ये शब्द कस्टम अधिकारी ने कहे। उसने सफ़िया से कहा कि कानून अपनी जगह है लेकिन मुहब्बत के आगे कानून की भी नहीं चलती। जब मुहब्बत आगे आड़े आ जाए तो कानून धरे रह जाते हैं। वास्तव में इस दुनिया में इंसानियत सब कानूनों से परे हैं।
प्रश्न 4.
हमारी जमीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है!
उत्तर-
भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन मानते हैं। लेखिका की पूरी बात सुनकर उन्हें अपनी जमीन, डाभ आदि की याद आती है। वे भावुक हो उठते हैं और यह बात कहने लगते हैं।
पहलवान की ढोलक
प्रश्न 1.
कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्ट्टन के दाँव-पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए।
उत्तर:
कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाँव-पेंच में अद्भुत तालमेल था। ढोल बजते ही लुट्टन की रगों में खून दौड़ने लगता था। उसे हर थाप में नए दाँव-पेंच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज उसे साहस प्रदान करती थी। ढोल की आवाज और लुट्टन के दाँव-पेंच में निम्नलिखित तालमेल था
- धाक-धिना, तिरकट तिना – दाँव काटो, बाहर हो जाओ।
- चटाक्र-चट्-धा – उठा पटक दे।
- धिना-धिना, धिक-धिना — चित करो, चित करो।
- ढाक्र-ढिना – वाह पट्ठे।
- चट्-गिड-धा – मत डरना। ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं।
प्रश्न 2.
कहानी के किस-किस मोड़ पर लुटेन के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए? (CBSE-2008)
उत्तर:
लुट्न पहलवान का जीवन उतार-चढ़ावों से भरपूर रहा। जीवन के हर दुख-सुख से उसे दो-चार होना पड़ा। सबसे पहले उसने चाँद सिंह पहलवान को हराकरे राजकीय पहलवान का दर्जा प्राप्त किया। फिर काला खाँ को भी परास्त कर अपनी धाक आसपास के गाँवों में स्थापित कर ली। वह पंद्रह वर्षों तक अजेय पहलवान रहा। अपने दोनों बेटों को भी उसने राजाश्रित पहलवान बना दिया। राजा के मरते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विलायत से राजकुमार ने आते ही पहलवान और उसके दोनों बेटों को राजदरबार से अवकाश दे दिए। गाँव में फैली बीमारी के कारण एक दिन दोनों बेटे चल बसे। एक दिन पहलवान भी चल बसा और उसकी लाश को सियारों ने खा लिया। इस प्रकार दूसरों को जीवन संदेश देने वाला पहलवान स्वयं खामोश हो गया।
प्रश्न 3.
लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? (CBSE-2008, 2009)
उत्तर:
पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना और एकलव्य की भाँति हमेशा उसी की आज्ञा का अनुकरण करता रहा। ढोल को ही उसने अपने बेटों का गुरु बनाकर शिक्षा दी कि सदा इसको मान देना। ढोल लेकर ही वह राज-दरबार से रुखसत हुआ। ढोल बजा-बजाकर ही उसने अपने अखाड़े में बच्चों-लड़कों को शिक्षा दी, कुश्ती के गुर सिखाए। ढोल से ही उसने गाँव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी शक्ति प्रदान की थी। ढोल के सहारे ही बेटों की मृत्यु का दुख पाँच दिन तक दिलेरी से सहन किया और अंत में वह भी मर गया। यह सब देखकर लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का संबल, जीवन-साथी ही था।
प्रश्न 4.
गाँव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? (CBSE-2009, 2011, 2015)
उत्तर:
ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों में जीने की इच्छा जाग उठती थी। पहलवान नहीं चाहता था कि उसके गाँव का कोई आदमी अपने संबंधी की मौत पर मायूस हो जाए। इसलिए वह ढोल बजाता रहा। वास्तव में ढोल बजाकर पहलवान ने अन्य ग्रामीणों को जीने की कला सिखाई। साथ ही अपने बेटों की अकाल मृत्यु के दुख को भी वह कम करना चाहता था।
प्रश्न 5.
ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था। (CBSE-2008, 2012, 2015)
अथवा
पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है? (CBSE-2013)
उत्तर
महामारी की त्रासदी से जूझते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। यह आवाज बूढ़े-बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी। उनकी स्पंदन शक्ति से शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। ठीक है कि ढोलक की आवाज में बुखार को दूर करने की ताकत न थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आँखें मूंदते समय कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गाँव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती थी।
प्रश्न 6.
महामारी फैलने के बाद गाँव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? (CBSE-2008)
उत्तर:
महामारी ने सारे गाँव को बुरी तरह से प्रभावित किया था। लोग सुर्योदय होते ही अपने मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गाँव के श्मशान की ओर जाते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। सूर्यास्त होते ही सारे गाँव में मातम छा जाता था। किसी न किसी बच्चे, बूढ़े अथवा जवान के मरने की खबर आग की तरह फैल जाती थी। सारा गाँव श्मशान घाट बन चुका था।
प्रश्न 7.
कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा
विशेष सम्मान दिया जाता था।
(क) ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है?
(ख) इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है?
(ग) कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या-क्या कार्य किए जा सकते हैं?
उत्तर:
(क) कुश्ती या दंगल पहले लोगों व राजाओं के प्रिय शौक हुआ करते थे। राजा पहलवानों को सम्मान देते थे, परंतु आज स्थिति बदल गई है। अब पहले की तरह राजा नहीं रहे। दूसरे, मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गए हैं।
(ख) कुश्ती की जगह अब अनेक आधुनिक खेल प्रचलन में हैं; जैसे-क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल आदि।
(ग) कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा सकती साथ-साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण तथा कुश्ती को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का सहयोग लिया जा सकता है।
प्रश्न 8.
आंशय स्पष्ट करें आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हँस पड़ते थे।
उत्तर:
लेखक ने इस कहानी में कई जगह प्रकृति का मानवीकरण किया है। यह गद्यांश भी प्रकृति का मानवीकरण ही है। यहाँ लेखक के कहने का आशय है कि जब सारा गाँव मातम और सिसकियों में डूबा हुआ था तो आकाश के तारे भी गाँव की दुर्दशा पर आँसू बहाते प्रतीत होते हैं। क्योंकि आकाश में चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। यदि कोई तारा अपने मंडल से टूटकर पृथ्वी पर फैले दुख को बाँटने आता भी था तो वह रास्ते में विलीन (नष्ट) हो जाता था। अर्थात् वह पृथ्वी तक पहुँच नहीं पाता था। अन्य सभी तारे उसकी इस भावना को नहीं समझते थे। वे तो केवल उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हँस देते थे।
प्रश्न 9.
पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
मानवीकरण के अंश
- औधेरी रात चुपचाप आँसू बहा रही थी।
आशय-रात का मानवीकरण किया गया है। ठंड में ओस रात के आँसू जैसे प्रतीत होते हैं। वे ऐसे लगते हैं मानो गाँव वालों की पीड़ा पर रात आँसू बहा रही है। - तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हँस पड़ते थे। आशय-तारों को हँसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है। वे मजाक उड़ाते प्रतीत होते हैं।
- ढोलक लुढ़की पड़ी थी। आशय-यहाँ पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। पहलवान व ढोलक का गहरा संबंध है। ढोलक का बजना पहलवान के जीवन का पर्याय है।
रुबाइयाँ, गज़ल
प्रश्न 1.
शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है?
उत्तर:
शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय आकाश में घटाएँ छाई होती हैं तथा उनमें बिजली भी चमकती है। राखी के लच्छे बिजली कौधने की तरह चमकते हैं। बिजली की चमक सत्य को उद्घाटित करती है तथा राखी के लच्छे रिश्तों की पवित्रता को व्यक्त करते हैं। घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है।
प्रश्न 2.
खुद का परदा खोलने से क्या आशय है?
उत्तर:
परदा खोलने से आशय है – अपने बारे में बताना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है या बुराई करता है। तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है। इसीलिए शायर ने कहा कि मेरा परदा खोलने वाले अपना परदा खोल रहे हैं।
प्रश्न 3.
किस्मत हमको रो लेवे है हम किस्मत को रो ले हैं – इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए।
उत्तर:
कवि अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहा। किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह अत्यधिक निराश हो जाता है। वह अपनी बदकिस्मती के लिए खीझता रहता है। दूसरे, कवि कर्महीन लोगों पर व्यंग्य करता है। कर्महीन लोग असफलता मिलने पर भाग्य को दोष देते हैं और किस्मत उनकी कर्महीनता को दोष देती है।
प्रश्न 4.
टिप्पणी करें।
(क) गोदी के चाँद और गगन के चाँद का रिश्ता।
(ख) सावन की घटाएँ व रक्षाबंधन का पर्व।
उत्तर:
(क) गोदी के चाँद से आशय है – बच्चा और गगन के चाँद से आशय है – आसमान में निकलने वाला चाँद। इन दोनों में गहरा और नजदीकी रिश्ता है। दोनों में कई समनाताएँ हैं। आश्चर्य यह है कि गोदी का चाँद गगन के चाँद को पकड़ने के लिए उतावला रहता है तभी तो सूरदास को कहना पड़ा ”मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों।”
(ख) रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार सावन के महीने में आता है। सावन की घटाएँ जब घिर आती हैं तो चारों ओर खुशी की बयार बहने लगती है। राखी का यह त्यौहार इस मौसम के द्वारा और अधिक सार्थक हो जाता है। सावन की काली-काली घटाएँ भाई को संदेश देती हैं कि तेरी बहन तुझे याद कर रही है। यदि तू इस पवित्र त्यौहार पर नहीं गया तो उसकी आँखों से मेरी ही तरह बूंदें टपक पड़ेगी।
कविता के आसपास
प्रश्न 1.
इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोकभाषा के मिले-जुले प्रयोग को छाँटिए।
उत्तर:
हिंदी के प्रयोग-
- आँगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी
हाथों में झुलाती है उसे गोद-भरी - गूँज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हँसी
- किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को
- दीवाली की शाम घर पुते और सजे
- रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली
- छायी है घटा गगन की हलकी-हलकी
- बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे
- भाई के है बाँधती चमकती राखी
उर्दूके प्रयोग-
- उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके
- देख आईने में चाँद उतर आया है
लोकभाषा के प्रयोग-
- रह-रह के हवा में जो लोका देती है।
- जब घुटनियों में ले के है पिन्हाती कपड़े
- आँगन में दुनक रहा है जिदयाया है
- बालक तो हई चाँद पै ललचाया है
आपसदारी
प्रश्न 1.
कविता में एक भाव, एक विचार होते हुए भी उसका अंदाजे बयाँ या भाषा के साथ उसका बर्ताव अलग-अलग रूप में अभिव्यक्ति पाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए और दी गई फ़िराक की गज़ल-रूबाई में से समानार्थी पंक्तियाँ ढूंढ़िए
(क) मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों। -सूरदास
(ख) वियोगी होगा पहला कवि उमड़ कर आँखों से चुपचाप
आह से उपजा होगा गान बही होगी कविता अनजान -सुमित्रानंदन पंत
(ग) सीस उतारे भुईं धरे तब मिलिहैं करतार -कबीर
उत्तर:
(क) आँगन में तुनक रहा है जिदयाया है।
बालक तो हई चाँद पै ललचाया है।
(ख) आबो ताबे अश्आर न पूछो तुम भी आँखें रक्खो हो
ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं।
ऐसे में तू याद आए हैं अंजमने मय में रिंदो को,
रात गए गर्दै पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं।
(ग) “ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती-ए-होशो हवास
तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होलें हैं।”
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
बच्चे की हँसी सबसे ज्यादा कब पूँजी है?
उत्तर:
जब माँ अपने बच्चे को उछाल-उछाल कर प्यार करती है तो बच्चे की हँसी सबसे ज्यादा पूँजती है। बच्चा खुले वातावरण में आकर बहुत खुशी महसूस करता है। जब वह ऊपर की ओर बार-बार उछलता है तो वह रोमांचित हो उठता है।
प्रश्न 2.
माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है?
उत्तर:
माँ बच्चे को छलकते हुए निर्मल और स्वच्छ पानी से नहलाती है। उसके बालों में प्यार से कंघी करती है। उसे कपड़े पहनाती है। यह सारे कार्य देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। वह ठंडे पानी से नहाकर ताजा महसूस करता है। अपनी माँ को प्यार से देखता है।
प्रश्न 3.
बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन जाता है?
उत्तर:
बच्चा जब चाँद को देखता है तो उसका मन लालची हो जाता है। वह चाँद को पकड़ने की जिद करता है। वह माँ से कहता है कि मुझे यही वस्तु चाहिए। चाँद को देखते ही उसका मन लालच से भर जाता है।
प्रश्न 4.
क्या शायर भाग्यवादी है?
उत्तर:
शायर बिलकुल भी भाग्यवादी नहीं है। उसे अपने भाग्य पर बिलकुल भरोसा नहीं। वह तो कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों मिलकर रोते हैं। वह मुझ पर रोती है और मैं उस पर रो लेता हूँ। दोनों परस्पर विरोधी हैं। इसलिए कह सकते हैं। कि शायर भाग्यवादी नहीं कर्मवादी है। भाग्य की अपेक्षा उसे अपने कर्म पर विश्वास है।
प्रश्न 5.
इश्क की फितरत को शायर ने क्या बताया है?
उत्तर:
इश्क की फितरत अर्थात् आदत है कि इससे व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति जितना पाता है उतना ही नँवा भी देता है। इसलिए इश्क में कुछ पा लेना संभव ही नहीं है। किसी ने आज तक इश्क में कुछ भी नहीं पाया केवल खोया ही है। अपना चैन आँवाया है।
प्रश्न 6.
फिराक गोरखपुरी की भाषा-शैली पर विचार करें।
उत्तर:
फिराक गोरखपुरी मूलत: शायर हैं। रुबाइयाँ भी उन्होंने लिखी हैं। इन सबके लिए उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। खास बात यह है कि इनकी भाषा में कठिनाई नहीं है। हाँ, कुछ शब्द उलझाव पैदा करते हैं, लेकिन वे पाठक को कठिन नहीं लगते।
प्रश्न 7.
गोरखपुरी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालें।
उत्तर:
फिराक ने कई अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इसलिए उनकी रुबाइयों और गजलों में अलंकारों का प्रयोग थोपा हुआ नहीं लगता। ये भावों और प्रसंगों के अनुकूल इनमें आए हैं। शायर ने मुख्य रूप से रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया है।
प्रश्न 8.
गोरखपुरी की रुबाइयों के कला पक्ष के बारे में बताएँ।
उत्तर:
गोरखपुरी की रूबाइयाँ कलापक्ष की दृष्टि से बेहतरीन बन पड़ी हैं। भाषा सहज, सरल और प्रभावी हैं। भावानुकूल शैली का प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दावली के साथ-साथ शायर ने देशज संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविक ढंग से किया है। लोका, पिन्हाती, पुते, लावे आदि शब्दों के प्रयोग से उनकी रुबाइयाँ अधिक प्रभावी बन पड़ी हैं।
प्रश्न 9.
रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छायी है घटा गगन की हलकी-हलकी बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के हैं बाँधती चमकती राखी”-इस रुबाई का कला सौंदर्य स्पष्ट करें।
उत्तर:
भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली है। शायर ने उर्दू शब्दों के साथ-साथ देशज शब्दों का भावानुकूल प्रयोग किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है।
प्रश्न 10.
काव्य-सौंदर्य स्पष्ट करें-
आँगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ीं
हाथों पे झुलाती है उसे गोद-भरी
रह-रह के हवा में जो लोका देती है
गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हँसी।
उत्तर:
कवि बताता है कि माँ अपने चाँद जैसे बच्चे को आँगन में लिए खड़ी है। वह हाथों के झूले में झुला रही है। वह उसे हवा में धीरे-धीरे उछाल रही है। इस काम से बच्चे की हँसी गूंज उठती है। ‘चाँद के टुकड़े’ में उपमा अलंकार है। ‘रहरह’ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बालसुलभ चेष्टाओं का वर्णन है। उर्दू मिश्रित शब्दावली है। गेयता है। दृश्य बिंब है। भाषा सहज व सरल है। उर्दू भाषा है।
प्रश्न 11.
फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।
अथवा
‘फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप की स्वाभाविकता और सात्विकता के अनूठे चित्र चित्रित हुए हैं’ – पाठ्यपुस्तक में संग्रहीत रुबाइयों के आधार पर उत्तर दीजिए। (CBSE-2013)
उत्तर:
फिराक की रुबाइयों में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। माँ अपने शिशु को आँगन में लिए खड़ी है। वह उसे झुलाती है। बच्चे को नहलाने का दृश्य दिल को छूने वाला है। दीवाली व रक्षाबंधन पर जिस माहौल को चित्रित किया गया है। वह आम जीवन से जुड़ा हुआ है। बच्चे का किसी वस्तु के लिए जिद करना तथा उसे किसी तरह बहलाने के दृश्य सभी परिवारों में पाए जाते हैं।







 Profile
Profile Signout
Signout



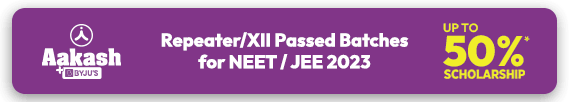










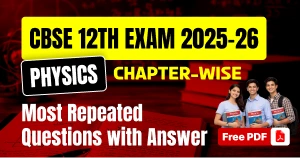

 Quiz
Quiz
 Get latest Exam Updates
Get latest Exam Updates 










