JAC Board 12th Accountancy Exam 2025 : Most Important ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ - परीक्षा से पहले रटलो
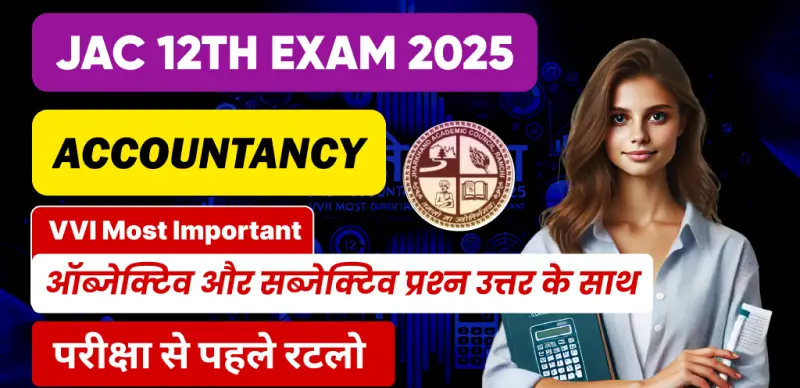
SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
JAC बोर्ड कक्षा 12 अकाउंटेंसी परीक्षा 20 फरवरी 2025 को होगी। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का संकलन यहां दिया गया है। यह प्रश्न बैंक पिछले वर्षों के पेपर और विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा सवालों पर आधारित है।
ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में MCQs, Fill in the Blanks और सही-गलत प्रकार के सवाल शामिल हैं, जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। वहीं, सब्जेक्टिव प्रश्नों में 2, 3, 5 और 8 अंकों के विस्तृत उत्तर सहित महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। इससे परीक्षा पैटर्न को समझने और बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी।
अच्छे अंक पाने के लिए अपने रिवीजन को मजबूत बनाएं। सही रणनीति और अभ्यास से 90%+ अंक पाना संभव है!
JAC Board Class 12 Study Material
| JAC Board Class 12 Study Material | |
| JAC Board Class 12 Books | JAC Board Class 12 Previous Year Question Paper |
| JAC Board Class 12 Syllabus | JAC Board Class 12 Model Paper |
JAC Board 12th Accountancy Important Question Answer 2025
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
1. प्राप्ति और भुगतान खाता किस प्रकार का खाता है।
(a) व्यक्तिगत खाता
(b) वास्तविक खाता
(c) नाममात्र खाता
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर : (b)
2. साझेदारों की पूँजी पर ब्याज है
(a) व्यय
(b) विनियोजन
(c) लाभ
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:- (b)
3. सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है:
(a) अधिलाभ
(b) निश्चित लाभ
(c) असामान्य लाभ
(d) सामान्य लाभ
उत्तर:- (a)
4. अभिषेक, रजत और विवेक लाभ का विभाजन 5: 3:2 के अनुपात में करते हैं । यदि विवेक सेवानिवृत्त होता है तो अभिषेक तथा रजत का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा
(a) 3:2
(b) 5:3
(c) 5:2
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:- (b)
5. साझेदारी फर्म के विघटन की स्थिति में, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को स्थानांतरित कर दिया जाता है:
(a) वसूली खाता
(b) साझेदार पूँजी खाते
(c) विविध देनदार खाता
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर:- (a)
👉 ये भी पढ़े - JAC Board 12th Accountancy Question Bank 2024-25
6. जब कोई कंपनी प्रीमियम पर अंश जारी करती है, तो कंपनी द्वारा प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकती है:
(a) आवेदन राशि के साथ
(b) आवंटन राशि के साथ
(c) याचना के साथ
(d) उपरोक्त में से कोई भी।
उत्तर : (d)
7. ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा की प्रकृति होती है
(a) आयगत हानि
(b) पूंजीगत हानि
(c) आस्थगित आयगत व्यय
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर:- (b)
8. वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के........ उत्पाद हैं।
(a) प्रथम
(b) द्वितीय
(c) तृतीय
(d) अन्तिम
उत्तर:- (d)
9. तुलनात्मक विवरण और नकदी प्रवाह विवरण _________ के उदाहरण हैं
(a) स्थिर
(b) क्षैतिज
(c) कार्यक्षेत्र
(d) आंतरिक
उत्तर- (b)
10. तरल अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है-
(a) साधारण अनुपात में
(b) गुना में
(c) प्रतिशत में
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:- (a)
11. ऋणपत्रों का शोधन है:
(a) रोकड़ का अन्तर्वाह
(b) रोकड़ का बहिर्वाह
(c) न अन्तर्वाह और न बहिर्वाह
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर :- (a)
अति लघु उतरीय प्रश्न
Q1. आयगत प्राप्ति के दो उदाहरण दीजिए।
उत्तरः चंदा, प्रवेश शुल्क |
Q2. नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के लाभ - विभाजन अनुपात की गणना की आवश्यकता क्यों है?
उत्तर- नया लाभ - विभाजन अनुपात - नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभ व हानियां को आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहा जाता है। नए साझेदार के प्रवेश के कारण पुराने साझेदारों के लाभ-हानि का अनुपात बदल जाता है क्योंकि पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ भाग नए साझेदार को दे देते हैं। अतः नये लाभ - विभाजन का अनुपात ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है।
Q3. साझेदारी के विघटन से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:- जब सभी साझेदारों ने साझेदारी को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है, तो फर्म का विघटन हो जाता है (अर्थात्, फर्म समाप्त हो जाती है)।
Q4. वसूली खाता क्या है?
उत्तर:- किसी फर्म की संपत्ति के निपटान और उसकी दायित्वों का भुगतान करने की प्रक्रिया को वसूली कहा जाता है। वसूली खाता वह खाता है। जिसका उपयोग परिसंपत्तियों की बिक्री और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
Q5. अदत्त याचना किसे कहते हैं?
उत्तर- जब कोई अंशधारी आबंटन या किसी याचना की राशि का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं करता है तो इसे अदत्त याचना कहा जाता है।
Q6. ऋणपत्र क्या है?
उत्तर:- ऋणपत्र सरकार या कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक ऋण है। ऋणपत्र के बदले में कंपनी द्वारा ऋणपत्रधारी को ब्याज दिया जाता है।
Q7. वित्तीय विवरण शब्द में क्या सम्मिलित है ?
उत्तर:- लाभ-हानि विवरण एवं चिट्ठा ।
Q8. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ बताइए ।
उत्तर:- वित्तीय विवरणों में शामील सूचनाओं का विवेचनात्मक जाँच वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है।
Q9. अनुपात विश्लेषण से आपका क्या तात्पर्य है?
उत्तर- लेखांकन अनुपात के आधार पर किसी उद्यम के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए विभिन्न वित्तीय घटकों के मध्य संबंध का विश्लेषण करना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरण विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है।
Q10. रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है?
उत्तर: रोकड़ प्रवाह विवरण किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान एक फर्म के संचालन, विनियोग और वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी और नकद समकक्षों के अंतर्वाह और बहिर्वाह को सारांश के रूप में दर्शाता है।
Q11. संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए हास का लेखा किस प्रकार से किया जाता है?
उत्तरः संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए हास को शुद्ध लाभ हानि में जोड़ दिया जाता है।
Short Answer Type Questions
Q1. एक साझेदारी समझौता लिखित में क्यों होना चाहिए।
उत्तरः- भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारी समझौता लिखित में ही होना चाहिए लेकिन फिर भी हमेशा यह सुझाव दिया जाता है कि यह लिखित रूप में ही होना चाहिए क्योंकि आज साझेदारों के बीच बहुत अच्छे संबंध है लेकिन भविष्य में हो सकता है कि किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया तो एक लिखित समझौता साझेदारों के बीच विवादों और गलतफहमी ओं से बचने में मदद करेगा।
Q2. सेवानिवृत्त / मृत साझेदार फर्म की ख्याति में उसका भाग पाने का अधिकारी क्यों होता है?
उत्तर:- सेवानिवृत्त / मृत साझेदार फर्म की ख्याति में उसका भाग पाने का अधिकारी होता है क्योंकि ख्याति साझेदारों के सामूहिक प्रयत्नों का फल होती है। इसमें सेवानिवृत्त होने वाले अथवा मृत साझेदार की भी मेहनत होती है। इसलिए वह फर्म की ख्याति में अपना भाग पाने का अधिकारी होता है।
Q3. किसी साझेदार के सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय फर्म को अपनी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन और दायित्वों के दोबारा निर्धारण की आवश्यकता क्यों होती है?
उत्तर:- साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर कुछ परिसम्पत्तियाँ ऐसी हो सकती हैं जिन्हें उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं दर्शाया जाता तथा इसी प्रकार कुछ दायित्वों के मूल्य तथा फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्यों में अन्तर होता है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी अलिखित सम्पत्तियाँ भी होती हैं जिनको पुस्तकों में लाए जाने की आवश्यकता होती है, जैसा कि साझेदार के प्रवेश की स्थिति में होता है। पुनर्मूल्यांकन खाते को सम्पत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने तथा अलिखित मदों को फर्म की पुस्तकों में लाकर लाभ-हानि की गणना करने के लिए तैयार किया जाता है। इस लाभ अथवा हानि में सेवानिवृत्त/मृत साझेदार की भी हिस्सा होती है अतः इसे सभी साझेदारों के पूँजी खातों में, जिसमें सेवानिवृत्त/मृत साझेदार भी शामिल है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।
Q4. विघटन पर खातों के निपटान का क्रम बतायें।
उत्तर:- साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार विघटन पर खातों के निपटान के नियम निम्नलिखित हैं।
i. परिसंपत्तियों का उपयोग:- परिसंपत्तियों की वसूली (बिक्री) से प्राप्त राशि का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा:
a. सबसे पहले बाहरी दायित्वों और खर्चों का भुगतान करना होगा।
b. फिर, साझेदारों द्वारा अग्रेषित सभी ऋण और अग्रिम का भुगतान किया जाना चाहिए।
c. फिर, प्रत्येक साझेदार की पूंजी का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि (a), (b) और (c) के भुगतान के बाद कोई अधिशेष बचता है, तो इसे साझेदारों के बीच उनके लाभ-विभाजन अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए।
ii. हानि का व्यवहारः- हानि और पूंजी की किसी कमी की स्थिति में इसका भुगतान निम्नलिखित क्रम में किया जाना चाहिए:
a. सबसे पहले इन्हें फर्म के लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए।
b. फिर, फर्म की कुल पूँजी के विरुद्ध ।
c. यदि कोई हानि या कमी है तो भी इसे सभी साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने लाभ - विभाजन अनुपात में वहन किया जाना चाहिए।
Q5. सार्वजनिक कंपनी क्या है?
उत्तर: एक सार्वजनिक कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंश बाजार के माध्यम से आम जनता को अंश, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रतिभूतियों के रूप में अपने स्वामित्व का एक हिस्सा प्रदान करती है। सार्वजनिक कंपनी का अर्थ है एक कंपनी जो
(a) एक निजी कंपनी नहीं है,
(b) जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5,00,000 रुपये या उससे हो।
(c) एक निजी कंपनी है, जो एक ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है।
Q6. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है?
उत्तर: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने सदस्यों द्वारा अंशों या गारंटी द्वारा सीमित होती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी न्यूनतम चुकता अंश पूंजी 1,00,000 रुपये है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है:
(a) यह अपने अंशों को स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।
(b) एक निजी कंपनी बनाने के लिए कम से कम दो और अधिकतम 200 सदस्य होने चाहिए।
(c) यह अपने अंशों, या ऋणपत्र की सदस्यता के लिए आम जनता से आवेदन आमंत्रित नहीं कर सकता है।
(d) यह अपने सदस्यों, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों से जमा आमंत्रित या स्वीकार नहीं करता है।
Q7. एक ऋणपत्र से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:- ऋणपत्र कम्पनी द्वारा निर्गत एक प्रमाण पत्र है, जो कम्पनी द्वारा लिए गये कर्ज का प्रमाण होता है। इसमें कंपनी द्वारा लिये गए कर्ज की रकम, ब्याज की दर, कर्ज के शोधन का समय आदि का उल्लेख रहता है। इस पर एक निर्धारित दर से ब्याज छमाही या वार्षिक दिया जाता है। इसके धारक को ऋणपत्रधारी कहते है। इस पत्र पर कम्पनी की सार्वमुद्रा रहती है।
Q8. वित्तीय विवरणों का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर:- कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के संचालन के परिणामों की एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद हैं। ये वार्षिक विवरण हैं जो विभिन्न उद्यमों या संगठनों द्वारा एक विशेष लेखा अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण के माध्यम से निगम (कंपनी) प्रबंध, स्वामियों तथा अन्य विभिन्न बाह्रय उपयोगकर्ताओं, निवेशक, कराधान अधिकारी, सरकार, कर्मचारी आदि को वित्तीय सूचनाएँ संचारित करता है। यह समान्यतः कंपनी के लेखांकन अवधि के अंत के तुलन-पत्र तथा लाभ हानि विवरण को प्रदर्शित करती है।
Q9. विश्लेषण एवं निर्वचन का अर्थ समझाइए |
उत्तर:- विश्लेषण और निर्वचन वित्तीय विवरणों की एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण जाँच को संदर्भित करता है। यह न केवल वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों के बीच कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है बल्कि वित्तीय आंकड़ों को भी उचित तरीके से प्रस्तुत करता है। विश्लेषण और निर्वचन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत करना है जो आसानी से समझा जा सके और व्याख्यात्मक हो। यह न केवल लेखा उपयोगकर्ताओं को समय की अवधि में व्यापार के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करता है बल्कि उन्हें निर्णय लेने और नीति और वित्तीय नियोजन में भी सक्षम बनाता है।
Q10. अनुपात विश्लेषण से आपका क्या तात्पर्य है?
उत्तरः अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण की एक तकनीक है। यह तलपट और आय विवरण के विभिन्न मदों के बीच संबंध का वर्णन करता है। यह एक फर्म की लाभप्रदता, परिचालन दक्षता, ऋण शोधन क्षमता आदि का पता लगाने में हमारी मदद करता है। इसे अनुपात, प्रतिशत और गुणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह विभिन्न वित्तीय चरों के बीच गुणात्मक संबंध का आकलन करके बजटीय नियंत्रण को सक्षम बनाता है। अनुपात विश्लेषण एक फर्म की वित्तीय स्थिति व्यवहार्यता और प्रदर्शन के संबंध में विभिन्न लेखांकन उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने और नीति तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचा भी निर्धारित करता है।
Q11. रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते है?
उत्तर: रोकड़ प्रवाह विवरण एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान एक फर्म के संचालन, विनियोग और वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी और नकद समकक्षों के अंतर्वाह और बहिर्वाह को सारांश के रूप में दर्शाता है। यह एक लेखा वर्ष के दौरान नकद एवं नकद समतुल्य के प्राप्तियों, भुगतानों और उनके आरंभिक और अंतिम शेष में परिवर्तन के कारणों को दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह से आशय रोकड़ के अंतर्वाह और बहिर्वाह से हैं। रोकड़ अंतर्वाह का अर्थ होता है विभिन्न मदों से प्राप्त रोकड़ या नकद रुपए, जैसे परिचालन क्रियाओं से प्राप्तियां, भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि इत्यादि । रोकड़ बहिर्वाह से हमारा तात्पर्य विभिन्न मदों में किए गए नकद भुगतानों से है। उदाहरण माल का नकद क्रय, संपत्तियों का क्रय आदि।
Long Answer Type Questions
Q1. कथन स्पष्ट कीजिए: "प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रोकड़ बही का सारांश है।
उत्तरः प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही की तरह ही बनाया जाता है। इस खाते में सभी प्राप्तियों एवं भुगतानों को लिखा जाता है। गैर-व्यापारिक संस्थाओ द्वारा सभी नकद लेन-देन का लेखा रोकड़ बही की सहायता से प्राप्ति एवं भुगतान खाता में लिखा जाता है। यह एक वास्तविक खाता होता है। इसके डेबिट पक्ष में आयगत एवं पूँजीगत दोनो मदों की प्राप्तियों को लिखा जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष में सभी आयगत एवं पूँजीगत मदों के भुगतान को लिखते है। इसमें चालू वर्ष, गतवर्ष या आगामी वर्ष से सम्बन्धित सभी प्राप्तियो एवं भुगतान को लिखा जाता है। इस खाते में केवल रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानो को लिखा जाता है। इसमे गैर रोकड़ व्यय जैसे- हास, अदत्त - व्यय, पूर्वदत्त-व्यय, उपार्जित आय एवं अनुपार्जित आय का लेखा नही किया जाता है। इसे रोकड़ बही की तरह तिथिवार बनाया जाता है। इस खाते का प्रारम्भ रोकड़ के प्रारम्भिक शेष से तथा अन्त रोकड़ के अन्तिम शेष से होता है। इस खाते से लाभ-हानि का पता नहीं चलता है। इसकी सहायता से आय-व्यय खाता एवं आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है । प्राप्ति एवं भुगतान खाता द्वारा एक निश्चित तिथि को गैर-व्यापारिक संस्था की रोकड़ की स्थिति, बैंक शेष एवं बैंक अधिविकर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी सहायता से संस्था के रोकड़ पर नियंत्रण किया जा सकता है।
Q2. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होते हैं।
उत्तर:- साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में वर्णित निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं-
(a) लाभ एवं हानियों का विभाजन साझेदारों में बराबर-बराबर होगा।
(b) किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन, कमीशन या अन्य परिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।
(c) साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा।
(d) प्रत्येक साझेदार को फर्म के व्यापार तथा प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होगा।
(e) प्रत्येक साझेदार को व्यापार के लेखा अभिलेखों को देखने, जांचने व उनकी नकल लेने का अधिकार होगा।
(f) साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। हानि की दशा में भी ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
(g) सभी साझेदारों की सहमति के बिना साझेदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
(h) साझेदारों को उनके पूँजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
Q3. साझेदार के प्रवेश के समय परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए?
उत्तर- नये साझेदार के प्रवेश के समय परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मल्यांकन किया जाना चाहिए। नये साझेदार के प्रवेश पर सम्पत्तियों व दायित्वों का पुस्तक मूल्य बाजार मूल्य से कम अथवा अधिक हो सकता है। अतः नये साझेदार के प्रवेश पर पुराने तथा नये साझेदार दोनों यही पसन्द करते सम्पत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कर लिया जाए। पुनर्मूल्यांकन पर हुई लाभ अथवा हानि को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बाँटते हैं। यदि सम्पत्तियों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से अधिक हो गया है अथवा दायित्वों का मूल्य कम हो गया है तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होगा तथा पुराने साझेदार नये साझेदार को इस लाभ में से हिस्सा नहीं देना चाहेंगे। इसके विपरीत यदि सम्पत्तियों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से कम हो गया है अथवा दायित्वों का मूल्य बढ़ गया है तो पुनर्मूल्यांकन पर हानि होगी तथा नया साझेदार इस हानि में भागीदारी नहीं बनना चाहेगा। इस समस्या के समाधान के लिए नये साझेदार के प्रवेश पर सम्पत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं तथा इससे होने वाली लाभ-हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बाँट देते हैं। सम्पत्तियों व दायित्वों के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन करने के लिए जिस खाते के माध्यम से समायोजन किया जाता है, उसे पुनर्मूल्यांकन खाता (Revaluation Account) कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर इस खाते को डेबिट तथा सम्बन्धित सम्पत्ति व दायित्व को क्रेडिट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर इस खाते को क्रेडिट तथा सम्बन्धित सम्पत्ति व दायित्व को डेबिट किया जाता है।
Q4. आप मृत साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार करेंगे?
उत्तर- सामान्यतः सेवानिवृत्त होने वाला साझेदार, लेखा वर्ष की समाप्ति वाले दिन अथवा आगामी लेखा वर्ष के प्रथम दिन ही फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में उसको देय राशि का निर्धारण, अन्तिम चिट्टे में दिखाए गए उसके पूँजी खाते तथा चालू खाते के समायोजित शेष के आधार पर किया जा सकता है, बशर्ते कि फर्म की सम्पत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन उचित प्रकार से किया गया हो। यदि इनका मूल्यांकन उचित प्रकार से न किया गया हो तो इनके पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा हानि के सम्बन्ध में उचित समायोजन किया जाएगा।
किसी साझेदार की मृत्यु अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों में लेखा वर्ष के दौरान भी ऐसे साझेदार को देय राशि का निर्धारण करने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः साझेदार की सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के समय देय राशि का निर्धारण सेवानिवृत्त साझेदार (सेवानिवृत्ति के समय) और मृत साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी (मृत्यु के समय को देय राशि में निम्न शामिल हैं:
a. उसके पूँजी खातों का जमा (credit) शेष
b. उसके चालू खातों का जमा शेष
c. उसकी ख्याति का हिस्सा
d. उसके निर्धारित लाभ का हिस्सा
e. परिसम्पत्तियों तथा दायित्व के पुनर्मूल्यांकन में उसके अभिलाभ का हिस्सा
f. उसके सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख तक उसके लाभ का हिस्सा
g. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक उसके पूँजी पर ब्याज (यदि शामिल है) का भाग तथा
h. वेतन/कमीशन, यदि कोई हो, तो सेवानिवृत्त/मृत्यु की तिथि तक उसको देय राशि।
दी गई कटौतियाँ, यदि कोई हों, तो उसके हिस्से से ली जाएँगी :
a. उसके चालू खातों का नाम (Debit) शेष
b. अपलिखित ख्याति का हिस्सा
c. उसकी निर्धारित हानियों का हिस्सा
d. सम्पत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर उसकी हानियों का हिस्सा
e. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक उसके हानियों का हिस्सा
f. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक उसके द्वारा आहरित राशि हिस्सा
g. आहरण पर ब्याज, यदि शामिल है, सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि तक
इस प्रकार सेवानिवृत्त / मृत साझेदार को देय राशि की गणना कर निर्धारित विधि द्वारा सेवानिवृत्त साझेदार अथवा मृत साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान किया जा सकता है।
Q5. लेनदारों की देय राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?
उत्तरः- किसी फर्म के विघटन के समय, फर्म की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग लेनदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। यदि बिक्री प्राप्तियां कम हो जाती हैं, तो साझेदारों की निजी संपत्तियों का उपयोग फर्म के लेनदारों के बकाया का निपटान करने के लिए किया जाता है। यदि लेनदारों को देय राशि का कुछ भाग भुगतान न किया गया हो तो भी लेनदारों की कमी उत्पन्न हो जाती है। लेनदारों की कमी के भुगतान के लिए आम तौर पर दो प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
1. कमी को कमी खाते में स्थानांतरित करना
2. कमी को साझेदार के पूँजी खाते में स्थानांतरित करना
पूर्व प्रक्रिया में, फर्म के लेनदारों के लिए एक अलग खाता तैयार किया जाता है। फिर फर्म की संपत्तियों और साझेदारों की निजी संपत्तियों की बिक्री से अर्जित नकदी शेष का पता लगाने के लिए, नकद खाता तैयार किया जाता है। फर्म के पास नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद, लेनदारों और बाहरी दायित्वों का भुगतान आनुपातिक रूप से (आंशिक रूप से) किया जाता है। शेष अवैतनिक लेनदारों या कमी को कमी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
बाद की प्रक्रिया में, लेनदारों को साझेदार के व्यक्तिगत योगदान सहित फर्म के पास उपलब्ध नकदी से भुगतान किया जाता है। कमी या अवैतनिक लेनदारों की राशि भागीदार के पूँजी खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। इस प्रकार ऋणदाताओं की कमी को सभी साझेदारों द्वारा अपने लाभ विभाजन अनुपात में वहन किया जाता है। यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है और कमी को सहन करने में असमर्थ होता है, तो इसे फर्म के लिए पूँजीगत हानि माना जाएगा। यदि साझेदारी विलेख किसी भागीदार के दिवालिया होने की स्थिति में इस तरह की पूँजी हानि के बारे में चुप है, तो गार्नर बनाम मरे मामले के अनुसार, इस तरह की पूँजी हानि को उनके पूँजी अनुपात में दिवालिया साझेदारों द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
Q6. एक कंपनी की अंश पूँजी को स्पष्ट करें।
उत्तरः- एक कंपनी की अंश पूँजी का मुख्य श्रेणियों में विभाजन को आरेखीय रूप से नीचे समझाया गया है।
i. अधिकृत पूँजी: यह एक राशि है जो पार्षद सीमा नियम (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में बताई गई है। यह अधिकतम राशि है जो कंपनी अंश जारी करके जुटा सकती है।
ii. निर्गमित पूँजी: यह अधिकृत पूंजी का एक हिस्सा है जो कंपनी द्वारा आम जनता को सदस्यता के लिए दी जाती है।
iii. प्रार्थित पूँजी : यह निर्गमित पूंजी का एक हिस्सा है जो वास्तव में आम जनता द्वारा प्रार्थित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश के 8,000 अंश जारी किए हैं और जनता ने 7,500 अंशों की सदस्यता ली है, तो कंपनी की प्रार्थित अंश पूंजी 75,000 रुपये है। इसके दो भाग हैं:
(a) प्रार्थित और पूरी तरह से भुगतान किया गया
(b) प्रार्थित लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया
Q7. वित्तीय विवरणों के महत्व को विस्तार से समझाइए ।
उत्तरः वित्तीय विवरणों के महत्व निम्नलिखित है-
(i) सूचना प्रदान करता है- वित्तीय विवरण अंशधारकों को प्रबन्धकों की कार्यदक्षता की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय विवरणों की सहायता से प्रबन्धन की कार्यदक्षता या निष्पादन तथा स्वामित्व की अपेक्षाओं के बीच अन्तर को समझा जा सकता है। वित्तीय विवरण आंतरिक और बाह्य दोनों उपयोगकर्ताओं को अपने निवेश की स्थिति, सुरक्षा तथा वापसी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कि वे व्यवसाय में निवेश को बनाये रखें या उसे समाप्त कर दें। इस तरह के महत्त्वपूर्ण निर्णयों को लेने में वित्तीय विवरण अंशधारकों को मदद करते हैं इसके साथ ही साथ वित्तीय विवरण कंपनी की कर देयता की राशि की गणना करने में कर अधिकारियों की मदद करते हैं।
(ii) रोकड़ प्रवाह - वित्तीय विवरण कंपनी के रोकड़ प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वित्तीय विवरण कंपनी की तरलता निर्धारित करने में लेनदारों और अन्य निवेशकों की मदद करते हैं।
(iii) लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण- वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा लेखांकन की विभिन्न नीतियों, विधियों, प्रथाओं और लेखांकन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों को सरल, सत्य
नाता है और विभिन्न लेखांकन उपयोगकर्ताओं को बिना किसी अस्पष्टता के समझने में सक्षम बनाता है।
(iv) सरकार के लिए महत्त्व - वित्तीय विवरण राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक विकास आदि का निर्धारण करने के लिए आवश्यक
होती है। लेखांकन सूचना के आधार पर ही सरकार औद्योगिक, कराधान एवं अनेक आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है और विभिन्न आर्थिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी आदि को दूर करने में सहायता करती है। इस प्रकार सरकार के लिए भी वित्तीय विवरणों का बहुत महत्त्व है।
(v) निवेशकों के लिए महत्त्व - वित्तीय विवरण निवेशकों को दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता का आकलन के साथ-साथ व्यवसाय की लाभदायकता को भी आँकने में सहायता करते हैं। क्योंकि निवेशक मुख्यतः अपने निवेश की सुरक्षा एवं तरलता के साथ- साथ न्यायोचित लाभ की भी अपेक्षा रखते हैं।
(vi) ऋणपत्रधारियों के लिए महत्त्व ऋणपत्रधारी संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि वित्तीय विवरणों से आसानी से जानी जा सकती है।
Q8. समरूप विवरणों को कैसे तैयार करते हैं उदाहरण देकर बताइए।
उत्तरः- समरूप विवरण का अर्थ एक ऐसे विवरण से है जिसमें समान आधार पर विभिन्न मदों को % (प्रतिशत) के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें लाभ-हानि विवरण के विभिन्न मदों में परिवर्तनों को शुद्ध विक्रय या कुल आय तथा कुल सम्पत्तियों या कुल दायित्वों को चिट्ठा के योग से प्रतिशत के रूप मे व्यक्त किया जाता है। यह एक सरल एवं संक्षिप्त विधि है। यह व्यवसाय के कार्यकलापों में तेजी से उच्चावच हो रहे है तो उस स्थिति में यह विधि विशेष रूप से उपयोगी प्रतीत होती है। समरूप विवरण को समान आकार वाले विवरण भी कहते है। यह दो प्रकार के होते है :-
(1) समान आकार का आय विवरण
(ii) समान आकार का स्थिति विवरण
(i) समान आकार का आय विवरण- समान आकार का आय विवरण एक ऐसा विवरण है जिसमें शुद्ध विक्रय की राशि को 100 मान लिया जाता है और आय विवरण के सभी मदों को उसके प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
(ii) समान आकार का स्थिति विवरण: इसका अभिप्राय एक ऐसे विवरण से है जिसमें कुल दायित्वों अथवा कुल सम्पतियों को 100 मानकर सम्पति व दायित्व पक्ष की मदों राशियों को इस योग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
Q9. लेखांकन अनुपात के उद्देश्यों को लिखिए।
उत्तरः लेखांकन अनुपात के निम्नलिखित उद्देश्य है-
i) व्यवसाय की लाभदायकता का मापन करना ।
ii) व्यवसाय की शोधन क्षमता का मापन करना ।
iii) संगठन की परिचालन कुशलता ज्ञात करना ।
iv) व्यवसाय की तरलता को मापना ।
v) लेखांकन सूचनाओं को सरल एवं सारांशित रूप से व्यक्त करना ।
vi) तुलनात्मक अध्ययन में सहायता प्रदान करना ।
vii) पूर्वानुमान एवं बजट बनाने में सहायता करना ।
viii) प्रबन्धकों को निर्णय लेने में मदद करना ।
ix) वित्तीय नियोजन में प्रबंध को सहायता प्रदान करना ।
Q10. एक रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने के उद्देश्यों को लिखिए।
उत्तर:- रोकड़ प्रवाह विवरण एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान एक फर्म के संचालन, विनियोग और वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी और नकद
i) समकक्षों के अंतर्वाह और बहिर्वाह को सारांश के रूप में दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं- विभिन्न गतिविधियों से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के शुद्ध अंतर्वाह और बहिर्वाह का निर्धारण करना रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का प्राथमिक उद्देश्य है।
ii) लगातार दो वित्तीय वर्षों के आर्थिक चिट्ठों में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में हुए परिवर्तन को ज्ञात करना।
iii) कंपनी के कुशल प्रबंधन में सहायता प्रदान करना।
iv) रोकड़ बजट के निर्माण में प्रबंधन को सहायता प्रदान करना।
(v) वित्तीय नीतियों के निर्धारण में सहायता प्रदान करना
vi) अंशधारियों को लाभांश के भुगतान करने के संबंध में निर्णय लेने में प्रबंधन को सहायता प्रदान करना।
vii) संस्था की तरलता की स्थिति पता लगाना ।
Q11. रोकड़ प्रवाह विवरण के उपयोगों की व्याख्या कीजिए
उत्तर: रोकड़ प्रवाह विवरण के उपयोग इस प्रकार हैं:
i) रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ अंतर्वाहों और बहिर्वाहों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करके अल्पकालिक वित्तीय नियोजन में मदद करता है।
ii) यह कंपनी के रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के शेष राशि में परिवर्तन के कारण को निर्धारित करने में मदद करता है।
iii) यह कंपनी की तरलता और ऋण शोधन क्षमता को मापने और विश्लेषण करने में मदद करता है।
iv) यह एक फर्म की विभिन्न गतिविधियों से नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह के रुझानों की जांच और अध्ययन करने में मदद करता है और इस तरह विभिन्न नीतियों और अल्पकालिक योजना बनाने में मदद करता है।
v) यह विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से नकदी प्रवाह को संचालन, विनियोजन और वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह या बहिर्वाह के रूप में अलग करना संभव बनाता है।
vi) यह रोकड़ की उपलब्धता के आधार पर लाभ के वितरण पर निर्णय लेने में मदद करता है।







 Profile
Profile Signout
Signout










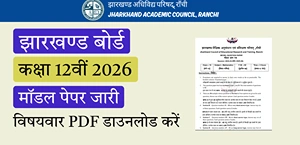

 Quiz
Quiz
 Get latest Exam Updates
Get latest Exam Updates 










