JAC 12th History Exam 2025 : Important ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ, परीक्षा से पहले रटलो
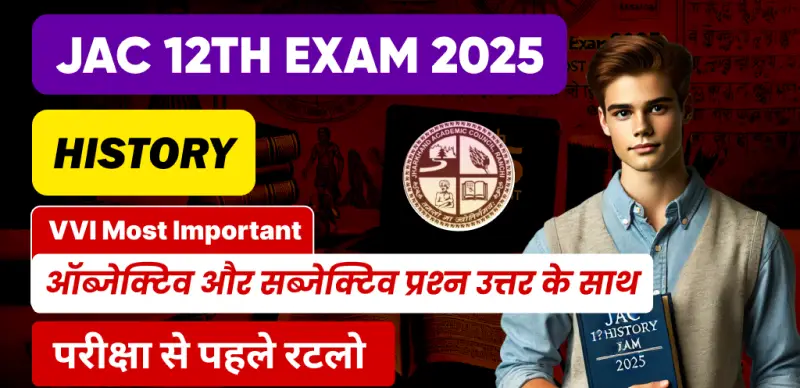
SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
JAC बोर्ड कक्षा 12 इतिहास परीक्षा 28 फरवरी 2025 को होगी। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का संकलन यहां दिया गया है। यह प्रश्न बैंक पिछले वर्षों के पेपर और विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा सवालों पर आधारित है।
ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में MCQs, Fill in the Blanks और सही-गलत प्रकार के सवाल शामिल हैं, जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। वहीं, सब्जेक्टिव प्रश्नों में 2, 3, 5 और 8 अंकों के विस्तृत उत्तर सहित महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। इससे परीक्षा पैटर्न को समझने और बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी।
JAC Board Class 12 Study Material
| JAC Board Class 12 Study Material | |
| JAC Board Class 12 Books | JAC Board Class 12 Previous Year Question Paper |
| JAC Board Class 12 Syllabus | JAC Board Class 12 Model Paper |
अच्छे अंक पाने के लिए अपने रिवीजन को मजबूत बनाएं। सही रणनीति और अभ्यास से 90%+ अंक पाना संभव है!
JAC Board 12th History Important Question Answer 2025
बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1. भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है ?
A. एलेग्जेंडर कनिंघम
B. दयाराम साहनी
C. राखलदास बनर्जी
D. एस आर राव
उत्तर: A. एलेग्जेंडर कनिंघम
प्रश्न 2. हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी?
A. लोथल
B. हड़प्पा
C. मोहनजोदड़ो
D. कालीबंगा
उत्तर: B. हड़प्पा
प्रश्न 3. अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा ?
A. जॉन मार्शल
B. कनिंघम
C. जेम्स प्रिंसेप
D. अर्नेस्ट मैके
उत्तर: C. जेम्स प्रिंसेप
प्रश्न 4. अभिलेखों में 'देवनाम पियदस्सी' किस राजा को कहा गया है?
A. अशोक
B. चन्द्रगुप्त मौर्च
C. समुद्रगुप्त
D. बिन्दुसार
उत्तर: A. अशोक
प्रश्न 5. महाभारत की रचना किसने की?
A. मनु
B. वेदव्यास
C. बाल्मीकि
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर: B. वेदव्यास
प्रश्न 6. दुर्योधन की मां कौन थी ?
A. गांधारी
B. कुंती
C. माद्री
D. सत्यवती
उत्तर: A. गांधारी
प्रश्न 7. सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
A. विदिशा
B. रायसेन
C. सागर
D. भोपाल
उत्तर: B. रायसेन
प्रश्न 8. स्तूप किस धर्म से संबंधित है?
A. जैन धर्म
B. बौद्ध धर्म
C. शैव धर्म
D. वैष्णवधर्म
उत्तर: B. बौद्ध धर्म
प्रश्न 9. महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था?
A. कबीर
B. वर्धमान
C. सिद्धार्थ
D. देवदत्त
उत्तर: B. वर्धमान
प्रश्न 10. अलबरूनी का जन्म कहां हुआ था ?
(A) ख्वारिज्म
(B) मोरक्को
(C) तुर्की
(D) सीरिया
उत्तर: (A) ख्वारिज्म
प्रश्न 11. अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे?
(A) सीरियाई भाषा
(B) फारसी भाषा
(C) संस्कृत भाषा
(D) यूनानी भाषा
उत्तर: (D) यूनानी भाषा
प्रश्न 12. इब्नबतूता सिंध कब पहुंचा?
A 1342
B 1333
C 1345
D 1347
उत्तर: B 1333
प्रश्न 13. पद्मावत किसकी रचना है?
A. कबीर
B. तुलसीदास
C. अमीर खुसरो
D. मलिक मोहम्मद जायसी
उत्तर: D. मलिक मोहम्मद जायसी
प्रश्न 14. विजय नगर के संस्थापक कौन थे?
A. कृष्णदेवराय
B. देवराय
C. महमूद गवा
D. हरिहर और बुक्का
उत्तर: D. हरिहर और बुक्का
प्रश्न 15. तालिकोटा की लड़ाई कब हुई ?
A. 1526 ईसवी
B. 1556 ईस्वी
C. 1565 ईसवी
D. 1575 ईसवी
उत्तर: C. 1565 ईसवी
प्रश्न 16. अकबरनामा की रचना किसने की थी?
A. अमीर खुसरो
B. अलबरूनी
C. इब्नबतूता
D. अबुल फजल
उत्तर: D. अबुल फजल
प्रश्न 17. भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है?
A. बाबर
B. हुमायूं
C. औरंगजेब
D. जहांगीर
उत्तर: A. बाबर
प्रश्न 18. किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था?
A. बाबर
B. हुमायूं
C. अकबर
D. औरंगजेब
उत्तर: C. अकबर
प्रश्न 19. जोतदार कौन होते थे ?
A. गाँव का मुखिया
B. धनवान रैय्यत
C. जमींदार
D. न्यायधीश
उत्तर: B. धनवान रैय्यत
प्रश्न 20. 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
A लॉर्ड वेलेजली
B लॉर्ड विलियम बेंटिक
C लॉर्ड डलहौजी
D लॉर्ड कैनिंग
उत्तर: D लॉर्ड कैनिंग
👉 Download PDF - JAC Board 12th History Important Question Answer 2025
अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है?
उत्तर: हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टिन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था।
प्रश्न 2. हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है?
उत्तर: हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है ।
प्रश्न 3. मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था?
उत्तर: मेगास्थनीज भारत में चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार मे आया था।
प्रश्न 4. महाकाव्य से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: एक लम्बी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो जैसे महाभारत ।
प्रश्न 5. स्तूप क्या है?
उत्तर: स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला, ढेर या थहा होता है महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को आठ भागों में बांटा गया तथा उन पर सामाधियों का निर्माण किया गया, इन्हीं को स्तूप कहते हैं।
प्रश्न 6. अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी?
उत्तर: अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी।
प्रश्न 7. अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी?
उत्तर: अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी।
प्रश्न 8. हंपी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय किसे जाता है?
उत्तर: अभियंता और पूराविद कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा हंपी के भग्नावशेषों 1800 ईसवी में प्रकाश में लाए गए थे।
प्रश्न 9. पटवारी किसे कहते थे?
उत्तर: पटवारी गांव की जमीन प्रत्येक किसान द्वारा जुते जाने वाले खेतों, फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता था।
प्रश्न 10. मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ?
उत्तर: मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है मुगलों ने स्वयं इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया क्योंकि पितृ पक्ष से वे तैमूर के वंशज थे, और तैमूरी कहलाते थे। तथा मातृ पक्ष से बाबर चंगेज खान से संबंधित था। 16 वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उसके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया।
प्रश्न 11. उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है और अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है।
प्रश्न 12. 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेताओं के नाम बताएं।
उत्तर: नाना साहेब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर ।
प्रश्न 13. बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 ई० में कहां आक्रमण किया था?
उत्तर: 1756 ई0 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा बनाए गए माल गोदाम (छोटे किले) पर कब्जा कर लिया।
प्रश्न 14. दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया?
उत्तर: दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया।
प्रश्न 15. भारत का विभाजन कब हुआ ?
उत्तर: भारत का विभाजन 1947 ई. को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, जो दो संप्रभु राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान के रूप में सामने आया।
प्रश्न 16. महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे?
उत्तर: महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे।
प्रश्न 17. हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से थे?
उत्तर: हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था।
प्रश्न 18. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया ?
उत्तर: नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया।
प्रश्न 19. गोत्र को परिभाषित करें।
उत्तर: गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति-रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है।
प्रश्न 20. स्त्रीधन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहारस्वरूप धन को स्त्रीधन कहा जाता है। यह दहेज से भिन्न है क्योंकि दहेज़ वर पक्ष को दिया जाता है। स्त्रीधन पर सम्पूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है।
लघु उत्तरी प्रश्न
प्रश्न 1. हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें?
उत्तर: हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। खुदाई में बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना किया करते थे। हड़प्पा वासी मातृ देवी के साथ देवताओं की भी पूजा किया करते थे । मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारते बनाई गई होंगी लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। पशुपतिनाथ वृक्ष, लिंग, योनि, और पशु आदि की भी पूजा थी । वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी। इस काल के लोग जादू टोना, भूत, प्रेत और अंधविश्वासों पर विश्वास किया करते थे। वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे। हड़प्पा वासी कूबड़ वाला सांड की भी पूजा किया करते थे। ये लोग पक्षियों की भी पूजा किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवत हड़प्पा वासियों की ही देन है।
प्रश्न 2. सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
उत्तर: मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के किले में स्थित है। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है । यह जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है। इसके दोनों किनारों पर अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईटों का बना हुआ है। इसके तीन ओर कमरे बने हुए थे। इनमें से एक में एक बड़ा कुआँ था जिससे जलाशय से पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए एक नाली थी। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में आठ स्नानघर बने हुए थे। इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है।
प्रश्न 3. अभिलेख से आप क्या समझते हैं? इनका का क्या महत्व है?
उत्तर: अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है तथा जिन पर तिथि नहीं होती उनका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया है।
महत्व:
1. अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रमाणिक और विश्वसनीय स्रोत होते हैं क्योंकि ये समकालीन होते हैं।
2. अभिलेख बनवाने वाले के अभिलेखों से शासक के विचार, राज्य विस्तार, उपलब्धियाँ, चरित्र, जन भावना का पता चलता है।
3. अभिलेखों से तत्कालिन धर्म-संस्कृति, रीति-रिवाजों की जानकारी मिलती है।
4. अभिलेखों से तात्कालिन भाषा और लिपि का ज्ञान होता है।
5. शासकों के आदेश, शत्रु- विजय तथा नागरिक अधिकारों की जानकारी मिलती है।
6. अभिलेखों से उस काल के समय का ज्ञान होता है।
7. अभिलेख प्राचीन इतिहास के स्थाई प्रमाण होते है।
8. अभिलेख से तात्कालिन अर्थव्यवस्था की भी जानकारी मिलती है।
9. अभिलेख से शासक और प्रजा के बीच का संबंध भी पता चलता है।
10. अभिलेख से कला का भी ज्ञान होता है।
प्रश्न 4. स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्त्वपूर्ण रही होगी?
उत्तर: पितृवंशकिता का आशय वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र इत्यादि से चलती है। विशिष्ट परिवारों में वस्तुतः शासक एवं संपन्न परिवार शामिल थे। ऐसे परिवारों की पितृवंशिकता निम्नलिखित दो कारणों से महत्त्वपूर्ण रही होगी।
1. वंश-परंपरा को नियमित रखने हेतु- धर्मसुत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं। अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र प्राप्ति की थी। यह तथ्य ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय इंद्र से उसके लिए पुत्र की कामना करता है।
2. उत्तराधिकार संबंधी विवाद से बचने हेतु - विशिष्ट परिवारों के माता-पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकार को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हो । राज परिवारों में तो उत्तराधिकार के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी। अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था।
प्रश्न 5. जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें?
उत्तर: जैन धर्म के प्रमुख पांच सिद्धांत निम्नलिखित हैं:-
1. सत्य- हमेशा सत्य बोलना चाहिए
2. अहिंसा - कभी हिंसा नहीं करना चाहिए
3. आस्तेय- कभी चोरी नहीं करना चाहिए
4. अपरिग्रह - संपत्ति का संग्रह ना करना
5. ब्रह्मचर्य - इंद्रियों को वश में रखना।
प्रश्न 6. किताब उल हिंद पर एक लेख लिखे ?
उत्तर: “किताब-उल-हिन्द” पुस्तक की रचना अलबरूनी ने सुल्तान महमूद गजनवी के शासकाल की थी। अलबरूनी इस पुस्तक की रचना अरबी भाषा में की थी। यह पुस्तक 80 अध्यायो और अनेक उप अध्यायों में विभक्त है। इस पुस्तक से महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अलबरूनी अपनी पुस्तक में भारतीय समाज रहन - सहन, खान-पान, वेश-भूषा सामाजिक प्रथाओं, त्योहार धर्म, दर्शन कानून, अपराध, दंड, ज्ञान - विज्ञान, खगोलशास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन दर्शन आदि का वर्णन करते हैं। वे भारत में प्रचलित विभिन्न संवतो, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और उनकी दूरी का भी उल्लेख करते है। चूँकि यह पुस्तक महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई, परंतु इसमें महमूद गजनवी के क्रियाकलापो का यदा-कदा ही उल्लेख मिलता है इस पुस्तक से तत्कालीन राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती है, परंतु भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए किताब - उल - हिन्द अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है।
प्रश्न 7. इब्नबतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यो की विवेचन कीजिए।
उत्तर: इब्नबतूता के विवरण से पता चलता है कि चौदहवीं शताब्दी भारत में दास प्रथा का प्रचलन व्यापक रूप से था। दासों की खुलेआम बिक्री होती थी। जगह- जगह पर दासो की बिक्री के लिए बाजार लगते थे। राजघराने और कुलीन परिवारों में दास बडी संख्या में रखे जाते थे। सामान्य लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार एक-दो दास रख लेते थे। स्त्री - दास अर्थात् दासियाँ भी रखी जाती थी। दास-दासियो को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। दासों को भेट के रूप में देने की प्रथा का प्रचलन था । स्वयं इब्नबतूता ने सिंध पहुचने पर दिल्ली सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, ऊँट और दास खरीदे थे। सुल्तान किसी व्यक्ति विशेष से प्रसन्न होन पर उसे इनाम के रूप में दास प्रदान करते थे। दास-दासी सामान्यता स्वामी के नौकर के रूप में कार्य करते थे एवं उनका मूल्य उनके काम और योग्यता के अनुसार निर्धारित किया जाता था। दासों से आर्थिक कार्यो सहायता ली जाती थी। उनसे गुप्तचरी का काम भी लिया जाता था और विशेष अवसरो पर दास दासी मुक्त भी किए जाते थे ।
प्रश्न 8. क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया?
उत्तर: चोल शासकों ने नयनार संतो के साथ संबंध बनाने पर बल दिया और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न किया। अपने राजस्व के पद को दैवीय स्वरूप प्रदान करने और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए चोल शासकों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया और उनमें पत्थर तथा धातु से बनी मूर्तियां स्थापित कराई। इस प्रकार लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया। चोल शासकों ने तमिल भाषा शैव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित किया।
परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को मात्र उत्सव के दौरान निकाला जाता था। सूफी संत सामान्यता सत्ता से दूर रहने की कोशिश करते थे किंतु यदि कोई शासक बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो वे उसे स्वीकार करते थे । कई सुल्तानों ने खानकाओं को कर मुक्त भूमि इनाम में दे दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। सूफी संत अनुदान में मिले धन और सामान का इस्तेमाल जरूरतमंदों के खाने, कपड़े एवं रहने की व्यवस्था तथा अनुष्ठानों के लिए करते थे। शासक वर्ग इन संतों की लोकप्रियता, धर्म निष्ठा और विद्वत्ता के कारण उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे।
प्रश्न 9. पिछली दो शताब्दियों में हंपी के भवनावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है? आपके अनुसार यह पद्धति विरुपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का किस प्रकार पूरक रहीं?
उत्तर: आधुनिक कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल हंपी है जिसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता मिली। हंपी के भवनावशेष 1800 ईसवी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कालिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, हंपी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा प्राप्त शुरुआती जानकारियां विरुपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी । कालांतर में 1856 ईसवी में एलेग्जेंडर ग्रनिलो ने हंपी के पुरातात्विक अवशेषों के विस्तृत चित्र लिए इसके परिणाम स्वरूप शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए।
1836 ईस्वी से ही अभिलेख कर्ताओं ने यहां और हंपी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के बृत्तांतो और तेलगु, कन्नड़, तमिल एवं संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया, इनसे उन्हें साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिली।
1876 ईसवी में जे.एफ. फ्लीट ने पुरास्थल के मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन प्रारंभ किया। जो विरुपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदत सूचनाओं की पुष्टि करता है। निसंदेह यह पद्धति विरुपाक्ष मंदिरों के पुरोहित द्वारा प्रदत सूचनाओं की पूरक थी।
प्रश्न 10. कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए?
उत्तर: मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। खेतिहर परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे जबकि महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी ।
पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी सहयोग प्रदान करती थी। वास्तव में मध्यकाल विशेष रुप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण इकाइयां एवं व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन तथा श्रम उत्पादन का प्रमुख आधार बन गया । अतः महिलाएं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचना कठिन हो गया था। उत्पादन के कुछ पहलू जैसे सूत कातना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थी। किसान और दस्तकार महिलाएं न केवल खेती के काम में सहयोग प्रदान करती थी अपितु आवश्यक होने पर नियोक्ताओं के घरों में भी काम करती थी और अपने उत्पादन के बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। उल्लेखनीय है कि श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता था क्योंकि उनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता थी।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. पुरातत्वविद हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वह कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं?
उत्तर: पुरातत्वविद संस्कृति विशेष के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां हैं शवान का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं की खोज ।
शवाधानो का अध्ययन - शवाधानो का अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने का महत्वपूर्ण तरीका है । उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों में जो शवाधान मिले हैं उनसे स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्यो अथवा गड्ढों में दफनाया जाता था। परंतु सभी गर्तो की बनावट एक जैसी नहीं थी । अधिकांश शवाधान गर्तौ की बनावट सामान्य थी, लेकिन कुछ की सतहों पर ईटों की चिनाई की गई थी। ईटों की चिनाई वाले गर्त उच्च अधिकारी वर्ग अथवा संपन्न शवाधान रहे होंगे। शवाधान गर्तो में शव सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाते थे। कुछ कब्रों में शव मृदभांडों और आभूषणों के साथ दफनाया मिले हैं और कुछ में तांबे के बर्तन, सीप और सुईया भी मिली है । कुछ स्थानों से बहुमुल्य आभूषण एवं अन्य समान मिले हैं, तो अनेक जगहों से सामान्य आभूषण की प्राप्ति हुई है । कालीबंगा में छोटे-छोटे वृत्ताकार गड्ढों में अन्न के दाने तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं कुछ गड्ढों में हड्डिया भी एकत्रित मिली हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीकों से कम से कम 3 तरीकों से किया जाता था। शव का सावधानीपूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री उनके साथ रखने जैसे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे।
विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना - सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता के अस्तित्व का पता लगाने की एक अन्य महत्वपूर्ण विधि विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना है। साधनों से उपलब्ध होने वाली पुरा वस्तुओं का अध्ययन करके पुरातत्वविद उन्हें दो वर्गों अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुओं में विभाजित करते हैं। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्किया, मृदभांड सुई आदि आती है । इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी पूर्वक बनाया जा सकता था। इस प्रकार की वस्तुएँ लगभग सभी हड़प्पा पुरास्थलों से प्राप्त हुई हैं। विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत बहुत महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएँ सम्मिलित थी। जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से एवं जटिल तकनीकों द्वारा किया जाता था। ऐसी वस्तुएँ मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगरों से ही मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा समाज में विद्यमान विभिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक स्थिति रहा होगा। उदाहरण के लिए कालीबंगा में प्रमाण से पता लगता है कि पुरोहित वर्ग दुर्ग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिका पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार पुरातत्वविद हड़प्पा समाज की सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातें जैसे लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति नगरों अथवा छोटी बस्तिओं में निवास, खानपान एवं रहन-सहन और साधनों से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य अथवा सामान्य वस्तुओं पर विशेष रुप से ध्यान देते थे।
प्रश्न 2. मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे?
उत्तर: छठी शताब्दी ई० पूर्व से चौथी शताब्दी ई. पूर्व तक एक प्रमुख शक्ति के रूप मे मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे:
1. भौगोलिक स्थिति : मगध की दोनो राजधानियों राजगृह गृह और पाटलिपुत्र - सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित थी। राजगीर पाँच पहाड़ियों से घिरा एक दुर्ग के समान था वही पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों तथा पुनपुन नदी से घिरे होने के कारण एक जलदुर्ग के समान था ।
2. लोहे के समृद्ध भंडार : मगध के दक्षिणी क्षेत्र आधुनिक झारखंड में लोहे के भंडार होने के कारण लोहे के हथियार एवं उपकरण आसानी से उपलब्ध थे।
3. उपजाऊ कृषि : मगध का क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफी उर्वर था । यहां के लोग अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर थे।
4. जलमार्ग से यातयात के साधन: गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के समीप होने के कारण जलमार्ग से यात्रा सस्ता एवं आसान था।
5. हाथी की उपलब्धता: इस क्षेत्र के घने जंगलो में हाथी काफी संख्या में पाये जाते थे जिनका युद्ध में काफी महत्व था। हाथी से दलदल स्थान तथा दुर्गो को तोड़ने में काफी सहायता मिलती थी।
6. योग्य शासक : मगध के आरंभिक शासक बिंबिसार, अज्ञातशत्रु और महापद्मनंद आदि अत्यधिक योग्य एवं महत्वाकांक्षी थे। इनकी नीतियों ने मगध का विस्तार किया।
प्रश्न 3. क्या यह संभव है की महाभारत का एक ही रचियता था?
उत्तर: महाभारत के रचनाकार के विषय में भी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। जनश्रुतियों के अनुसार महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ को श्रीगणेश जी से लिखवाया था। परंतु आधुनिक विद्वानों का विचार है कि इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुई। वर्तमान में इस ग्रंथ में एक लाख श्लोक हैं लेकिन शुरू में इसमें मात्र 8800 श्लोक ही थे । दीर्घकाल में रचे गए इन श्लोकों का रचयिता कोई एक लेखक नहीं हो सकता | विजयों का बखान करने वाली यह कथा परंपरा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रही। इतिहासकारों का अनुमान है कि पाँचवीं शताब्दी ई०पू० से इस कथा परंपरा को ब्राह्मण लेखकों ने अपनाकर इसे और विस्तार दिया। साथ ही इसे लिखित रूप भी दिया। यही वह समय था जब उत्तर भारत में क्षेत्रीय राज्यों और राजतंत्रों का उदय हो रहा था । कुरु और पांचाल, जो महाभारत कथा के केंद्र बिंदु हैं, भी छोटे सरदारी राज्यों से बड़े राजतंत्रों के रूप में उभर रहे थे। संभवत: इन्हीं नई परिस्थितियों में महाभारत की कथा में कुछ नए अंश शामिल हुए। यह भी संभव है कि नए राजा अपने इतिहास को नियमित रूप से लिखवाना चाहते हो अतः ऐसा मानना की महाभारत का एक ही रचियता था, संभव प्रतीत नहीं होता।
प्रश्न 4. स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? वर्णन कीजिए?
उत्तर: स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला, ढेर या थूहा होता है। स्तूप का संबंध मृतक के दाह संस्कार से था, मृतक के दाह संस्कार के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढंक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। क्योंकि इस स्तूप में पवित्र अवशेष रखे होते थे अतः समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। पहले मात्र भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बने बाद में बुद्ध के शिष्यों के अवशेषों पर भी स्तूप निर्मित किए गए।
स्तुपों की संरचना स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्ध गोलाकार मिलता है उसमें मेधी के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का थूहा पाया जाता है जिसे अंड कहते हैं, इस अंड की ऊपरी चोटी सिरे पर चपटी होती थी जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था इसे हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। हर्मिका का अर्थ देवताओं का निवास स्थान होता है।
स्तूप को चारों ओर से एक दीवार द्वारा घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा लगाने के लिए बना स्थल प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, कालांतर में वेदिका के चारों ओर चार दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए । प्रवेश द्वार पर मेहराबदार तोरण बनाए गए। इस प्रकार स्तूप की संरचना की गई।
प्रश्न 5. वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अलबरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए?
उत्तर: अरबी लेखक अलबरूनी ने भारत के विषय में अपनी पुस्तक 'किताब-उल-हिन्द' या 'तहकीक-ए-हिंद' में भारत की सामाजिक स्थिति, रीति-रिवाजों, भारतीय खान पान, वेशभूषा उत्सव, त्योहार आदि के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अपनी पुस्तक 'किताब-उल-हिंद' के नौवे अध्याय में अलबरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला है।
अलबरूनी के अनुसार भारतीय समाज चार वर्णों में बंटा हुआ था। 1. ब्राह्मण 2. क्षत्रिय 3. वैश्य 4. शूद्र ।
इन चारों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे। और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई थी । क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधे और हाथ से जबकि वैश्यों की उत्पत्ति जांघों से हुई थी। इसलिए समाज में ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का और उसके बाद वैश्यो का स्थान था। समाज के सबसे निचले स्थान पर शूद्र थे क्योंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई थी। प्रत्येक वर्ण, जाति और उप-जाति में बटा हुआ था ।
वर्ण और जाति-व्यवस्था के बाहर भी अनेक सामाजिक समूह थे जिन्हें अल- बरुनी 'अंत्यज' कहते हैं और इनकी स्थिति के बारे में बताते हुए अलबरूनी कहते हैं कि इनकी स्थिति शूद्रों से भी नीची थी। इनकी आठ जातियाँ थी धुनिये, मोची, मदारी, टोकरी और ढाल बनाने वाले, नाविक, मछली पकड़ने वाले, आखेट करने वाले एवं जुलाहे । ये नगरों और गांव के बाहर रहते थे। अंत्यजो से भी खराब स्थिति "गंदा काम" करने वाले लोगों का था। इसके अंतर्गत हादी, डोम, चांडाल और वधतू थे । ये चारों एक अलग सामाजिक वर्ग के थे । इनकी स्थिति अछूतों के समान थी। इन्हें सामान्यतः शुद्र पिता और ब्राह्मण माता की अवैध संतान माना जाता था। और इनका अन्य वर्गों तथा जाति के लोगों से सामाजिक संपर्क नहीं होता था।
प्रश्न 6. कबीर और बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए, इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ।
उत्तर: कबीर के मुख्य उपदेश निम्नलिखित हैं:-
1. कबीर के अनुसार परम सत्य अथवा परमात्मा एक हैं भले ही विभिन्न संप्रदायों के लोग उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं।
2. उन्होंने परमात्मा को निरंकार बताया ।
3. उनके अनुसार भक्ति के माध्यम से मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
4. उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया।
5. उन्होंने जाति- पाती, भेदभाव, ऊंच-नीच, छुआछूत आदि का विरोध किया।
कबीर ने अपने विचारों को काव्य की आम बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया जिसे आसानी से समझा जा सकता था । उनके देहांत के बाद उनके अनुयायियों ने अपने प्रचार प्रसार द्वारा उनके विचारों का संप्रेषण किया।
बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश:-
1. उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया।
2. धर्म के सभी बाहरी आडंबर को उन्होंने अस्वीकार किया। जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप।
3. उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकारा।
4. उन्होंने रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप ।
उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा शब्द के माध्यम से सामने रखें। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग-अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रकाब बजाकर उनका साथ देता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कबीर और बाबा गुरु नानक के उद्देश्यों को लोगों ने हाथों हाथ लिया।
प्रश्न 7. विट्ठल मंदिर तथा विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य कला पर प्रकाश डालें!
उत्तर: विजयनगर में बड़े पैमाने पर मूर्तियों तथा मंदिरों का निर्माण कराया गया। मंदिर स्थापत्य राजकीय सत्ता की पहचान थी, जिन्होंने विशाल संरचनाओं का निर्माण कराया । इसका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। यह संभवतः शासकों की ताकत का एहसास भी दिलाते थे क्योंकि वह इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने हुए थे, सम्मिलित हैं जिसमें विरुपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर प्रमुख है।
विरुपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। इसका सबसे प्रसिद्ध मंदिर नवी दसवीं शताब्दीयों का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे और अधिक बड़ा दिया गया । मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। सभागारों का प्रयोग देवी- देवताओं के विवाह के अवसर पर आनंद मनाने और कुछ अन्य देवी- देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था। यह छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी।
दूसरा देवस्थान विट्ठल मंदिर था, जहां के प्रमुख देवता विट्ठल थे। सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। इस देवता की पूजा कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग-अलग परंपराओं को आत्मसात किया । अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का अनूठा मंदिर भी है। मंदिर परिसर की एक विशेषता रथ गलियां है जो मंदिर को गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं । इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे।
जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा उसे और अधिक व्यापक बनाया वैसे ही उन्होंने मंदिरों के निर्माण की परंपराओं को कायम रखा। कुछ दर्शनीय गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया।
प्रश्न 8. पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे? विवेचना कीजिए ।
उत्तर: 16 वीं और 17 वीं शताब्दी के काल में ग्रामीण समाज में पंचायत और मुखिया का पद बहुत महत्वपूर्ण था। ये दोनों पद ग्रामीण समाज की रीढ़ की हड्डी थी ।
पंचायतों का गठन- मुगलकालीन गाँव की पंचायत गांव बुजुर्गों की सभा होती थी । प्रायः वे गाँव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे। जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी जिन गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे । वहां पंचायतों में विविधता पाई जाती थी । पंचायत का निर्णय गाँव में सब को मानना पड़ता था।
पंचायत का मुखिया - पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। कुछ स्रोतों से प्रतीत होता है कि मुखिया का चुनाव गाँव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था | चुनाव के बाद उन्हें उसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी । मुखिया तब तक अपने पद पर बना रहता था। जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था । गांव की आय-व्यय का हिसाब किताब अपनी निगरानी में तैयार करवाना मुखिया का मुख्य काम था। इस काम में पंचायत का पटवारी उसकी सहायता करता था।
पंचायत का आम खजाना - पंचायत का खर्चा गांव की आम खजाने से चलता था इसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस कोष का प्रयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी होता था । इस कोष से ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए भी खर्च होता था जो किसान स्वयं नहीं कर सकते थे ।जैसे कि मिट्टी के छोटे-मोटे बांध बनाना या नहर खोदना।
ग्रामीण समाज का नियमन - पंचायत का एक बड़ा काम यह देखना था कि गांव में रहने वाले सभी समुदाय के लोग अपनी जाति की सीमाओं के अंदर रहे । पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की उपस्थिति में होती थी ।जाति की अवहेलना को रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की एक
महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी।
पंचायतों को जुर्माना लगाने तथा किसी दोषी को समुदाय से निष्कासित करने जैसे अधिकार प्राप्त थे। समुदाय से बाहर निकलना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था । इसके अंतर्गत दंडित व्यक्ति को दिए गए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति तथा व्यवसाय से हाथ धो बैठता था । ऐसे नीतियों का उद्देश्य जातिगत रिवाजों की अवहेलना को रोकना था।
प्रश्न 9. मुग़ल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने?
उत्तर: मुग़ल राज्य का महत्त्वपूर्ण स्तम्भ अधिकारियों का दल था जिसे इतिहासकारों ने सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग की संज्ञा से परिभाषित किया है। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था जो वफ़ादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे।
साम्राज्य के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूँ के साथ भारत चले आए थे। कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों-राजपूतों व भारतीय मुसलमानों (शेखजादाओं) ने शही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया आंबेर का राजा भारमल कछवाहा था। जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था।
शिक्षा और लेखाशास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्तमंत्री टोडरमल का है जो खत्री जाति का था। जहाँगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहाँगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहाँ (1645) ईरानी थी औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया।
फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी-खासी संख्या में थे। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक रिया थी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभि र याचिका देता था जो बादशाह के सामने तजवीज प्रस्तुत करता था। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। मीरबख्शी (उच्चतम वेतन दाता) खुले दरबार में बादशाह के दाएँ ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ-साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था।
केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे दीवान ए आला (वित्त मंत्री) और सद्र उस सुदूर (मदद ए मास अथवा अनुदान विभाग मंत्र और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी) यह तीन मंत्री कभी-कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे लेकिन यह एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक राजकोषीय और मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया।
दरबार में नियुक्त (तैनात ए रकाब) अभिजातों का एक ऐसा समूह था जिसे किसी भी प्रान्त या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वह शासक और उसके घराने की सुरक्षा भी करता था।
प्रश्न 10. इस्तमरारी बंदोवस्त के बाद बहुत-सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गयी?
उत्तर: इस्तमरारी व्यवस्था में सरकार जमींदारों की भूमि का कुछ भाग बेचकर लगान की वसूली कर सकती थी । इस्तमरारी बन्दोबस्त के बाद बहुत सी ज़मींदारियां नीलाम की जाने लगी।
इसके अनेक कारण थे:-
1. कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारंभिक राजस्व माँगें अत्यधिक ऊँची थीं। स्थायी अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत राज्य की राजस्व माँग का निर्धारण स्थायी रूप से किया गया था। इसका तात्पर्य था कि आगामी समय में कृषि में विस्तार तथा मूल्यों में होने वाली वृद्धि का कोई अतिरिक्त लाभ कंपनी को नहीं मिलने वाला था। अतः इस प्रत्याशित हानि को कम-से-कम करने के लिए कंपनी राजस्व की माँग को ऊँचे स्तर पर रखना चाहती थी। ब्रिटिश अधिकारियों का विचार था कि कृषि उत्पादन एवं मूल्यों में होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप ज़मींदारों पर धीरे-धीरे राजस्व की माँग का बोझ कम होता जाएगा और उन्हें राजस्व भुगतान में कठिनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। किंतु ऐसा संभव नहीं हो सका । परिणामस्वरूप ज़मींदारों के लिए राजस्व - राशि का भुगतान करना कठिन हो गया।
2. उल्लेखनीय है कि भू-राजस्व की ऊँचीं माँग 1790 की दशक में लागू की गई थी। इस काल में कृषि उत्पादों की कीमतें कम थी, जिससे रैयत (किसानों) के लिए, जमींदार को उनकी देय राशियाँ चुकाना मुश्किल था। इस प्रकार जमींदार किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता था और कंपनी को अपनी निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता था।
3. राजस्व की माँग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। उत्पादन अधिक हो या बहुत कम, राजस्व का भुगतान ठीक समय पर करना होता था। इस संबंध में सूर्यास्त कानून का अनुसरण किया जाता था । इसका तात्पर्य था कि यदि निश्चित तिथि को सूर्य छिपने तक भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदारियों को नीलाम किया जा सकता था।
4. इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों के अनेक विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। उनके सीमाशुल्क वसूल करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उन्हें उनकी स्थानीय न्याय तथा स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति से भी वंचित कर दिया गया। परिणामस्वरूप अब ज़मींदार शक्ति प्रयोग द्वारा राजस्व वसूली नहीं कर सकते थे।
5. राजस्व वसूली के समय जमींदार का अधिकारी जिसे सामान्य रूप से 'अमला' कहा जाता था, ग्राम में जाता था। कभी कम मूल्यों और फसल अच्छी न होने के कारण किसान अपने राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते थे, तो कभी रैयत जानबूझकर ठीक समय पर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। इस प्रकार जमींदार ठीक समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पाता था और उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी।
6. कई बार ज़मींदार जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। भूमि के नीलाम किए जाने पर उनके अपने एजेन्ट कम से कम बोली लगाकर उसे (अपने ज़मींदार के लिए) प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार ज़मींदार को राजस्व के रूप में पहले की अपेक्षा कहीं कम धनराशि का भुगतान करना पड़ता था।







 Profile
Profile Signout
Signout










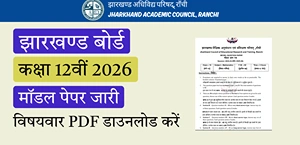

 Quiz
Quiz
 Get latest Exam Updates
Get latest Exam Updates 










