राजस्थान बोर्ड 12th Exam 2023 : History - इतिहास, महत्वपूर्ण प्रश्न Solution के साथ
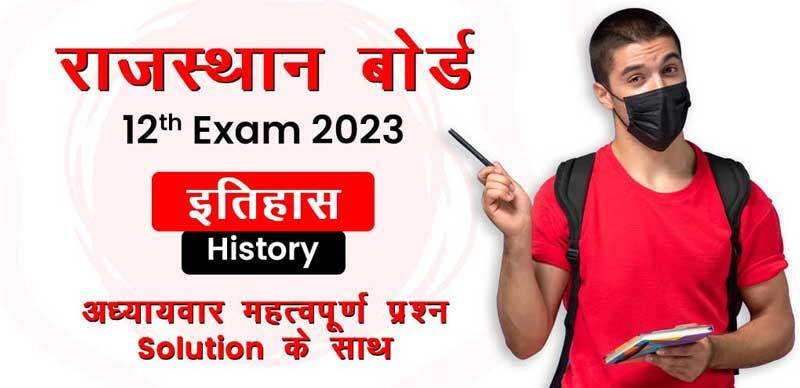
SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
राजस्थान बोर्ड 12th Exam 2023 : History - इतिहास, महत्वपूर्ण प्रश्न Solution के साथ
यहां History - इतिहास 12वी Exam 2023 के लिए New Blue Print पर आधारित Most Important Question दिए गए है. ये महत्वपूर्ण Question Study Material के रूप में तैयार किये गए I
जो आपके Paper के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये Most Important Question तैयारी को और बेहतर बना सकते है I
Most Important Question
खंड 'अ'
Q.1. बहुविकल्पीय प्रश्न
i. हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें किस पत्थर से बनाई गई थी?
(अ) जैस्पर
(ब) चर्ट
(स) स्फटिक
(द) सेलखड़ी
Ans. हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवर के चित्र तथा एक ऐसे लिपि के चिह्न उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
ii. प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी?
(अ) शक
(स) सातवाहन
(ब) मौर्य
(द) वाकाटक
Ans. प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी । उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था।
iii. श्लोकों की तुलना करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों को कितना समय लगा?
(अ) 15 वर्ष
(ब) 19 वर्ष
(स) 21 वर्ष
(द) 47 वर्ष
Ans. 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी. एस. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे।
iv. खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी?
(अ) गुरु नानक
(ब) गुरु अंगद
(स) अमरदास
(द) गुरु गोबिंद सिंह
Ans. गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली और उनके पांच प्रतीकों का वर्णन किया: बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा | गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया।
v. विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया था?
(अ) फर्नावो नूनिज़
(ब) कर्नल कॉलिन मैकेन्जी
(स) डोमिंगो पेस
(द) अब्दुर रज़्ज़ाक
Ans. हंपी के भग्नावशेष 1800 ई. में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, उन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया।
vi. भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था?
(अ) दुआर्ते बरबोसा
(ब) डोमिंगो पेस
(स) फर्नावो नूनिज़
(द) कर्नल कॉलिन मैकेन्जी
Ans. 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया।
vii. आइन-ए-अकबरी की रचना किसने की थी?
(अ) अबुल फ़ज़्ल
(स) अमीर खुसरो
(ब) अल बिरूनी
(द) इब्नबतूता
Ans. अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फ़ज़्ल ने आईन -ए-अकबरी की रचना की, जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है।
viii मुग़लकाल का “रज़्मनामा" किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है?
(अ) रामायण
(स) पुराण
(ब) महाभारत
(द) उपनिषद्
Ans. मुग़ल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फ़ारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया । महाभारत का अनुवाद रज्मनामा (युद्धों की पुस्तक) के रूप में हुआ ।
ix. "बंगाल आर्मी की पौधशाला" किस रियासत को कहा जाता था?
(अ) कानपुर
(स) अवध
(ब) झाँसी
(द) रंगपुर
Ans. बंगाल आर्मी के सिपाहियों में बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या "ऊंची जाति" के थे। अवध को "बंगाल आर्मी की पौधशाला" कहा जाता था।
X. भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारम्भ किया गया था?
(अ) 1935 में
(ब) 1942 में
(स) 1939 में
(द) 1946 में
Ans. क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू किया गया था।
xi. संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे?
(अ) 5 सत्र
(स) 15 सत्र
(ब) 11 सत्र
(द) 23 सत्र
Ans. संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए जिनमें 165 दिन बैठकों में गए | सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मस्विदे को सुधारने और संवारने का काम करती थी।
xii. निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सामने "उद्देश्य प्रस्ताव " पेश किया था?
(अ) पंडित जवाहरलाल नेहरु
(स) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(ब) वल्लभभाई पटेल
(द) महात्मा गाँधी
Ans. संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन छह में से तीन- जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, " उद्देश्य प्रस्ताव" को नेहरू ने पेश किया था।
Q.2. रिक्त स्थान की पूर्ति करो-
i. सोलह महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद ______ था।
Ans. मगध
ii. हिन्दू धर्म की एक परम्परा वैष्णव है तो दूसरी_____है।
Ans. शैव
iii. सहायक संधि______द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी।
Ans. लॉर्ड वेलेज़्ली
iv. मोहनदास करमचंद गाँधी विदेश में दो दशक रहने के बाद________ में अपनी गृहभूमि वापस आए।
Ans. जनवरी 1915
V. मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार_____ईसवी में लागू किए गए।
Ans. 1919
Q.3. अति लघुउत्तरीय प्रश्न
i. भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है?
Ans. अलेक्जैंडर कनिंघम को ।
ii. धर्मशास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार वैश्यों को कौनसे कार्य करने अपेक्षित थे?
Ans. वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान-दक्षिणा देना तथा कृषि, गौ-पालन करना और व्यापार अपेक्षित था।
iii. महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब व किसके नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ ?
Ans. 1919 ई. में वी. एस. सुकथांकर के नेतृत्व में।
iv. “किताब-उल-हिन्द" नामक कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना हैं? यह कौनसी भाषा में लिखी गयी है?
Ans. अरबी भाषा में लिखित " किताब - उल - हिन्द" नामक कृति 'अल- बिरूनी' की रचना हैं।
v.अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे, तो वहाँ स्थित किस सूफ़ी संत के दरगाह की ज़ियारत करेंगे?
Ans. शेख मुइनुद्दीन चिश्ती।
vi. हम्पी नाम का आविर्भाव किस स्थानीय देवी के नाम से हुआ था?
Ans. पम्पा देवी ।
vii. फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा क्यों और किसने बनवाया था?
Ans. अकबर द्वारा, गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में
viii. ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में कौनसा क़िला बनवाया था?
Ans. फ़ोर्ट सेंट जॉर्ज ।
ix. सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की माँग किसने की थी?
Ans. कवि मोहम्मद इकबाल ।
X. 1971 में बंगाली मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लेकर जिन्ना के किस सिद्धांत को नकार दिया गया था?
Ans. द्विराष्ट्र सिद्धांत।
xi. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौनसी क्रांतियों का हवाला देते हुए संविधान निर्माण के इतिहास को तिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध किया?
Ans. अमेरिकी और फ्रांसिसी क्रांति ।
xii. संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था?
Ans. सोमनाथ लाहिड़ी ।
खण्ड 'ब'
लघुउत्तरीय प्रश्न
Q.4.महाभारत की भाषा एवं विषयवस्तु पर टिप्पणी लिखिए।
Ans. महाभारत की भाषा :- महाभारत संस्कृत भाषा में है किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत, वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है।
विषयवस्तु :- इतिहासकार इस ग्रंथ की विषयवस्तु को दो मुख्य शीर्षकों-आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार-विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है - उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है।
Q.5.साँची कनखेड़ा की इमारतों की खोज में अलेक्ज़ेंडर कनिंघम के योगदान का उल्लेख कीजिए ।
Ans. भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत साँची कनखेड़ा की इमारतें हैं। बुद्ध की मूर्तियाँ और प्राचीन तोरणद्वार के अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं। मेजर अलेक्ज़ेंडर कनिंघम इस इलाके में कई हफ़्तों तक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढाँचे के बीचों-बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेज़ी पुस्तक में लिखा है, भोपाल की नवाब (शासनकाल 1868-1901), शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा "ताज-उल-इकबाल तारीख भोपाल " (भोपाल का इतिहास) से। 1876 में एच.डी. बारस्टो ने इसका अनुवाद किया।
Q.6. "प्रथम सहस्राब्दि ईसा पूर्व का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।" व्याख्या कीजिए ।
Ans. ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दि का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ-साथ वे इनसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये मनीषी सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे।
Q.7. जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है?
Ans. जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा - खासकर इनसानों, जानवरों, पेड़-पौधों और कीड़े-मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। जैन साधु और साध्वी पाँच व्रत करते थे: हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य (अमृषा) और धन संग्रह न करना।
Q.8. "किताब-उल-हिन्द" पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ।
Ans. अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब-उल-हिन्द की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक- जीवन, भार-तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर अस्सी अध्यायों में विभाजित है।
लेखन की विशिष्ट शैली :- सामान्यत: अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना ।
Q.9. फ्रांस्वा बर्नियर ने "पूर्व" व "पश्चिम" की तुलना किस प्रकार की?
Ans. बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे।
वह सामान्यत: भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई XIV को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया।
Q.10. कर्नल कॉलिन मैकेन्जी ने किस रूप में प्रसिद्धि हासिल की?
Ans. 1754 ई. में जन्मे कॉलिन मैकेन्जी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक, तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया।
Q.11. सोलहवीं एवं सत्रहवीं सदी के आरंभ में कृषि समाज के इतिहास को जानने के स्रोत कौन-कौनसे हैं ?
Ans. सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों के कृषि इतिहास के मुख्य स्रोत :-
i. आइन-ए-अकबरी :- सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ "आइन-ए- अकबरी" में खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोशों यानी कि ज़मींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा-जोखा पेश किया गया है।
ii. गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान से प्राप्त महत्वपूर्ण दस्तावेज़ :- मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए सत्रहवीं व अठारहवीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज़ सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं।
iii. ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज :- ये पूर्वी भारत में कृषि-संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, ज़मींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं।
Q.12. अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया ?
Ans. अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण :-
i. पोलज वह ज़मीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है।
ii. परौती वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोयी ताकत वापस पा सके।
iii. चचर वह ज़मीन है जो तीन या चार वर्षों तक खाली रहती है।
iv. बंजर वह ज़मीन है जिस पर पाँच या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो।
Q.13. मुग़लकालीन प्रांतीय प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Ans. मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन : केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों (सूबों) में दुहराया गया था। केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ (दीवान, बख्शी और सद्र) होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर (सूबेदार) होता था जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बंटा हुआ था। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देख-रेख तीन अर्ध- वंशानुगत अधिकारियों, कानूनगो, चौधरी और काज़ी द्वारा की जाती थी।
Q.14. इस्तमरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हों? यह बंदोबस्त सर्वप्रथम कब तथा कहाँ पर लागू किया गया था ?
Ans. अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम बंगाल में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया गया था तथा वहाँ भूमि संबंधी अधिकारों की नयी व्यवस्था तथा एक नयी राजस्व प्रणाली लागू की गई। जिसके तहत सन् 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक ज़मींदार को अदा करनी होती थी। जो ज़मींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएँ नीलाम कर दी जाती थीं, इसे ही इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है।
Q.15. जोतदारों की स्थिति क्या थी? वे ज़मींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे?
Ans. उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते-आते, जोतदारों ने ज़मीन के बड़े-बड़े रकबे, जो कभी-कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। गाँवों में, जोतोदारों की शक्ति, ज़मींदारों की ताक़त की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जोतदार ग़रीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। ज़मींदार अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे; जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और ज़मींदार को राजस्व के भुगतान में जान-बूझकर देरी करा देते थे। जब ज़मींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अकसर जोतदार ही उन जमीनों को ख़रीद लेते थे।
Q.16. आपके अनुसार भारत विभाजन के लिए कौनसी परिस्थितियों उत्तरदायी थीं ?
Ans. अंग्रेज़ 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर चल रहे थे। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों, साहित्य, लेखों तथा भारतीय मध्यकालीन इतिहास की घटनाओं का बार-बार जिक्र किया जिन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाया। 23 मार्च, 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
i. मुसलमानों में मस्जिदों के सामने संगीत बजाए जाने, गोरक्षा-आन्दोलन तथा शुद्धिकरण आदि कार्यों से तीव्र आक्रोश व्याप्त था।
ii. 1909 के मार्ले-मिण्टों सुधारों में मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई जिसका साम्प्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा।
iii. 1937 में सम्पन्न हुए चुनावों के बाद संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परन्तु कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिससे मुसलमानों के मन में निराशा उत्पन्न हुई।
iv. सांप्रदायिक दंगे भी विभाजन का कारण बने । 16 अगस्त, 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की माँग पर बल देते हुए 'प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस' मनाया। उस दिन कलकत्ता में भीषण दंगा भड़क उठा तथा विभाजन अपरिहार्य हो गया।
खंड 'स'
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
Q.17. मौर्य काल में सैनिक गतिविधियों के संचालन का उल्लेख कीजिए ।
Ans. मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और छ: उपसमितियों का उल्लेख किया है :-
i. प्रथम उप-समिति का काम नौसेना का संचालन करना था।
ii. दूसरी यातायात और खान-पान का संचालन करती थी।
iii. तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था।
iv. चौथी का अश्वारोहियों का संचालन करना तथा
v. पाँचवी का रथारोहियों का संचालन करना और
vi. छठी का काम हाथियों का संचालन करना था।
दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था : उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना।
Q.18. भक्ति आंदोलन में "महान" और "लघु" परंपराओं पर टिप्पणी लिखिये।
Ans. "महान" और "लघु" जैसे शब्द बीसवीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। महान परंपराएँ :- किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने "महान" परंपरा की संज्ञा दी।
लघु परंपराएँ :- कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें "लघु" परंपरा के नाम से अभिहित किया। महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण परिवर्तन हुए।
Q.19. 1857 के विद्रोह ने किस प्रकार वैधता हासिल कर ली ?
Ans. 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए।
दिल्ली पर नियंत्रण तथा विद्रोह द्वारा वैधता की प्राप्ति :- अँधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ़ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल क़िले के फाटक पर पहुँचा। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि "हम मेरठ के सभी अंग्रेज़ पुरुषों को मारकर आए हैं क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दाँतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान, सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।" सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए, दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल क़िले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी माँग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली क्योंकि अब उसे मुग़ल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था।
Q.20. आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ?
Ans. अठारहवीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन :-
i. राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा।
ii. मुग़ल सत्ता के क्रमिक शरण के कारण ही उसके शासन से सम्बद्ध नगरों का अवसान हो गया।
iii. मुग़ल राजधानियों, दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया।
iv. नयी क्षेत्रीय ताकतों का विकास क्षेत्रीय राजधानियों लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्म, पूना, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर के बढ़ते महत्त्व में परिलक्षित हुआ।
v. व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुग़ल केन्द्रों से इन नयी राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे।
vi. नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिकों को भी यहाँ तैयार रोजगार मिलता था।
vii. कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुग़ल साम्राज्य से सम्बद्ध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग 'कस्बे' और 'गंज' जैसी नयी शहरी बस्तियों को बसाने में किया।
viii. कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी, कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूट-पाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणित हुई।
ix. व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केन्द्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए।
खण्ड 'द'
निबन्धात्मक प्रश्न
Q.21. सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए?
Ans. हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। पहले चबूतरों का यथास्थान निर्माण किया गया उसके बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर इसके अनुसार कार्यान्वयन ।
नगर नियोजन की विशेषताएँ निम्नलिखित है :-
i.बस्ती का विभाजन :- मोहनजोदड़ो की बस्ती दो भागों में विभाजित थी।
दुर्ग तथा निचला शहर :- एक छोटा भाग ऊँचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा भाग नीचे बनाया गया। जिन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊँचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे।
ii. ईंटें :- नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो धूप सुखाकर या भट्टी में पकाकर एक निश्चित अनुपात में निर्मित की गई थी। इन ईंटों की लंबाई और चौड़ाई, ऊँचाई की क्रमशः चारगुनी और दोगुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थीं।
iii. नियोजित जल निकासी प्रणाली :- हड़प्पाई शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता "नियोजित जल निकास प्रणाली" थी। पहले नालियों का निर्माण किया गया उसके साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल-बगल आवासों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की एक दीवार गली से सटी हुई बनाई गई थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक "ग्रिड" पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
iv.गृहस्थापत्य :-
आँगन पर केंद्रित कमरे :- मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आँगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। ये कमरे खाना पकाने और कताई करने के काम आते थें।
एकांतता को महत्व :- लोगों द्वारा अपनी एकांतता को महत्व दिया जाता था। उदाहरणार्थ :-
(1) भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं।
(2) मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आँगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है।
स्नानघर :- हर घर का ईंटों के फ़र्श से बना अपना एक स्नानघर होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों जुड़ी हुई थीं।
बहुमंजिला मकान :- कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे, जो इस बात का संकेत है कि मकान बहुमंजिला भी होते थे।
कुएँ :- कई आवासों में कुएँ थे जो अधिकांशत: एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका
प्रयोग संभवत: राहगीरों द्वारा किया जाता था । विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी।
v. माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार :- दुर्ग में ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवत: विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवत: लकड़ी से बने हुए थे, बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। मोहनजोदड़ो से आँगन में बना एक आयताकार जलाशय प्राप्त हुआ है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष आनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था।
अथवा
"हड़प्पाई शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता नियोजित जल निकास प्रणाली थी । " व्याख्या कीजिये ।
Ans. हड़प्पाई शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता नियोजित जल निकास प्रणाली थी। पहले नालियों का निर्माण किया गया उसके साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की एक दीवार गली से सटी हुई बनाई गई थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक "ग्रिड" पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
नालियों के विषय में 'मैके' लिखते है : "निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है" हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफ़ाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढँकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थीं जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों पर कुछ अंतरालों पर सफ़ाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थीं। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये छोटी बस्तियों में भी मिली थी। लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थीं।
Q.22. "1919 तक महात्मा गाँधी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभर चुके थे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी।" उदाहरण सहित कथन को सिद्ध कीजिए ।
Ans. गाँधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति :- पहली महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। जब गाँधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों को ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि :-
i. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 'निश्चय ही अत्यंत शानदार' है किंतु उन्होंने वहाँ धनी व सजे-सँवरे भद्रजनों की उपस्थिति और 'लाखों गरीब' भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की ।
ii. गाँधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि 'भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें' ।
iii. 'हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग सम्पूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है।
गाँधी जी की मंशा :- भारतीय राष्ट्रवाद को सम्पूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गाँधी जी की स्वयं की इच्छा की यह प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गाँधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला।
गाँधी जी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक के आंदोलन :-
i. चंपारन सत्याग्रह :- दिसम्बर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारन से आए एक किसान ने उन्हें वहाँ अंग्रेज़ नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गाँधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ-साथ अपनी पसंद की फ़सल उपजाने की आजादी दिलाने में बीता।
ii. अहमदाबाद मिल-मजदूर आंदोलन :- 1918 में गाँधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में दो अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की माँग की।
iii. खेड़ा सत्याग्रह :- खेड़ा में फ़सल चौपट होने पर गाँधी जी ने राज्य से किसानों का लगान माफ़ करने की माँग की। चंपारन, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गाँधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे।
iv. रॉलेट एक्ट :- 1914-18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जाँच के कारावास की अनुमति दे दी थी। विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गाँधी जी ने देशभर में 'रॉलेट एक्ट' के खिलाफ एक अभियान चलाया। रॉलेट सत्याग्रह से गाँधी जी एक सच्चे राष्ट्री नेता बन गए।
अथवा
महात्मा गाँधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारणों व आंदोलन के कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए ।
Ans. चंपारन, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गाँधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें ग़रीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। असहयोग आंदोलन के कारण :-
i. रॉलेट एक्ट :- 1914-18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जाँच के कारावास की अनुमति दे दी थी। विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गाँधी जी ने देशभर में 'रॉलेट एक्ट' के खिलाफ एक अभियान चलाया। रॉलेट सत्याग्रह से गाँधी जी एक सच्चे राष्ट्री नेता बन गए।
ii. जलियाँवाला बाग हत्याकांड : पंजाब में, विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेज़ों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे ईनाम की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गाँधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेसजनों को गिरफ़्तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे-धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खूनखराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुँच गई। जब एक अंग्रेज़ ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया तब जलियाँवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में चार सौ से अधिक लोग मारे गए। रॉलेट सत्याग्रह से ही गाँधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए।
असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम :- रॉलेट सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर गाँधी जी ने अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ 'असहयोग' अभियान की माँग कर दी। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएँ तथा कर न चुकाएँ। संक्षेप में सभी को अंग्रेज़ी सरकार के साथ (सभी) ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया।
स्वराज की प्राप्ति :- गाँधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा।
गाँधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाना :- अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफ़त आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व-इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की माँग कर रहा था। गाँधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय - हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे।
असहयोग आंदोलन की प्रगति :-
i. विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया।
ii. वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया।
iii. कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया।
iv.सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्यदिवसों का नुकसान हुआ था।
v. देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए । कुमाऊँ के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। विरोध आंदोलनों द्वारा स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ 'असहयोग' के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की।
असहयोग आंदोलन का प्रभाव :- असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व- अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणामस्वरूप अंग्रेज़ी राज की नींव हिल गई ।
चौरी-चौरा कांड असहयोग आंदोलन का अंत :- फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी-चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गाँधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा।
सरकार द्वारा आंदोलन का दमन तथा गाँधी जी गिरफ़्तारी :- असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गाँधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया। उन पर जाँच की कार्रवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस सी. एन. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्त्वपूर्ण भाषण दिया । "इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैने आज तक जिनकी जाँच की है अथवा करूंगा आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूँकि गाँधी जी ने कानून की अवहेलना की थी अतः उस न्याय पीठ के लिए गाँधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि 'यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा" ।
Rajasthan Board Study Material
| Rajasthan Board Study Material | |
| Rajasthan Board Class 12 Syllabus 2022-23 | RBSE Textbook Solutions |
| Rajasthan Board Class 12th Model Paper | RBSE Previous Year Question Papers |







 Profile
Profile Signout
Signout

















 Quiz
Quiz
 Get latest Exam Updates
Get latest Exam Updates 










