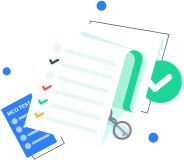प्रश्नानुवाद - 'पीताम्बरः' यहाँ समास है-
स्पष्टीकरण -
- शब्द - पीताम्बरः
- अर्थ - पीला वस्त्र
- समासविग्रह - पीतम् अम्बरं यस्य सः (श्रीकृष्णः)
सूत्र - अनेकमन्यपदार्थे।
- नियम - जब दो या दो से अधिक सभी शब्द किसी अन्य शब्द का बोध कराते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इस समास को अन्यपद प्रधान समास भी कहते हैं।
उदाहरण -
- चक्रं पाणौ यस्य सः - चक्रपाणिः (विष्णुः)
इसी नियमानुसार पीताम्बर पद में बहुव्रीहि समास है, जहाँ दोनों पद अन्य शब्द का बोध करा रहे हैं।
अतः यहाँ बहुव्रीहि समास सही उत्तर है।
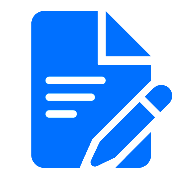 Additional Information
Additional Information
समसनं समासः अर्थात् संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। समास एक संज्ञा है। दो या दो से अधिक शब्दों का जब समास होकर एक पद बनता है, तो उसे समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं - 1. पूर्व पद, 2. उत्तर पद
समास के मुख्यतः 4 भेद है।
- अव्ययीभाव
- तत्पुरुष
- बहुव्रीहि
- द्वन्द्व
(1) अव्ययीभाव समास - ‘पूर्वपदार्थप्रधानोSव्ययीभावः’ अर्थात् जिस पद में पूर्व पद की प्रधानता हो या पद का आरम्भ किसी अव्यय पद से हो रहा हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है।
उदाहरण -
- रूपस्य योग्यम् - अनुरूपम्
- रामस्य पश्चात् - अनुरामम्
(2) तत्पुरुष समास - ‘उत्तरपदप्रधानो तत्पुरुषः’ अर्थात जिस पद में उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है।
उदाहरण -
- सुखम् आपन्नः - सुखापन्नः
- कूपं पतितः - कूपपतितः
तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं -
- व्यधिकरण तत्पुरुष समास
- समानाधिकरण तत्पुरुष
1. व्यधिकरण तत्पुरुष समास के सात (7) भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं -
द्वितीया तत्पुरुष - जहाँ श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न इन शब्दों का संयोग होता है, वहाँ द्वितीया तत्पुरुष समास होता है।
उदाहरण -
तृतीया तत्पुरुष - जहाँ तृतीयान्त शब्द के साथ पूर्व, सदृश, सम शब्द आता है, तो वहाँ तृतीया तत्पुरुष समास होता है।
उदाहरण -
चतुर्थी तत्पुरुष - जहाँ पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में होता है अथवा बलि, हित, सुख, रक्षित इन शब्दों को संयोग होता है, वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है।
उदाहरण -
- ब्राह्मणाय हितम् - ब्राह्मणहितम्
पञ्चमी तत्पुरुष - जहाँ भय, भीत, भीति इन शब्दों का संयोग होता है, वहाँ पञ्चमी तत्पुरुष समास होता है।
उदाहरण -
- व्याघ्राद् भीतिः - व्याघ्रभीतिः
षष्ठी तत्पुरुष - जब पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में होता है, तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है।
उदाहरण -
सप्तमी तत्पुरुष - जब पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में रहता है अथवा शौण्ड (चतुर), धूर्त, कितव (शठ), प्रवीण, कुशल, पण्डित इन शब्दों का संयोग होता है, तो वहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है।
उदाहरण -
- सभायां पण्डितः - सभापण्डितः
नञ् तत्पुरुष - जब पूर्व पद न शब्द हो, तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो, वहाँ नञ् तत्पुरुष समास होता है।
उदाहरण -
2. समानाधिकरण तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं -
- कर्मधारय तत्पुरुष
- द्विगु तत्पुरुष समास
(1) कर्मधारय तत्पुरुष समास - ऐसा तत्पुरुष समास जहाँ विशेषण-विशेष्य और उपमान-उपमेय का सम्बन्ध होता है, वह कर्मधारय समास होता है।
उदाहरण-
- पीतम् उत्पलम् - पीतोत्पलम्
- घन इव श्यामः - घनश्यामः
(2) द्विगु तत्पुरुष समास - जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। यह तत्पुरुष समास का ही भेद है।
उदाहरण -
- त्रयानां भुवनानां समाहारः - त्रिभुवनम्
- चतुर्णां भुजानां समाहारः - चतुर्भुजम्
(3) बहुव्रीहि समास - ‘अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः’ जहाँ दो या दो से अधिक समस्त शब्द किसी अन्य पद को इंगित करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है।
उदाहरण -
- महान् आत्मा यस्य सः (बुद्धः) - महात्मा
- दश आननानि यस्य सः (रावणः) - दशाननः
बहुव्रीहि समास के दो भेद हैं-
- समानाधिकरण बहुव्रीहि- (जहाँ दोनों शब्द प्रथमान्त होते हैं। जैसे - पीतम् अम्बरम् यस्य सः)
- व्यधिकरण बहुव्रीहि - (जहाँ दोनों शब्द प्रथमान्त नहीं होते हैं। एक प्रथमान्त होता है और दूसरा शब्द षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होता है। जैसे - चन्द्र शेखरे यस्य सः)
(4) द्वन्द्व समास - ‘उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः’ जहाँ दोनों पद (पूर्व पद एवं उत्तर पद) प्रधान होते हैं, वहाँ द्वन्द्व समास होता है।
उदाहरण -
- रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च - रामलक्ष्मणभरताः
- पाणी च पादौ च - पाणिपादम्


 Get latest Exam Updates
Get latest Exam Updates 
 ×
×