CGBSE Chhattisgarh Board 12th Exam 2024 : Economics Important Question with Answers
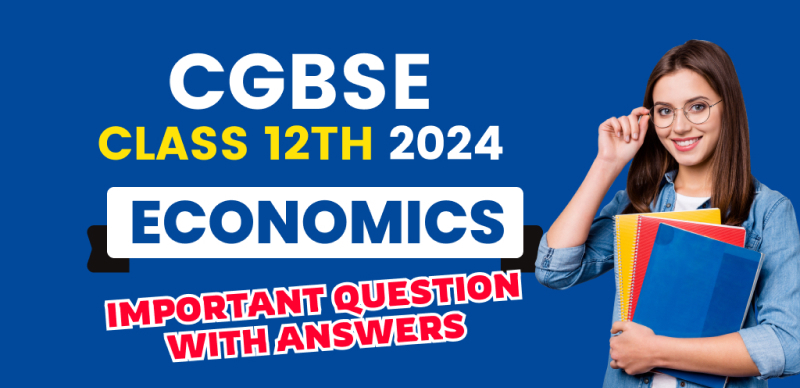
SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की अर्थशास्त्र परीक्षा 21 मार्च, 2024 को निर्धारित है। तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि इस आर्टिकल में आपको बोर्ड परीक्षा के लिए वो ही प्रश्न दिए गए है जो बोर्ड पेपर में आने जा रहे है।
इस पोस्ट में छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th परीक्षा 2024 के लिए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण (CG Board 12th Economics Important Question 2024) प्रश्न दिये गये है जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
CG Board 12th Economics Important Question 2024
छात्रों को इन (CG Board 12 Economics Viral Question 2024) प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। अब आपकी परीक्षा में कुछ ही घंटे बचे है I जिससे अर्थशास्त्र के पेपर की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते है I
CG Board 12th Important Very Short Answers Questions
प्रश्न 1. मांग किसे कहते हैं?
Ans. मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं।
प्रश्न 2. सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं?
Ans. सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी खपत की गई मात्रा के साथ घटती जाती है।
प्रश्न 3. कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है?
Ans. कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है।
प्रश्न 4. मांग के नियम का महत्व लिखिए । (कोई एक )
Ans. मांग का नियम यह बताता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, तो लोग उसकी अधिक मांग करते हैं।
प्रश्न 5. बजट समूह में परिवर्तन किस कारण से हो सकता है ?
Ans. बजट समूह में परिवर्तन कई कारणों से हो सकता है, जिनमें शामिल हैं:
- आय में परिवर्तन:
- कीमतों में परिवर्तन:
- रुचि और पसंद में परिवर्तन:
- सरकारी नीतियां:
प्रश्न 6. मांग की कीमत लोच शून्य कब होती है ?
Ans. मांग की कीमत लोच शून्य तब होती है जब किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन के प्रति असंवेदनशील होता है।
प्रश्न 7. उपयोगिता से क्या अभिप्राय है?
Ans. उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त संतुष्टि या सुख की मात्रा है। यह वस्तु या सेवा की उपयोगिता या मूल्य का मापन है।
प्रश्न 8. भारत में सिक्के कौन जारी करता है?
Ans. भारत में सिक्के भारत सरकार जारी करती है।
प्रश्न 9. मुद्रा पूर्ति के दो घटक बताइए ।
Ans. मुद्रा पूर्ति के दो मुख्य घटक हैं:
- मुद्रा: इसमें नकदी के रूप में जनता के पास मौजूद सिक्के और नोट शामिल हैं।
- जमा: इसमें बैंकों में जमा धनराशि शामिल है।
प्रश्न 10. भारत की वास्तविक मुद्रा कौन सी है ?
Ans. भारत की वास्तविक मुद्रा भारतीय रुपया है।
प्रश्न 11. 'चेक' किस प्रकार की मुद्रा है ?
Ans. चेक मुद्रा नहीं है, यह भुगतान का एक साधन है।
प्रश्न 12. अनुसूचित बैंक से क्या आशय है?
Ans. अनुसूचित बैंक वह बैंक होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होता है। यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करता है।
प्रश्न 13. रिजर्व बैंक के किन्ही दो विभागों के नाम लिखिए ?
Ans. रिजर्व बैंक के दो विभागों के नाम हैं:
- बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (Banking Supervision Department): यह विभाग बैंकों की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन की निगरानी करता है। यह बैंकों के लिए नियम और विनियम भी बनाता है।
- मुद्रा प्रबंधन विभाग (Monetary Management Department): यह विभाग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
प्रश्न 14. बजट में किसका वर्णन किया जाता है ?
Ans. बजट में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वर्णन किया जाता है।
प्रश्न 15. भारत में एक रुपये का नोट कौन जारी करता है ?
Ans. भारत में एक रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
प्रश्न 16. बजट का कोई एक उद्देश्य लिखिए ?
Ans. बजट का एक मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
प्रश्न 17. कर क्यों लगाया जाता है ?
Ans. कर लगाया जाता है सरकार को राजस्व प्रदान करने के लिए।
प्रश्न 18. प्रगतिशील कर को परिभाषित कीजिए ?
Ans. प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जिसमें आय बढ़ने के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अधिक कमाते हैं, वे कम कमाने वालों की तुलना में अधिक कर का भुगतान करते हैं।
प्रश्न 19. प्राथमिक घाटा से क्या अभिप्राय बताइए?
Ans. प्राथमिक घाटा सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर होता है, जिसमें ब्याज भुगतान को छोड़ दिया जाता है।
प्रश्न 20. सरकारी घाटा कम करने के कोई एक उपाय लिखिए ।
Ans. सरकारी घाटा कम करने के कई उपाय हैं, जिनमें से एक सरकारी खर्चों को कम करना है।
प्रश्न 21. संतुलित बजट का कोई एक गुण लिखिए।
Ans. संतुलित बजट का एक गुण यह है कि यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है।
प्रश्न 22. मनोरंजन कर किस कर का उदाहरण है ?
Ans. मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है।
प्रश्न 23. भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है ?
Ans. भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है।
प्रश्न 24. प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए ।
Ans. प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण आयकर है।
प्रश्न 25. राजकोषीय नीति के अन्तर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ?
Ans. राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा सरकारी खर्च और करों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का अध्ययन किया जाता है।
CG Board 12th Important Short Answers Questions
प्रश्न 1. चयन की समस्या क्या है? यह क्यों उत्पन्न होती है?
Ans. चयन की समस्या: परिभाषा और कारण
चयन की समस्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें सीमित संसाधनों के कारण हमें अनेक विकल्पों में से कुछ चुनने होते हैं। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं हमारी क्षमता से अधिक होती हैं।
चयन की समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण:
- सीमित संसाधन: हमारे पास धन, समय, ऊर्जा, और अन्य संसाधनों की सीमित मात्रा होती है।
- अनंत विकल्प: हमारे पास हमेशा कई विकल्प होते हैं, जिनमें से सभी को चुनना संभव नहीं होता है।
- अनिश्चितता: हम हमेशा भविष्य के बारे में निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए यह जानना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा।
प्रश्न 2. अर्थशास्त्र कला और विज्ञान है । कैसे?
Ans. अर्थशास्त्र: कला और विज्ञान का मिश्रण
अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। विज्ञान के रूप में, अर्थशास्त्र अनुभवजन्य डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करता है। यह आर्थिक सिद्धांतों और मॉडलों को विकसित करता है जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। कला के रूप में, अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार और सामाजिक संस्थाओं को समझने पर केंद्रित है। यह तर्क और विश्लेषण का उपयोग करता है ताकि हमें आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सके।
प्रश्न 3. उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं लिखिए। (कोई चार)
Ans. उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं:
-
अवतल आकार: उत्पादन संभावना वक्र (PPC) अवतल होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे-जैसे हम एक वस्तु का अधिक उत्पादन करते हैं, हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है।
-
सीमित संसाधन: यह वक्र सीमित संसाधनों की धारणा पर आधारित है।
-
कुशलता: यह वक्र यह मानता है कि सभी संसाधनों का उपयोग कुशलता से किया जा रहा है।
-
विकल्प लागत: यह वक्र विकल्प लागत की अवधारणा को दर्शाता है।
प्रश्न 4. व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार लिखिए |
Ans. व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार:
व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ताओं, उत्पादकों, और बाजारों का अध्ययन करती है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य प्रकार हैं:
-
उपभोक्ता व्यवहार: यह उपभोक्ताओं द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है।
-
उत्पादन का सिद्धांत: यह उत्पादकों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है।
-
बाजार संरचना: यह विभिन्न प्रकार के बाजारों और उनमें प्रतिस्पर्धा की प्रकृति का अध्ययन करता है।
प्रश्न 5. अर्थव्यवस्था के प्रकार समझाइए ।
Ans. अर्थव्यवस्था के प्रकार:
अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:
1. उत्पादन के साधनों की स्वामित्व:
- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था: उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों और कंपनियों के पास होता है।
- समाजवादी अर्थव्यवस्था: उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य के पास होता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था: यह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है।
2. विकास का स्तर:
- विकसित अर्थव्यवस्था: उच्च आय, उच्च जीवन स्तर और विकसित बुनियादी ढांचे वाली अर्थव्यवस्था।
- विकसितशील अर्थव्यवस्था: निम्न आय, निम्न जीवन स्तर और विकासशील बुनियादी ढांचे वाली अर्थव्यवस्था।
3. राजनीतिक व्यवस्था:
- लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था: लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था।
- अधिनायकवादी अर्थव्यवस्था: अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था।
प्रश्न 6. उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव किन कारणों से होता है?
Ans. उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव के कारण:
उत्पादन संभावना वक्र (PPC) में खिसकाव संसाधनों या तकनीक में बदलाव के कारण होता है।
1. संसाधनों में बदलाव:
- संसाधनों की मात्रा में वृद्धि: PPC दाईं ओर खिसकता है।
- संसाधनों की मात्रा में कमी: PPC बाईं ओर खिसकता है।
- संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार: PPC दाईं ओर खिसकता है।
- संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट: PPC बाईं ओर खिसकता है।
2. तकनीक में बदलाव:
- तकनीकी प्रगति: PPC दाईं ओर खिसकता है।
- तकनीकी गिरावट: PPC बाईं ओर खिसकता है।
प्रश्न 7. व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए ।
Ans. व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं:
1. व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्यान: व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ताओं, उत्पादकों, और बाजारों पर ध्यान केंद्रित करता है।
2. सीमित संसाधन: यह सीमित संसाधनों की धारणा पर आधारित है और यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे व्यक्ति इन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं।
3. विकल्प लागत: यह विकल्प लागत की अवधारणा पर केंद्रित है, जो कि एक वस्तु का चयन करने पर दूसरी वस्तु का त्याग करना होता है।
4. सीमांत विश्लेषण: यह सीमांत विश्लेषण का उपयोग करता है, जो कि एक इकाई में परिवर्तन का प्रभाव का अध्ययन करता है।
प्रश्न 8. अल्पकाल एवं दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाईए ।
Ans. अल्पकाल एवं दीर्घकाल की संकल्पनाएं:
अल्पकाल और दीर्घकाल अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो समय की अवधि को दर्शाती हैं।
अल्पकाल:
- समय: यह एक छोटी अवधि है, आमतौर पर एक वर्ष से कम।
- उत्पादन के साधन: कुछ उत्पादन के साधन स्थिर होते हैं, जैसे कि मशीनरी और भूमि।
- उत्पादन में परिवर्तन: उत्पादन में परिवर्तन केवल परिवर्ती साधनों, जैसे कि श्रम, का उपयोग करके किया जा सकता है।
- उदाहरण: एक कंपनी अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर सकती है।
दीर्घकाल:
- समय: यह एक लंबी अवधि है, आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक।
- उत्पादन के साधन: सभी उत्पादन के साधन परिवर्ती होते हैं।
- उत्पादन में परिवर्तन: उत्पादन में परिवर्तन किसी भी साधन को बदलकर किया जा सकता है।
- उदाहरण: एक कंपनी दीर्घकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मशीनरी खरीद सकती है।
प्रश्न 9. सीमांत लागत और औसत लागत के संबंध को समझाईए।
Ans. सीमांत लागत और औसत लागत का संबंध:
सीमांत लागत (MC) और औसत लागत (AC) अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो उत्पादन की लागत को मापती हैं।
सीमांत लागत:
- यह एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने की अतिरिक्त लागत है।
- यह उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि के कारण कुल लागत में परिवर्तन को दर्शाता है।
औसत लागत:
- यह कुल उत्पादन को उत्पादन की इकाइयों की संख्या से भाग करके प्राप्त किया जाता है।
- यह प्रति इकाई उत्पादन की औसत लागत को दर्शाता है।
सीमांत लागत और औसत लागत का संबंध:
- अल्पकाल में:
- जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, MC AC को काटता है।
- AC U आकार का होता है।
- दीर्घकाल में:
- MC AC के समान होता है।
- AC L आकार का होता है।
प्रश्न 10. पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के मुख्य कारण बताइए ।
Ans. पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के मुख्य कारण:
पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का अर्थ है कि उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि इनपुट में प्रतिशत वृद्धि से अधिक होती है।
इसके मुख्य कारण हैं:
1. विशेषज्ञता: जब उत्पादन बढ़ता है, तो श्रमिक और मशीनें विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञ हो सकते हैं, जिससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होती है।
2. तकनीकी प्रगति: बड़े पैमाने पर उत्पादन नई तकनीकों के उपयोग को अर्थव्यवस्थित बनाता है, जो उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है।
3. मात्रा छूट: बड़े पैमाने पर खरीद मात्रा छूट प्राप्त करने में मदद करती है, जो इनपुट की लागत को कम करती है।
4. सीखने की अवस्था: अनुभव के साथ, श्रमिक अधिक कुशल बनते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।
प्रश्न 11. परिवर्ती उत्पाद का नियम क्या है?
Ans. परिवर्ती उत्पाद का नियम:
परिवर्ती उत्पाद का नियम बताता है कि जब एक इनपुट को स्थिर रखा जाता है और अन्य इनपुट को बढ़ाया जाता है, तो प्रारंभिक में उत्पाद में वृद्धि होगी, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पाद में गिरावट शुरू हो जाएगी।
यह नियम कई कारणों से होता है:
- श्रम का विभाजन: जब एक इनपुट (जैसे श्रम) को बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन, एक बिंदु के बाद, श्रमिकों की संख्या अधिक हो जाती है और वे एक दूसरे के काम में बाधा डालने लगते हैं।
- सीमित पूरक इनपुट: जब एक इनपुट (जैसे श्रम) को बढ़ाया जाता है, तो अन्य इनपुट (जैसे मशीनरी) सीमित हो जाते हैं। इसके कारण, उत्पाद में गिरावट शुरू हो जाती है।
- थकान: जब श्रमिक लंबे समय तक काम करते हैं, तो वे थक जाते हैं और उत्पादन में गिरावट आती है।
प्रश्न 12. पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर स्पष्ट कीजिए ।
Ans. पूर्ति और स्टॉक में अंतर:
पूर्ति और स्टॉक दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं जो कमोडिटी की उपलब्धता को दर्शाती हैं।
पूर्ति:
- यह एक निश्चित समय अवधि में बाजार में उपलब्ध कमोडिटी की मात्रा है।
- यह उत्पादन और आयात से प्रभावित होता है।
- यह बाजार में कमोडिटी की कीमत को निर्धारित करता है।
स्टॉक:
- यह एक निश्चित समय पर बाजार में मौजूद कमोडिटी की मात्रा है।
- यह उत्पादन, आयात, खपत और निर्यात से प्रभावित होता है।
- यह बाजार में कमोडिटी की कीमत को प्रभावित कर सकता है।
प्रश्न 13. पूर्ति की लोच को कौन से घटक प्रभावित करते है?
Ans. पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटक:
पूर्ति की लोच यह दर्शाता है कि कमोडिटी की कीमत में परिवर्तन के प्रति उत्पादक कितना उत्तरदायी हैं।
इसे प्रभावित करने वाले मुख्य घटक हैं:
1. उत्पादन की तकनीक:
- यदि उत्पादन की तकनीक स्थिर है, तो पूर्ति कम लोचदार होगी।
- यदि उत्पादन की तकनीक लचीली है, तो पूर्ति अधिक लोचदार होगी।
2. इनपुट की कीमतें:
- यदि इनपुट की कीमतें स्थिर हैं, तो पूर्ति कम लोचदार होगी।
- यदि इनपुट की कीमतें अस्थिर हैं, तो पूर्ति अधिक लोचदार होगी।
3. प्रतिस्पर्धा का स्तर:
- यदि बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा है, तो पूर्ति अधिक लोचदार होगी।
- यदि बाजार में कम प्रतिस्पर्धा है, तो पूर्ति कम लोचदार होगी।
प्रश्न 14. तकनीकी सुधार होने पर बाजार पूर्ति कैसे प्रभावित होती है ?
Ans. तकनीकी सुधार होने पर बाजार पूर्ति कैसे प्रभावित होती है:
जब तकनीकी सुधार होता है, तो उत्पादन की लागत कम हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे बाजार पूर्ति में वृद्धि होती है। तकनीकी सुधार बाजार पूर्ति को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित कर सकता है:
1. उत्पादन क्षमता में वृद्धि:
- नई तकनीकें उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकती हैं, जिससे अधिक उत्पादन हो सकता है।
- उदाहरण: स्वचालन तकनीक उत्पादन प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बना सकती है।
2. उत्पादन की लागत में कमी:
- नई तकनीकें उत्पादन की लागत को कम कर सकती हैं, जिससे उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
- उदाहरण: नए उर्वरक कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और लागत को कम कर सकते हैं।
3. नए उत्पादों का विकास:
- नई तकनीकें नए उत्पादों के विकास को जन्म दे सकती हैं, जिससे बाजार पूर्ति में वृद्धि होती है।
- उदाहरण: नई दवाएं और चिकित्सा उपकरण स्वास्थ्य सेवा उद्योग में नई पूर्ति बनाते हैं।
प्रश्न 15. उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने के कारण लिखिए। (कोई चार)
Ans. उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने के चार कारण:
1. उत्पादन के साधनों की पूरकता:
- विभिन्न उत्पादन के साधनों का उपयोग एक दूसरे के साथ पूरक रूप से किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
- उदाहरण: यदि एक किसान अधिक भूमि का उपयोग करता है, तो उसे अधिक उर्वरक और बीज की आवश्यकता होगी।
2. श्रम विभाजन:
- जब श्रमिकों को विशिष्ट कार्यों में विभाजित किया जाता है, तो वे अधिक कुशल बन जाते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
- उदाहरण: एक कारखाने में, विभिन्न श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करते हैं।
3. विशेषज्ञता:
- जब श्रमिक और मशीनें विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो वे अधिक कुशल बन जाते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
- उदाहरण: एक डॉक्टर जो केवल हृदय रोगों का इलाज करता है, वह सामान्य चिकित्सक की तुलना में अधिक कुशल होगा।
4. तकनीकी प्रगति:
- नई तकनीकों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया को अधिक कुशल बना सकता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
- उदाहरण: स्वचालन तकनीक का उपयोग करके, कंपनियां कम श्रमिकों के साथ अधिक उत्पादन कर सकती हैं।
प्रश्न 16. पूर्ति का नियम लागू होने के कारण लिखिए।
Ans. पूर्ति का नियम लागू होने के चार कारण:
1. उत्पादन की लागत:
- जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।
- उदाहरण: यदि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ती है, तो उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी।
2. सरकारी नीतियां:
- सरकारें कभी-कभी उत्पादन पर कर लगाती हैं, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।
- उदाहरण: यदि सरकार आयातित कच्चे माल पर कर लगाती है, तो उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी।
3. प्राकृतिक आपदाएं:
- प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ या सूखा, उत्पादन को कम कर सकती हैं, जिससे पूर्ति कम हो सकती है।
- उदाहरण: यदि एक बाढ़ फसलों को नष्ट कर देती है, तो खाद्य उत्पादन कम हो जाएगा।
4. तकनीकी परिवर्तन:
- नई तकनीकों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया को अधिक कुशल बना सकता है, जिससे उत्पादन की लागत कम हो सकती है।
- उदाहरण: स्वचालन तकनीक का उपयोग करके, कंपनियां कम श्रमिकों के साथ अधिक उत्पादन कर सकती हैं।
प्रश्न 17. कुल स्थिर लागत और औसत स्थिर लागत को स्पष्ट कीजिए ।
Ans. कुल स्थिर लागत और औसत स्थिर लागत:
कुल स्थिर लागत (Total Fixed Cost - TFC):
- यह उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के बावजूद स्थिर रहती है।
- उदाहरण: किराया, वेतन, बीमा, आदि।
औसत स्थिर लागत (Average Fixed Cost - AFC):
- यह कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग कर प्राप्त किया जाता है।
- AFC = TFC / Q
- जहां Q उत्पादन की मात्रा है।
प्रश्न 18. समरूप वस्तुएँ किस बाजार की मुख्य विशेषता है ?
Ans. समरूप वस्तुएँ किस बाजार की मुख्य विशेषता है?
पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में समरूप वस्तुएँ मुख्य विशेषता हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं:
- बहुत सारे खरीदार और विक्रेता होते हैं।
- प्रत्येक खरीदार और विक्रेता कीमत लेने वाला होता है।
- वस्तुएँ समरूप होती हैं।
- बाजार में पूर्ण जानकारी होती है।
प्रश्न 19. माँग के कम होने का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता हैं ?
Ans. माँग के कम होने का कीमत पर प्रभाव:
माँग और कीमत एक दूसरे से व्यस्त संबंध रखते हैं। जब माँग कम होती है, तो कीमत भी कम हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं।
1. उपभोक्ताओं की आय में कमी:
- जब उपभोक्ताओं की आय कम होती है, तो वे कम खर्च करते हैं। इससे माँग कम हो जाती है और कीमत भी कम हो जाती है।
2. वस्तुओं के विकल्पों की उपलब्धता:
- जब किसी वस्तु के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो उपभोक्ता एक वस्तु की माँग कम कर सकते हैं। इससे कीमत भी कम हो जाती है।
3. सरकार की नीतियां:
- सरकार की नीतियां भी माँग और कीमत को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, सरकार किसी वस्तु पर कर बढ़ा सकती है, जिससे उसकी माँग कम हो जाएगी और कीमत भी कम हो जाएगी।
प्रश्न 20. अल्पाधिकार की 3 विशेषताएँ लिखिए ।
Ans. अल्पाधिकार की 3 विशेषताएँ:
- कम संख्या में विक्रेता: अल्पाधिकार बाजार में वस्तु या सेवा के कुछ ही विक्रेता होते हैं। ये विक्रेता बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं और कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
- अंतर्निर्भरता: अल्पाधिकार बाजार में, एक विक्रेता द्वारा किए गए निर्णयों का अन्य विक्रेताओं पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए, विक्रेताओं को एक दूसरे की रणनीतियों पर ध्यान देना होगा।
- प्रवेश में बाधाएं: अल्पाधिकार बाजार में प्रवेश करना मुश्किल होता है। उच्च प्रारंभिक लागत, पेटेंट, और सरकारी नियमों जैसी बाधाएं नए विक्रेताओं को बाजार में प्रवेश करने से रोक सकती हैं।
प्रश्न 21. चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार का होता है स्पष्ट कीजिए ।
Ans. चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होता है:
- वास्तविक चक्रीय प्रवाह: यह वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक प्रवाह है जो घरों और फर्मों के बीच होता है। इसमें उत्पादन, वितरण, और खपत शामिल हैं।
- आय चक्रीय प्रवाह: यह आय का प्रवाह है जो घरों और फर्मों के बीच होता है। इसमें वेतन, किराया, लाभ, और कर शामिल हैं।
दोनों प्रकार के चक्रीय प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं:
- घरों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत से फर्मों को आय प्राप्त होती है।
- फर्मों द्वारा घरों को वेतन, किराया, और लाभ का भुगतान किया जाता है।
- घरों द्वारा प्राप्त आय का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है।
प्रश्न 22. चक्रीय प्रवाह में अन्तः क्षेपण एवं क्षरण को परिभाषित कीजिए ।
Ans. चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण एवं क्षरण:
अंतःक्षेपण:
- यह चक्रीय प्रवाह में सरकार द्वारा किया गया हस्तक्षेप है।
- सरकार विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है, जैसे कि:
- राजकोषीय नीति: सरकार द्वारा करों और खर्चों में बदलाव।
- आय नीति: सरकार द्वारा वेतन और मूल्य नियंत्रण।
- नियामक नीति: सरकार द्वारा बाजारों के नियमन।
क्षरण:
- यह चक्रीय प्रवाह में आय के रिसाव को संदर्भित करता है।
- आय का रिसाव तब होता है जब आय का एक हिस्सा अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जाता है।
- आय का रिसाव निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है:
- बचत: जब लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाते हैं।
- कर: जब सरकार करों के रूप में आय का कुछ हिस्सा लेती है।
- आयात: जब लोग विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं।
प्रश्न 23. राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व लिखिए ।
Ans. राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व:
1. आर्थिक प्रगति का मापन:
- राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक प्रगति का मापन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
- राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।
2. विभिन्न देशों की तुलना:
- राष्ट्रीय आय का उपयोग विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए किया जा सकता है।
- यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सा देश अधिक समृद्ध है और कौन सा देश कम समृद्ध है।
3. नीति निर्माण:
- राष्ट्रीय आय का उपयोग सरकारों द्वारा नीति निर्माण के लिए किया जाता है।
- सरकारें राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करती हैं कि किन क्षेत्रों में निवेश करना है और किन नीतियों को लागू करना है।
प्रश्न 24. भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु 5 सुझाव दीजिए ।
Ans. भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु 5 सुझाव:
- कृषि क्षेत्र में सुधार:
- कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, और किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।
- उद्योगों का विकास:
- लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर, विदेशी निवेश को आकर्षित करके, और बुनियादी ढांचे में सुधार करके उद्योगों का विकास किया जा सकता है।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि:
- शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके, उद्यमिता को बढ़ावा देकर, और सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है।
- मानव पूँजी का विकास:
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करके, लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके मानव पूँजी का विकास किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे में सुधार:
- सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, और बिजली जैसी बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में सुधार करके देश में व्यापार और व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
प्रश्न 25. एक देश में विनियोग की मात्रा किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ?
Ans. एक देश में विनियोग की मात्रा निर्धारित करने वाले कारक:
- उत्पादन क्षमता:
- एक देश की उत्पादन क्षमता उसकी विनियोग क्षमता को निर्धारित करती है।
- यदि उत्पादन क्षमता अधिक है, तो देश अधिक विनियोग कर सकता है।
- बचत:
- एक देश में बचत की मात्रा विनियोग की मात्रा को निर्धारित करती है।
- यदि बचत अधिक है, तो देश अधिक विनियोग कर सकता है।
- उधार लेने की क्षमता:
- एक देश अपनी उधार लेने की क्षमता के आधार पर विनियोग कर सकता है।
- यदि देश की उधार लेने की क्षमता अधिक है, तो वह अधिक विनियोग कर सकता है।
- ब्याज दर:
- ब्याज दर विनियोग की मात्रा को प्रभावित करती है।
- यदि ब्याज दर कम है, तो विनियोग अधिक होगा।
CG Board 12th Important Long Answers Type Questions
प्रश्न 1. मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले छः कारको का वर्णन कीजिए ।
Ans. मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले छः कारक:
1. वस्तु का प्रकार:
- कुछ वस्तुएं, जैसे कि जीवन रक्षक दवाएं, अत्यंत आवश्यक होती हैं और इनकी मांग कीमत के प्रति कम लोचदार होती है।
- अन्य वस्तुएं, जैसे कि लक्जरी वस्तुएं, कम आवश्यक होती हैं और इनकी मांग कीमत के प्रति अधिक लोचदार होती है।
2. उपलब्ध विकल्प:
- यदि किसी वस्तु के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, तो उसकी मांग कीमत के प्रति अधिक लोचदार होगी।
- यदि किसी वस्तु के लिए कम विकल्प उपलब्ध हैं, तो उसकी मांग कीमत के प्रति कम लोचदार होगी।
3. उपभोक्ता की आय:
- यदि उपभोक्ता की आय कम है, तो वह कम कीमत वाली वस्तुओं को खरीदेगा और उसकी मांग कीमत के प्रति अधिक लोचदार होगी।
- यदि उपभोक्ता की आय अधिक है, तो वह उच्च कीमत वाली वस्तुओं को खरीदेगा और उसकी मांग कीमत के प्रति कम लोचदार होगी।
4. समय अवधि:
- अल्पकाल में, मांग कीमत के प्रति कम लोचदार होती है।
- दीर्घकाल में, मांग कीमत के प्रति अधिक लोचदार होती है।
5. भविष्य की अपेक्षाएं:
- यदि उपभोक्ताओं को लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी, तो वे वर्तमान में अधिक वस्तुएं खरीदेंगे और मांग कीमत के प्रति कम लोचदार होगी।
- यदि उपभोक्ताओं को लगता है कि भविष्य में कीमतें घटेंगी, तो वे वर्तमान में कम वस्तुएं खरीदेंगे और मांग कीमत के प्रति अधिक लोचदार होगी।
6. सरकारी नीतियां:
- सरकार द्वारा लगाए गए कर और सब्सिडी मांग कीमत लोच को प्रभावित करते हैं।
- कर मांग को कम करते हैं और मांग कीमत लोच को कम करते हैं।
- सब्सिडी मांग को बढ़ाते हैं और मांग कीमत लोच को बढ़ाते हैं।
प्रश्न 2. व्यक्तिगत तथा बाजार मांग तालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए ।
Ans. व्यक्तिगत तथा बाजार मांग तालिका में अंतर:
व्यक्तिगत मांग तालिका:
- यह एक तालिका है जो एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को दर्शाती है।
- यह तालिका यह दर्शाती है कि जैसे-जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा घटती जाती है।
- यह तालिका एक उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है।
बाजार मांग तालिका:
- यह एक तालिका है जो सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की कुल मात्रा को दर्शाती है।
- यह तालिका यह दर्शाती है कि जैसे-जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की कुल मात्रा घटती जाती है।
- यह तालिका सभी उपभोक्ताओं के लिए बनाई जाती है।
प्रश्न 3. मांग के नियम के लागू होने के कारणों को लिखिए ।
Ans. मांग के नियम के लागू होने के कारण:
1. प्रतिस्थापन प्रभाव:
- जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता उस वस्तु को कम खरीदना शुरू कर देते हैं और उसके स्थान पर अन्य वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देते हैं।
- यह प्रतिस्थापन प्रभाव मांग के नियम को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारण है।
2. आय प्रभाव:
- जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है।
- कम आय वाले उपभोक्ता कम वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे मांग कम हो जाती है।
- यह आय प्रभाव मांग के नियम को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारण है।
3. उपभोक्ता की संतुष्टि:
- जैसे-जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपभोग करते हैं, उनकी संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है।
- एक निश्चित स्तर के बाद, संतुष्टि का स्तर कम होने लगता है।
- यह उपभोक्ता को कम वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करता है, जिससे मांग कम हो जाती है।
- यह उपभोक्ता की संतुष्टि मांग के नियम को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारण है।
4. अन्य कारक:
- मांग के नियम को लागू करने के अन्य कारक भी हैं, जैसे कि उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, फैशन, और सरकारी नीतियां।
प्रश्न 4. मांग की कीमत लोच की श्रेणियां लिखिए ।
Ans. मांग की कीमत लोच की श्रेणियां:
मांग की कीमत लोच को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि वस्तु की मांग में परिवर्तन और उसकी कीमत में परिवर्तन के बीच संबंध को दर्शाती हैं।
1. पूर्णतः लोचदार मांग:
- जब वस्तु की कीमत में थोड़ा भी बदलाव उसकी मांग में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, तो मांग को पूर्णतः लोचदार माना जाता है।
- उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को नहीं खरीदेगा।
2. पूर्णतः बेलोचदार मांग:
- जब वस्तु की कीमत में कितना भी बदलाव उसकी मांग में कोई बदलाव नहीं लाता है, तो मांग को पूर्णतः बेलोचदार माना जाता है।
- उदाहरण के लिए, जीवन रक्षक दवाओं की मांग, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, लोग उन्हें खरीदेंगे।
3. अपेक्षाकृत लोचदार मांग:
- जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी मांग में अपेक्षाकृत बड़ा बदलाव लाता है, तो मांग को अपेक्षाकृत लोचदार माना जाता है।
- उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाती है, तो लोग उसकी मांग कम कर देंगे।
4. अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग:
- जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी मांग में अपेक्षाकृत कम बदलाव लाता है, तो मांग को अपेक्षाकृत बेलोचदार माना जाता है।
- उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाती है, तो लोग उसकी मांग में बहुत कम बदलाव करेंगे।
5. एकात्मक लोचदार मांग:
- जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन और उसकी मांग में परिवर्तन का प्रतिशत समान होता है, तो मांग को एकात्मक लोचदार माना जाता है।
- इसका मतलब है कि यदि वस्तु की कीमत 10% बढ़ती है, तो उसकी मांग भी 10% कम हो जाएगी।
प्रश्न 5. मांग की लोच का महत्व लिखिए । (कोई 6 )
Ans. मांग की लोच का महत्व:
मांग की लोच एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है जो व्यवसायों और सरकारों को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में मदद करती है। यह दर्शाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी मांग को कैसे प्रभावित करता है। मांग की लोच का महत्व निम्नलिखित 6 बिंदुओं में दर्शाया गया है:
1. मूल्य निर्धारण:
- व्यवसायों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयुक्त मूल्य निर्धारित करने में मदद करता है।
- उच्च मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, व्यवसाय कम मूल्य निर्धारित करके अधिक बिक्री प्राप्त कर सकते हैं।
- कम मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, व्यवसाय उच्च मूल्य निर्धारित करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2. उत्पादन योजना:
- व्यवसायों को अपनी उत्पादन योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- उच्च मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, व्यवसायों को उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता हो सकती है।
- कम मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, व्यवसायों को उत्पादन में कमी करने की आवश्यकता हो सकती है।
3. विपणन रणनीति:
- व्यवसायों को अपनी विपणन रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- उच्च मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, व्यवसायों को विज्ञापन और प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- कम मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, व्यवसायों को उत्पाद भेदभाव और ब्रांडिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है।
4. सरकारी नीतियां:
- सरकारों को विभिन्न नीतियां बनाने में मदद करता है, जैसे कि कर और सब्सिडी।
- उच्च मांग लोच वाली वस्तुओं पर कर लगाने से सरकार को राजस्व प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
- कम मांग लोच वाली वस्तुओं पर सब्सिडी देने से सरकार को उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
5. उपभोक्ता व्यवहार:
- उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच बेहतर चुनाव करने में मदद करता है।
- उच्च मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, उपभोक्ता कीमत में थोड़े बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- कम मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, उपभोक्ता कीमत में थोड़े बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं।
6. बाजार विश्लेषण:
- बाजार में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करने में मदद करता है।
- उच्च मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा होती है।
- कम मांग लोच वाली वस्तुओं के लिए, बाजार में कम प्रतिस्पर्धा होती है।
प्रश्न 6. पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे निर्धारित होता है ?
Ans. पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण:
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, मूल्य मांग और आपूर्ति के बलों द्वारा निर्धारित होता है।
1. मांग:
- मांग, किसी वस्तु की एक निश्चित मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा खरीदने की इच्छा और क्षमता को दर्शाती है।
- पूर्ण प्रतियोगिता में, बाजार में अनेक खरीदार होते हैं, और प्रत्येक खरीदार एक समान वस्तु खरीदता है।
- बाजार में सभी खरीदारों की कुल मांग को बाजार मांग कहा जाता है।
2. आपूर्ति:
- आपूर्ति, किसी वस्तु की एक निश्चित मूल्य पर उत्पादक द्वारा बेचने की इच्छा और क्षमता को दर्शाती है।
- पूर्ण प्रतियोगिता में, बाजार में अनेक उत्पादक होते हैं, और प्रत्येक उत्पादक एक समान वस्तु का उत्पादन करता है।
- बाजार में सभी उत्पादकों की कुल आपूर्ति को बाजार आपूर्ति कहा जाता है।
3. मूल्य निर्धारण:
- पूर्ण प्रतियोगिता में, मांग वक्र और आपूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर मूल्य निर्धारित होता है।
- यह प्रतिच्छेदन बिंदु संतुलन बिंदु कहलाता है।
- संतुलन बिंदु पर, बाजार में मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा, बाजार में आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की मात्रा के बराबर होती है।
4. मूल्य परिवर्तन:
- यदि मांग में वृद्धि होती है, तो मांग वक्र ऊपर की ओर खिसकता है, और मूल्य बढ़ जाता है।
- यदि आपूर्ति में वृद्धि होती है, तो आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर खिसकता है, और मूल्य घट जाता है।
- यदि मांग में कमी होती है, तो मांग वक्र नीचे की ओर खिसकता है, और मूल्य घट जाता है।
- यदि आपूर्ति में कमी होती है, तो आपूर्ति वक्र नीचे की ओर खिसकता है, और मूल्य बढ़ जाता है।
5. सरकार की भूमिका:
- पूर्ण प्रतियोगिता में, सरकार बाजार में हस्तक्षेप नहीं करती है।
- मूल्य पूरी तरह से मांग और आपूर्ति के बलों द्वारा निर्धारित होता है।
प्रश्न 7. अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए ।
Ans. अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताएं:
1. विक्रेताओं की कम संख्या:
- अल्पाधिकार बाजार में, कुछ ही विक्रेता होते हैं जो एक समान या विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं।
- इन विक्रेताओं का बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।
2. उच्च प्रवेश बाधाएं:
- अल्पाधिकार बाजार में प्रवेश करना मुश्किल होता है।
- उच्च प्रारंभिक लागत, पेटेंट, और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध प्रवेश बाधाओं के कुछ उदाहरण हैं।
3. मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता:
- अल्पाधिकार बाजार में, विक्रेताओं को मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता होती है।
- वे मांग और आपूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हैं।
4. परस्पर निर्भरता:
- अल्पाधिकार बाजार में, प्रत्येक विक्रेता अन्य विक्रेताओं के निर्णयों से प्रभावित होता है।
- एक विक्रेता द्वारा मूल्य में बदलाव अन्य विक्रेताओं को भी अपनी कीमतों में बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकता है।
5. गैर-मूल्य प्रतिस्पर्धा:
- अल्पाधिकार बाजार में, विक्रेता मूल्य के अलावा अन्य तरीकों से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- वे विज्ञापन, ब्रांडिंग, और उत्पाद भेदभाव का उपयोग करके उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं।
6. मुनाफाखोरी:
- अल्पाधिकार बाजार में, विक्रेता प्रतिस्पर्धी बाजार की तुलना में अधिक मुनाफा कमाते हैं।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता रखते हैं और बाजार में उनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।
प्रश्न 8. किसी वस्तु के विस्तृत बाजार के लिए देश की आंतरिक दशाएँ कैसे प्रभावित करती है ? 5 बिन्दुओं में वर्णन कीजिए ।
Ans. किसी वस्तु के विस्तृत बाजार के लिए देश की आंतरिक दशाएँ कैसे प्रभावित करती है? (5 बिन्दु)
1. राजनीतिक स्थिरता:
- राजनीतिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।
- अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियां, निवेशकों को डरा सकती हैं और व्यापार को बाधित कर सकती हैं।
- इससे वस्तुओं की मांग और आपूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
2. आर्थिक विकास:
- एक मजबूत अर्थव्यवस्था, वस्तुओं की मांग को बढ़ावा देती है।
- जब लोगों के पास अधिक पैसा होता है, तो वे अधिक वस्तुएं खरीदते हैं।
- इससे वस्तुओं के बाजार का विस्तार होता है।
3. बुनियादी ढांचा:
- एक अच्छा बुनियादी ढांचा, वस्तुओं के उत्पादन और परिवहन को आसान बनाता है।
- इससे वस्तुओं की लागत कम होती है और उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है।
- इससे वस्तुओं के बाजार का विस्तार होता है।
4. जनसंख्या:
- एक बड़ी और बढ़ती जनसंख्या, वस्तुओं की मांग को बढ़ाती है।
- इससे वस्तुओं के बाजार का विस्तार होता है।
5. सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:
- लोगों की जीवनशैली और प्राथमिकताएं, वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती हैं।
- बदलती जीवनशैली और प्राथमिकताओं से, नए बाजारों का निर्माण हो सकता है।
प्रश्न 9. एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? वर्णन कीजिए ।
Ans. एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण:
एकाधिकार बाजार में, केवल एक ही विक्रेता होता है जो किसी वस्तु का उत्पादन और बिक्री करता है। इस वजह से, विक्रेता को मूल्य निर्धारण में काफी स्वतंत्रता होती है।
मूल्य निर्धारण के लिए एकाधिकारी निम्नलिखित बातों पर विचार करता है:
1. मांग:
- एकाधिकारी वस्तु की मांग का विश्लेषण करता है।
- वह यह जानने की कोशिश करता है कि विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता कितनी वस्तु खरीदेंगे।
2. सीमांत लागत:
- एकाधिकारी वस्तु का उत्पादन करने की सीमांत लागत का विश्लेषण करता है।
- सीमांत लागत, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की लागत होती है।
3. सीमांत राजस्व:
- एकाधिकारी वस्तु की बिक्री से प्राप्त सीमांत राजस्व का विश्लेषण करता है।
- सीमांत राजस्व, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व होता है।
4. लाभ:
- एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य निर्धारित करता है।
- वह उस मूल्य पर वस्तु का उत्पादन और बिक्री करता है जहाँ सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर होता है।
5. सरकारी नीतियां:
- सरकार, एकाधिकार बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना सकती है।
- सरकार, मूल्य नियंत्रण भी लगा सकती है।
प्रश्न 10. एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होती हैं क्यों?
Ans. एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होती हैं क्यों?
एकाधिकार बाजार में, केवल एक ही फर्म होती है जो किसी वस्तु का उत्पादन और बिक्री करती है। इस वजह से, फर्म को मूल्य निर्धारण में काफी स्वतंत्रता होती है।
एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होने के मुख्य कारण:
1. एकमात्र विक्रेता:
- एकाधिकार बाजार में, केवल एक ही फर्म होती है जो किसी वस्तु का उत्पादन और बिक्री करती है।
- इस वजह से, फर्म बाजार में एकाधिकार का दर्जा प्राप्त करती है।
2. प्रतिस्पर्धा का अभाव:
- एकाधिकार बाजार में, फर्म को किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है।
- इस वजह से, फर्म अपनी इच्छानुसार मूल्य निर्धारित कर सकती है।
3. मांग वक्र का ढलान:
- एकाधिकार बाजार में, वस्तु की मांग वक्र नकारात्मक ढलान वाला होता है।
- इसका मतलब है कि मूल्य में वृद्धि के साथ, वस्तु की मांग में कमी आती है।
4. सीमांत राजस्व और सीमांत लागत:
- एकाधिकार बाजार में, फर्म उस मूल्य पर वस्तु का उत्पादन और बिक्री करती है जहाँ सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर होता है।
- इस मूल्य पर, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।
5. सरकारी नीतियां:
- सरकार, एकाधिकार बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना सकती है।
- सरकार, मूल्य नियंत्रण भी लगा सकती है।
प्रश्न 11. समग्र मांग किसे कहते हैं ? इसके प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए ।
Ans. समग्र मांग किसे कहते हैं ?
समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को दर्शाता है। यह एक निश्चित मूल्य स्तर पर, उपभोक्ताओं, व्यवसायों, सरकार और विदेशी क्षेत्रों द्वारा मांगी गई वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है।
समग्र मांग के प्रमुख घटक:
1. उपभोग (C):
- यह अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग को दर्शाता है।
- उपभोग, समग्र मांग का सबसे बड़ा घटक है।
- उपभोग, आय, ब्याज दर, कीमतों और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं से प्रभावित होता है।
2. निवेश (I):
- यह अर्थव्यवस्था में व्यवसायों द्वारा किए गए निवेश को दर्शाता है।
- निवेश, भविष्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- निवेश, ब्याज दर, भविष्य की आर्थिक गतिविधियों की उम्मीदों और सरकार की नीतियों से प्रभावित होता है।
3. सरकारी खर्च (G):
- यह अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा किए गए खर्च को दर्शाता है।
- सरकारी खर्च, वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाता है।
- सरकारी खर्च, सरकार की नीतियों, राजकोषीय स्थिति और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है।
4. शुद्ध निर्यात (NX):
- यह देश द्वारा निर्यात किए गए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और आयात किए गए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बीच का अंतर है।
- शुद्ध निर्यात, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, घरेलू और विदेशी कीमतों और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित होता है।
प्रश्न 12. पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज दर से क्या अभिप्राय है ?
Ans. पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज दर:
पूंजी की सीमांत कुशलता (MEC):
- यह किसी निश्चित समय अवधि में पूंजी के एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय को दर्शाता है।
- यह पूंजी के उपयोग की दक्षता को मापता है।
- MEC, समय के साथ घटता जाता है क्योंकि पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है।
ब्याज दर (r):
- यह पूंजी उधार लेने की लागत को दर्शाता है।
- यह ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता से ऋण पर लगाया जाने वाला शुल्क है।
- ब्याज दर, मुद्रास्फीति, जोखिम, और बाजार की स्थितियों से प्रभावित होती है।
संबंध:
- MEC और ब्याज दर एक दूसरे से नकारात्मक रूप से संबंधित होते हैं।
- जब MEC ब्याज दर से अधिक होता है, तो निवेश करना फायदेमंद होता है।
- जब MEC ब्याज दर से कम होता है, तो निवेश करना लाभदायक नहीं होता है।
- संतुलन:
- MEC और ब्याज दर बराबर होने पर निवेश का स्तर संतुलन में होता है।
महत्व:
- MEC और ब्याज दर, अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- MEC और ब्याज दर में बदलाव, अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित कर सकता है।
प्रश्न 13. अभावी मांग को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। (कोई 6)
Ans. अभावी मांग को दूर करने के उपाय:
1. सरकारी खर्च में वृद्धि:
- सरकार, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि कर सकती है।
- सरकार, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में निवेश कर सकती है।
2. करों में कमी:
- सरकार, करों में कमी करके उपभोक्ताओं और व्यवसायों के पास उपलब्ध आय को बढ़ा सकती है।
- इससे उपभोग और निवेश में वृद्धि होगी।
3. ब्याज दरों में कमी:
- सरकार, ब्याज दरों में कमी करके ऋण लेने की लागत को कम कर सकती है।
- इससे निवेश और उपभोग में वृद्धि होगी।
4. मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि:
- सरकार, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ा सकती है।
- इससे उपभोग और निवेश में वृद्धि होगी।
5. आय वितरण में सुधार:
- सरकार, आय वितरण में सुधार करके गरीबों की क्रय शक्ति को बढ़ा सकती है।
- इससे उपभोग में वृद्धि होगी।
6. आर्थिक सुधार:
- सरकार, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए आर्थिक सुधार कर सकती है।
- इससे निवेश और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
प्रश्न 14. समग्र माँग तथा समग्र पूर्ति की सहायता से आय तथा रोजगार के संतुलन स्तर के निर्धारण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए ।
Ans. समग्र माँग तथा समग्र पूर्ति की सहायता से आय तथा रोजगार के संतुलन स्तर के निर्धारण का सिद्धांत:
समग्र माँग (AD):
- यह अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को दर्शाता है।
- यह उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात का योग होता है।
समग्र पूर्ति (AS):
- यह अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति को दर्शाता है।
- यह उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कीमतों के स्तर को दर्शाता है।
संतुलन स्तर:
- वह स्तर जहाँ समग्र माँग और समग्र पूर्ति बराबर होती है।
- इस स्तर पर, अर्थव्यवस्था में कोई भी मुद्रास्फीति या अपस्फीति नहीं होती है।
सिद्धांत:
- समग्र माँग और समग्र पूर्ति वक्रों का उपयोग करके आय और रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण किया जाता है।
- जब समग्र माँग समग्र पूर्ति से अधिक होती है, तो मुद्रास्फीति होती है।
- जब समग्र माँग समग्र पूर्ति से कम होती है, तो अपस्फीति होती है।
- अर्थव्यवस्था संतुलन स्तर पर तब तक पहुंचती है जब तक कि समग्र माँग और समग्र पूर्ति बराबर नहीं हो जाती।
प्रश्न 15. समझाइए की मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय व्यवस्था की समस्याओं को हल करती है?
Ans. मुद्रा कैसे वस्तु विनिमय व्यवस्था की समस्याओं को हल करती है:
वस्तु विनिमय व्यवस्था की समस्याएं:
- दोहरा संयोग: वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए, दोनों पक्षों की इच्छाएं समान होनी चाहिए।
- मापन की कमी: वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना मुश्किल है।
- विभाज्यता की कमी: कुछ वस्तुओं को छोटे भागों में विभाजित करना मुश्किल है।
- मूल्य का भंडारण: वस्तुओं का मूल्य समय के साथ बदल सकता है।
- परिवहन की लागत: वस्तुओं का परिवहन करना महंगा हो सकता है।
मुद्रा कैसे इन समस्याओं को हल करती है:
- माध्यम of exchange: मुद्रा वस्तुओं के आदान-प्रदान को आसान बनाती है।
- मूल्य का मानक: मुद्रा वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने का एक मानक प्रदान करती है।
- विभाज्यता: मुद्रा को छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है।
- मूल्य का भंडारण: मुद्रा का मूल्य समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहता है।
- परिवहन की आसानी: मुद्रा को आसानी से परिवहन किया जा सकता है।
मुद्रा के लाभ:
- व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है: मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान को आसान बनाती है, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है: मुद्रा निवेश और बचत को प्रोत्साहित करती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- मूल्य स्थिरता: मुद्रा मूल्य स्थिरता प्रदान करती है, जो मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करती है।
प्रश्न 16. एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की क्या विशेषताएँ है ? वर्णन कीजिए ।
Ans. पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं:
1. बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता:
- बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं।
- कोई भी खरीदार या विक्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है।
2. समान उत्पाद:
- सभी विक्रेता एक समान उत्पाद बेचते हैं।
- उत्पादों में कोई भेदभाव नहीं होता है।
3. पूर्ण जानकारी:
- सभी खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार में सभी जानकारी उपलब्ध होती है।
- कोई भी जानकारी छिपी नहीं होती है।
4. मुक्त प्रवेश और निकास:
- कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश या निकास कर सकती है।
- प्रवेश और निकास पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है।
5. मूल्य निर्धारक:
- बाजार में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक होती है।
- कोई भी फर्म मूल्य निर्धारक नहीं होती है।
6. बाजार मूल्य:
- बाजार में मूल्य मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है।
- फर्मों को बाजार मूल्य स्वीकार करना होता है।
7. लाभ का अधिकतमकरण:
- फर्म उत्पादन का स्तर उस स्तर पर निर्धारित करती हैं जहाँ सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर होता है।
- इस स्तर पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।
प्रश्न 17. बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले किन्ही 5 तत्त्वो का उल्लेख कीजिए ।
Ans. बाजार विस्तार को प्रभावित करने वाले 5 तत्व:
1. उत्पाद:
- उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य, और डिजाइन बाजार विस्तार को प्रभावित करते हैं।
- उच्च गुणवत्ता वाले, उचित मूल्य वाले और आकर्षक डिजाइन वाले उत्पादों की मांग अधिक होती है।
2. विपणन:
- प्रभावी विपणन रणनीतियां बाजार विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- विज्ञापन, प्रचार, और बिक्री रणनीतियां बाजार में उत्पाद की जागरूकता बढ़ाने और ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करती हैं।
3. वितरण:
- उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक कुशल वितरण प्रणाली आवश्यक है।
- वितरण चैनलों की उपलब्धता और पहुंच बाजार विस्तार को प्रभावित करती है।
4. प्रतिस्पर्धा:
- प्रतिस्पर्धी बाजार में, फर्मों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी रणनीतियों में लगातार सुधार करना होता है।
- प्रतिस्पर्धा से नवाचार और उत्पाद विकास को बढ़ावा मिलता है।
5. सरकारी नीतियां:
- सरकारी नीतियां, जैसे कि कर नीतियां, व्यापार नीतियां, और विदेशी निवेश नीतियां बाजार विस्तार को प्रभावित करती हैं।
- अनुकूल सरकारी नीतियां बाजार विस्तार को प्रोत्साहित करती हैं।
प्रश्न 18. संतुलन मूल्य किसे कहते है माँग तथा पूर्ति की शक्तियाँ संतुलन कीमत को किस प्रकार निर्धारित करती है ?
Ans. संतुलन मूल्य और माँग तथा पूर्ति की शक्तियाँ:
संतुलन मूल्य:
- वह मूल्य जहाँ किसी वस्तु या सेवा की मांग और आपूर्ति बराबर होती है।
- इस मूल्य पर, बाजार में न तो अधिशेष होता है और न ही कमी होती है।
मांग और पूर्ति की शक्तियाँ:
- मांग:
- उपभोक्ताओं की वस्तु या सेवा के लिए इच्छा।
- मूल्य में वृद्धि से मांग में कमी आती है और मूल्य में कमी से मांग में वृद्धि आती है।
- पूर्ति:
- उत्पादकों द्वारा वस्तु या सेवा की आपूर्ति।
- मूल्य में वृद्धि से आपूर्ति में वृद्धि आती है और मूल्य में कमी से आपूर्ति में कमी आती है।
संतुलन मूल्य का निर्धारण:
- मांग और आपूर्ति वक्रों का प्रतिच्छेदन:
- जब मांग वक्र और आपूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो वह बिंदु संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा को दर्शाता है।
- संतुलन मूल्य पर, बाजार में न तो अधिशेष होता है और न ही कमी होती है।
प्रश्न 19. मांग के आवश्यक तत्वों को लिखिए ।
Ans. माँग के आवश्यक तत्व:
1. इच्छा:
- उपभोक्ता वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की इच्छा रखता है।
- यह इच्छा उसकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित होती है।
2. क्रय शक्ति:
- उपभोक्ता के पास वस्तु या सेवा को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए।
- यह उसकी आय और अन्य आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है।
3. मूल्य:
- वस्तु या सेवा का मूल्य माँग को प्रभावित करता है।
- मूल्य में वृद्धि से माँग में कमी आती है और मूल्य में कमी से माँग में वृद्धि आती है।
4. उपभोक्ता की प्राथमिकताएं:
- उपभोक्ता की प्राथमिकताएं माँग को प्रभावित करती हैं।
- उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं।
5. संबंधित वस्तुओं की कीमतें:
- संबंधित वस्तुओं की कीमतें माँग को प्रभावित करती हैं।
- यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता उसके विकल्प की मांग कर सकते हैं।
6. अपेक्षाएं:
- भविष्य की कीमतों और आय के बारे में उपभोक्ता की अपेक्षाएं माँग को प्रभावित करती हैं।
- यदि उपभोक्ता को भविष्य में कीमतों में वृद्धि की उम्मीद है, तो वे वर्तमान में अधिक मांग कर सकते हैं।
7. सरकारी नीतियां:
- सरकारी नीतियां माँग को प्रभावित करती हैं।
- कर नीतियां, सब्सिडी, और अन्य नीतियां उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और प्राथमिकताओं को प्रभावित करती हैं।
प्रश्न 20. उदासीनता वकों की विशेषताएं लिखिए ।
Ans. उदासीनता वक्रों की विशेषताएं:
1. ढलान:
- उदासीनता वक्र हमेशा नीचे की ओर झुके होते हैं।
- यह दर्शाता है कि उपभोक्ता एक वस्तु के लिए अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करने को तैयार है।
2. उत्तलता:
- उदासीनता वक्र हमेशा मूल के सापेक्ष उत्तल होते हैं।
- यह दर्शाता है कि उपभोक्ता एक वस्तु के लिए अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करने की इच्छा कम हो जाती है।
3. एक दूसरे को नहीं काटते:
- दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते।
- यदि वे एक दूसरे को काटते हैं, तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता एक ही संतुष्टि स्तर पर दो अलग-अलग वस्तुओं के संयोजन को पसंद करेगा, जो असंभव है।
4. उच्च उदासीनता वक्र उच्च संतुष्टि स्तर दर्शाता है:
- जितना ऊंचा उदासीनता वक्र, उतना ही अधिक संतुष्टि स्तर।
- यह दर्शाता है कि उपभोक्ता अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर रहा है।
5. उदासीनता वक्रों का मानचित्र:
- कई उदासीनता वक्रों को एक साथ रखकर, हम उदासीनता वक्रों का मानचित्र बना सकते हैं।
- यह मानचित्र हमें उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और संतुष्टि स्तर के बारे में जानकारी देता है।
6. सीमांत प्रतिस्थापन दर (MRS):
- उदासीनता वक्रों की ढलान सीमांत प्रतिस्थापन दर (MRS) को दर्शाता है।
- MRS यह दर्शाता है कि उपभोक्ता एक वस्तु के लिए अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का कितना त्याग करने को तैयार है।
--
CGBSE Class 12 To 9 Free Study Materials
| CGBSE Class 12 To 9 Free Study Materials | |
| CGBSE Class 12 Study Material | CGBSE Class 11 Study Material |
| CGBSE Class 10 Study Material | CGBSE Class 9 Study Material |







 Profile
Profile Signout
Signout










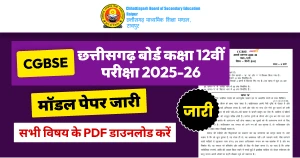

 Quiz
Quiz
 Get latest Exam Updates
Get latest Exam Updates 










