CGBSE Chhattisgarh Board 12th Business Studies Exam 2024 : Important Question with Answers
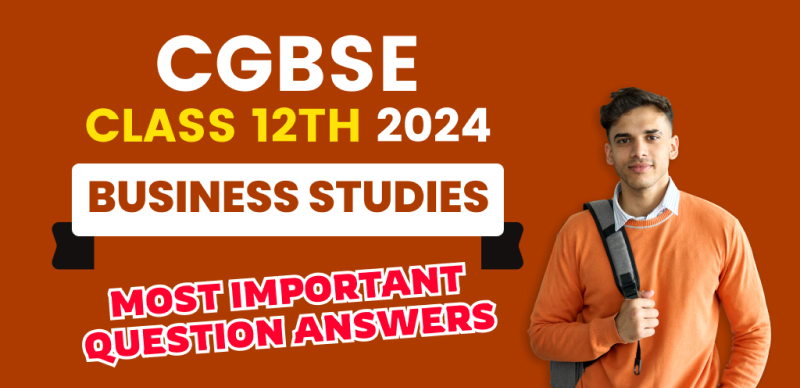
SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की बिजनेस स्टडीज परीक्षा 7 मार्च, 2024 को निर्धारित है। तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि इस आर्टिकल में आपको बोर्ड परीक्षा के लिए वो ही प्रश्न दिए गए है जो बोर्ड पेपर में आने जा रहे है।
इस पोस्ट में छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th परीक्षा 2024 के लिए बिजनेस स्टडीज के महत्वपूर्ण (CG Board 12th Business Studies Important Question 2024) प्रश्न दिये गये है जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
छात्रों को इन (CG Board 12 Business Studies Viral Question 2024) प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी।
अब आपकी परीक्षा में कुछ ही घंटे बचे है I जिससे बिजनेस स्टडीज के पेपर की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते है I
CGBSE Board 12th Exam 2024 Business Studies Important Questions
वस्तुनिष्ठ प्रश्न (1 अंक)
सही विकल्प का चयन कीजिये
1. उदारीकरण के अर्थ है-
(अ)अर्थव्यवस्था के बीच एकात्मकता
(ब) योजनाबद्व विनिवेश नीति
(स) सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी
(द) उपर्युक्त सभी
Ans: (द) उपर्युक्त सभी
2. निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है-
(अ) अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति
(स) देश की संरचना
(ब) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
(द) परिवार का गठन
Ans: (द) परिवार का गठन
3. किसी देश की विदेश नीति प्रभावित करती है वहाँ के -
(अ) सामाजिक वातावरण को
(स) राजनैतिक वातावरण को
(ब) तकनीकी वातावरण को
(द) उपर्युक्त सभी
Ans: (द) उपर्युक्त सभी
4. नई आर्थिक नीति के अंग है-
(अ) उदारीकरण
(स) भूमंडलीकरण
(ब) निजीकरण
(द) उपर्युक्त सभी
Ans: (द) उपर्युक्त सभी
5. प्रबंध का मुख्य एवं सर्वोपरि कार्य है-
(अ) संगठन
(स) नियोजन
(ब) नियंत्रण
(द) निर्णय
Ans: (स) नियोजन
| CGBSE Class 12 To 9 Free Study Materials | |
| CGBSE Class 12 Study Material | CGBSE Class 11 Study Material |
| CGBSE Class 10 Study Material | CGBSE Class 9 Study Materia |
6. नियोजन होता है-
(अ) भूतकाल के लिए
(स) भविष्य के लिये
(ब) वर्तमान के लिए
(द) इनमें से कोई नहीं
Ans: (स) भविष्य के लिये
7. नियोजन का लक्षण है-
(अ) बौद्धिक क्रिया
(स) सर्वश्रेठ विकल्पों के चयन
(ब) लक्ष्यों के निर्धारण
(द) उपर्युक्त सभी
Ans: (द) उपर्युक्त सभी
8. भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है-
(a) वरिष्ठ कर्मचारियों की
(b) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की
(c) भावी कर्मचारियों की
(d) विशिष्ट कर्मचारियों की ।
Ans: (c) भावी कर्मचारियों की
9. चयन का श्रेष्ठतम विरूप आधारित होता है
(a) मुख्य परीक्षा पर
(b) कार्यविधि पर
(c) विश्लेषण के अकलन पर
(d) नीतियों पर
Ans: (b) कार्यविधि पर
10. अंगूरीलता है-
(a) औपचारिक संप्रेषण
(b) संप्रेषण में बाधा
(c) पार्श्वीय संप्रेषण
(d) अनौपचारिक संप्रेषण
Ans: (d) अनौपचारिक संप्रेषण
11. नियंत्रण का लक्षण नहीं है -
(a) सकारात्मक
(b) सुधारात्मक
(c) व्यापकता
(d) अधिकारों का हनन
Ans: (a) सकारात्मक
12. निम्न का योजना से संबंध नहीं है-
(a) बजट
(b) कार्यक्रम
(c) कार्यविधि
(d) अभिप्रेरणा
Ans: (d) अभिप्रेरणा
13. एक अच्छे ब्राण्ड की विशेषता नहीं है :
(a) सरल उच्चारण
(b) स्मरणीय
(c) आकर्षक
(d) खर्चीला
Ans: (d) खर्चीला
14. विक्रय का उद्देश्य नहीं होता है।
(a) ग्राहक संतुष्टि
(b) लागत में कमी
(c) आत्म संतुष्टि
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans: (a) ग्राहक संतुष्टि
15. विपणन मिश्रण एक समूह है-
(a) विपणन साधनों का
(b) विक्रय साधनों का
(c) क्रय साधनों का
(d) निर्माण साधनों का
Ans: (a) विपणन साधनों का
16. किसी विशेष विपणनकर्ता द्वारा बाजार में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों की कुल संख्या कहलाती है:
(a) उत्पाद
(b) उत्पाद की किस्म
(c) उत्पाद मिश्रण
(d) उत्पादन प्रणाली
Ans: (c) उत्पाद मिश्रण
17. निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है?
(a) अभिप्रेरणा
(b) संप्रेषण
(c) हस्तांतरण
(d) पर्यवेक्ष
Ans: (c) हस्तांतरण
18. पद- भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है?
(a) सांकेतिक बाधा
(b) सांगठनिक बाधा
(c) विधिक बाधा
(d) मनोवैज्ञानिक बाधा
Ans: (a) सांकेतिक बाधा
19. नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित / प्रवर्तक सॉफ्टवेयर कंपनी है -
(a) विप्रो
(b) इंफोसिस
(c) सत्यम
(d) एच.सी.एल.
Ans: (b) इंफोसिस
20. निम्न में से क्या भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है-
(a) स्थानांतरण
(b) पदोन्नति
(c) समायोजन
(d) श्रम-संघ
Ans: (d) श्रम-संघ
लघुउत्तरीय प्रश्न (3 अंक)
Q1 - प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना जाता है?
Ans: प्रबन्ध एक बहु-आयामी अवधारणा है-प्रबन्ध एक बहुरूपीय या बहु-आयामी अवधारणा है। यह निम्न प्रकार से स्पष्ट होती है-
(1) कार्य का प्रबन्ध- सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। प्रबन्ध समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना, योजनाएँ बनाना, बजट बनाना, दायित्व निश्चित करना एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना आदि विभिन्न कार्य करता है। प्रबन्ध इन कार्यों को प्राप्य उद्देश्यों में परिवर्तित कर देता है तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित करता है।
(2) लोगों का प्रबन्ध- संगठन में लोगों से कार्य करवाने का कार्य भी प्रबन्ध करता है। यह लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर एवं उनकी कमजोरी को अप्रासंगिक बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कराता है।
(3) परिचालन का प्रबन्ध- प्रत्येक संगठन में एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल को उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत माल में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित करती है। यह कार्य के प्रबन्ध एवं लोगों के प्रबन्ध दोनों से जुड़ी होती है।
Q2 - प्रबंधन के कोई तीन सहायक कार्यों का वर्णन कीजिए
Ans: प्रबंधन के तीन सहायक कार्य:
-
संचार: प्रभावी संचार प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जानकारी का आदान-प्रदान, विचारों का प्रसार, और कर्मचारियों को प्रेरित करना शामिल है। संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि लिखित, मौखिक, और दृश्य।
-
निर्णय लेना: प्रबंधकों को नियमित रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इन निर्णयों में छोटी-छोटी बातें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि किस कर्मचारी को किस कार्य पर लगाना है, या बड़ी बातें, जैसे कि कंपनी की रणनीति क्या होनी चाहिए। प्रभावी निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों को सभी relevant जानकारी का विश्लेषण करना होगा और सबसे अच्छा विकल्प चुनना होगा।
-
समस्या समाधान: प्रबंधकों को नियमित रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें रचनात्मक और नवाचारी होना होगा। समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेटा विश्लेषण, और परीक्षण और त्रुटि।
Q3 - पीटर एफ ड्रकर द्वारा परिभाषित प्रबंध की परिभाषा लिखिए।
Ans: ड्रकर प्रबंध को "संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से निर्देशित करना" मानते हैं। उनकी परिभाषा में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैं:
1. उद्देश्य-केंद्रित: प्रबंध का मुख्य उद्देश्य संस्थान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
2. लोगों पर ध्यान: प्रबंध लोगों के कार्यों को व्यवस्थित करने और उन्हें प्रेरित करने पर केंद्रित है।
3. प्रभावशीलता: प्रबंध का लक्ष्य कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करना है।
4. व्यवस्था: प्रबंध एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करने पर केंद्रित है।
Q4 - उदारीकरण से आप क्या समझते हैं?
Ans: "सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है।" 1991 से पूर्व भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, मूल्य नियंत्रण, आयात लाइसेंस आदि अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। ये सभी प्रतिबंध भारतीय उद्योगों के विकास में बाधा डाल रहे थे। इसलिए 1991 में इनमें से अवांछित नियंत्रणों को हटाने का निश्चय किया गया।
Q5 - व्यावसायिक वातावरण का क्या तात्पर्य है?
Ans: 'व्यावसायिक वातावरण' शब्द उन सभी लोगों, संगठनों और अन्य ताकतों के कुल योग को इंगित करता है जो उद्योग की शक्ति से बाहर हैं लेकिन जो इसके उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। एक अनाम लेखक के अनुसार- "ब्रह्मांड की तरह, इसमें से उस उपसमुच्चय को अलग रखें जो सिस्टम का वर्णन करता है और बाकी पर्यावरण है"। इसलिए, किसी उद्यम के बाहर काम करने वाली वित्तीय, सांस्कृतिक, सरकारी, तकनीकी और विभिन्न ताकतें उसके पर्यावरण का हिस्सा हैं। व्यक्तिगत ग्राहक या सामना करने वाले उद्यमों के साथ-साथ प्रबंधन, ग्राहक समूह, विरोधियों, मीडिया, अदालतें और किसी उद्यम के बाहर काम करने वाले अन्य प्रतिष्ठान इसके वातावरण को शामिल करते हैं।
Q6 - सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक लिखिए | (कोई तीन)
Ans: सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक:
-
व्यक्ति: सामाजिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक व्यक्ति है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार और सामाजिक संबंधों के माध्यम से सामाजिक वातावरण को प्रभावित करते हैं।
-
समूह: समूह दो या दो से अधिक लोगों का संग्रह है जो साझा लक्ष्यों, मूल्यों और व्यवहारों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समूह सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को स्थापित करते हैं।
-
संस्थाएं: संस्थाएं सामाजिक जीवन के स्थापित और संगठित रूप हैं जो सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। परिवार, स्कूल, सरकार, धार्मिक संगठन और व्यवसाय कुछ प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं।
Q7 - नवीन आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषतायें लिखिए। (कोई तीन)
Ans: नवीन आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषताएं (तीन):
- उदारीकरण: यह नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। इसमें सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया, और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां बनाईं।
- निजीकरण: सरकार ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया, जिसके फलस्वरूप इन उद्योगों में कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई।
- वैश्वीकरण: सरकार ने व्यापार और निवेश के लिए वैश्विक बाजारों को खोल दिया, जिसके फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई।
Q8 - कर्मचारियों का स्थानांतरण क्यों किया जाता है?
Ans: कर्मचारियों के स्थानांतरण के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:
1. कौशल मिलान: कंपनी विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के कौशल और अनुभव का मिलान करने के लिए स्थानांतरण का उपयोग कर सकती है।
2. पदों को भरना: रिक्त पदों को भरने के लिए कंपनी कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकती है, खासकर जब उन पदों पर योग्य उम्मीदवारों की कमी हो।
3. कार्यभार वितरण: कंपनी कार्यभार को समान रूप से वितरित करने और किसी भी विभाग में अत्यधिक काम का बोझ कम करने के लिए स्थानांतरण का उपयोग कर सकती है।
4. प्रशिक्षण और विकास: कर्मचारियों को विभिन्न कौशल और अनुभव प्रदान करने के लिए कंपनी उन्हें विभिन्न विभागों में स्थानांतरित कर सकती है।
5. प्रदर्शन सुधार: अगर कोई कर्मचारी किसी विभाग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो कंपनी उसे दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर सकती है।
6. अनुशासनात्मक कार्रवाई: अगर कोई कर्मचारी अनुशासनहीनता या अन्य गलत कार्य करता है, तो कंपनी उसे दंडात्मक कार्रवाई के रूप में स्थानांतरित कर सकती है।
Q9 - भर्ती के बाह्य स्त्रोत की सीमाएँ लिखिय (कोई 3)
Ans: भर्ती के बाहरी स्रोत की सीमाएँ:-
उच्च व्यय- बाहर से उम्मीदवारों की भर्ती की प्रक्रिया में रिक्तियों के लिए विज्ञापन, स्क्रीनिंग और चयन के रूप में काफी खर्च शामिल है।
समय लेने वाली- बाहरी भर्ती में आंतरिक भर्ती की तुलना में अधिक समय लगता है क्योंकि उद्यम को रिक्तियों के बारे में प्रचार करना होता है, या अन्यथा स्रोतों से संपर्क करना होता है और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी होती है।
निश्चितता का अभाव - बाहर से आने वाले संभावित उम्मीदवार उद्यम के लिए अच्छे हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विज्ञापन और अन्य कदमों के बाद भी उद्यम उपयुक्त आवेदकों को आकर्षित करने में सक्षम होगा।
Q10 - मानव संसाधन की आवश्यकता किन कारणों से होती है?
Ans: मानव संसाधन की आवश्यकता अनेक कारणों से होती है, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:
1. कार्य निष्पादन: किसी भी संगठन या संस्था में कार्य निष्पादन के लिए मानव संसाधन अत्यंत आवश्यक है। मशीनों और तकनीक के युग में भी, मानव श्रम और कौशल के बिना कार्य पूर्ण नहीं हो सकते हैं।
2. रचनात्मकता और नवीनता: मानव संसाधन में रचनात्मकता और नवीनता की क्षमता होती है, जो किसी भी संगठन के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है।
3. निर्णय लेने और समस्या समाधान: मानव संसाधन में निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है, जो किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है।
4. नेतृत्व और प्रेरणा: मानव संसाधन में नेतृत्व और प्रेरणा की क्षमता होती है, जो संगठन के अन्य सदस्यों को प्रेरित और मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
5. सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता: मानव संसाधन में सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, जो टीम वर्क, सहयोग और संचार को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
6. ज्ञान और कौशल: मानव संसाधन में ज्ञान और कौशल होता है, जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
7. अनुकूलन और परिवर्तन: मानव संसाधन में अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता होती है, जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार संगठन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
8. नैतिकता और मूल्य: मानव संसाधन में नैतिकता और मूल्यों का ज्ञान होता है, जो संगठन के लिए महत्वपूर्ण है।
Q11 - प्रशिक्षण एवं विकास में कोई तीन अंतर स्पष्ट कीजिए।
Ans: प्रशिक्षण तथा विकास में अन्तर-
1. अर्थ- प्रशिक्षण का अर्थ कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाना है, जबकि विकास का अर्थ कर्मचारियों को सभी कार्यों में निपुण बनाना है।
2. सीखने का क्षेत्र- प्रशिक्षण में सीखने का क्षेत्र कम है, जबकि विकास में सीखने का क्षेत्र अधिक होता है।
3. आवश्यकता- प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रायः श्रमिक वर्ग एवं पर्यवेक्षीय वर्ग के लिए अधिक होती है, जबकि विकास की आवश्यकता प्रबन्धकीय वर्ग के लिए अधिक होती है।
4. केन्द्रित- प्रशिक्षण कार्य-केन्द्रित है, जबकि विकास व्यक्ति-केन्द्रित है।
5. प्रकृति- प्रशिक्षण की प्रकृति व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि करने की होती है, जबकि विकास की प्रकृति सैद्धान्तिक ज्ञान में वृद्धि करने की होती है।
6. विधियाँ- प्रशिक्षण की मुख्य विधियाँ कार्य पर प्रशिक्षण, नव-सीखुआ प्रशिक्षण तथा संयुक्त प्रशिक्षण हैं, जबकि विकास की मुख्य विधियाँ पद-बदली, पाठ्यक्रम, सम्मेलन व गोष्ठियाँ आदि हैं।
7. उद्देश्य- प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक निपुणता से कार्य करने योग्य बनाना है, जबकि विकास का उद्देश्य कर्मचारियों को वर्तमान कार्य के साथ-साथ भावी कार्यों व समस्याओं से कुशलतापूर्वक निपटने योग्य बनाना है।
Q12 - एक आदर्श वित्तीय योजना के किन्हीं तीन बिंदुओं को समझाइए ।
Ans: एक आदर्श वित्तीय योजना के तीन महत्वपूर्ण बिंदु:
-
वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें: सबसे पहले, अपनी दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इसमें घर खरीदना, सेवानिवृत्ति योजना, बच्चों की शिक्षा, यात्रा, आदि शामिल हो सकते हैं। लक्ष्यों को बनाना महत्वपूर्ण है।
-
बजट बनाएं और उसका पालन करें: अपनी आय और खर्चों का रिकॉर्ड रखें और एक बजट बनाएं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। बजट में सभी आवश्यक खर्चों को शामिल करें, जैसे कि आवास, भोजन, परिवहन, ऋण चुकाना, आदि। बजट का पालन करने के लिए, अपने खर्चों पर नज़र रखें और अनावश्यक खर्चों को कम करें।
-
निवेश करें: अपने लक्ष्यों को जल्दी से प्राप्त करने के लिए, अपनी बचत का एक हिस्सा निवेश करें। विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर, ऋण पत्र, आदि के बारे में जानें और अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों के आधार पर सही विकल्प चुनें।
Q13 - वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
Ans: 1. लाभ में वृद्धि: किसी संगठन को आमतौर पर भारी मुनाफा कमाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ लॉन्च किया जाता है, यही कारण है कि लाभ अधिकतम करना वित्तीय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यवसायों को लंबे और छोटे व्यवसाय में इष्टतम पैदावार मिलनी चाहिए।
2. धन वृद्धि: व्यवसायों को शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। हालाँकि, शेयरधारक कोई और नहीं बल्कि संगठन के वास्तविक मालिक हैं। चूँकि धन अधिकतम करना वित्तीय प्रबंधन का सर्वोच्च उद्देश्य है, इसलिए लाभांश और भुगतान नीति तय की जानी चाहिए।
वित्त कार्यकारी को कंपनी की स्थिति में सुधार करते हुए ग्राहकों को खुश रखने के लिए अधिकतम लाभांश वितरित करना चाहिए। यदि कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है, तो कंपनी की संपत्ति अधिकतम होने के साथ बाजार मूल्य भी अधिक होगा।
3. तरलता रखरखाव: उचित वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से, संगठन के नेता व्यवसाय में नियमित तरलता आपूर्ति को ट्रैक कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन का एक प्रमुख उद्देश्य प्रबंधकों को धन के सभी बहिर्प्रवाह और प्रवाह पर गहरी नजर रखने में मदद करना है ताकि नकदी अतिप्रवाह और कम प्रवाह के जोखिम को कम किया जा सके।
यदि स्वस्थ नकदी प्रवाह है, तो इसका मतलब जीविका और व्यावसायिक सफलता की संभावना में वृद्धि है। यह अनिश्चित स्थितियों, समय पर भुगतान, नकद छूट और नियमित देरी को समय पर संसाधित करने में उचित रूप से निपटने में मदद करता है।
4. वित्तीय आवश्यकताओं का सटीक अनुमान: वित्तीय प्रबंधन का एक मुख्य उद्देश्य संगठन की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं की भविष्यवाणी करने में वित्तीय प्रबंधकों की सहायता करना है। इसमें व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी, कंपनी की निश्चित पूंजी और बहुत कुछ के संदर्भ में अनुमान शामिल हैं। इस अनुमान के अभाव में निश्चित रूप से वित्त की कमी होगी।
इस तरह के अनुमान को लागू करने के लिए, वित्त प्रबंधक विभिन्न कारकों जैसे प्रौद्योगिकी, कर्मचारियों की संख्या, कानूनी आवश्यकताएं, संचालन के पैमाने और बहुत कुछ पर विचार करता है।
5. वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग: एक उचित वित्त प्रबंधन मंच के साथ, व्यवसाय वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए, वित्तीय प्रबंधक विभिन्न उपकरणों का लाभ उठा सकता है, जिसमें बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन, प्राप्य प्रबंधन, कुशल नीतियां और बहुत कुछ शामिल हैं।
ये उपकरण एक ही बार में संसाधनों की बर्बादी को कम करने के साथ-साथ बहुत सारा खर्च बचाने में मदद करते हैं।
Q14 - अल्प पूंजीकरण के तीन लक्षणों को लिखिए।
Ans: अल्प पूंजीकरण के तीन लक्षण:
- अस्थिरता: अल्प पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में अत्यधिक अस्थिरता देखी जाती है। छोटी खरीद या बिक्री भी शेयर की कीमत को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है।
- कम तरलता: अल्प पूंजीकरण वाले शेयरों में कम तरलता होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें खरीदना और बेचना मुश्किल हो सकता है।
- सूचना की कमी: अल्प पूंजीकरण वाली कंपनियों के पास बड़ी कंपनियों की तुलना में कम जानकारी उपलब्ध होती है। इससे निवेशकों के लिए कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करना और निवेश का निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है।
Q15 - अति पूंजीकरण के तीन लक्षणों को लिखिए।
Ans: अति पूंजीकरण के तीन लक्षण:
-
कम क्षमता उपयोग: जब किसी कंपनी के पास अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक पूंजी होती है, तो वह अपनी सभी पूंजी का उपयोग नहीं कर पाती है। इसका परिणाम कम क्षमता उपयोग होता है, जिससे कंपनी के लाभ में कमी आती है।
-
अनिश्चितता: अति पूंजीकरण कंपनी को भविष्य की अनिश्चितता के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। यदि बाजार में मांग में कमी आती है, तो कंपनी अपनी पूंजी का उपयोग करने में असमर्थ हो सकती है, जिससे उसे नुकसान हो सकता है।
-
ऋण का बोझ: अति पूंजीकरण के लिए अक्सर कंपनी को ऋण लेना पड़ता है। ऋण का बोझ कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और उसे दिवालियापन के जोखिम में डाल सकता है।
Q16 - ट्रेजरी बिल क्या है?
Ans: ट्रेजरी बिल भारत सरकार या किसी भी देश के केंद्रीय प्राधिकरण के अल्पकालिक (एक वर्ष तक) उधार उपकरण हैं जो निवेशकों को अपने बाजार जोखिम को कम करते हुए अपने अल्पकालिक अधिशेष धन को पार्क करने में सक्षम बनाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नियमित अंतराल पर इनकी नीलामी की जाती है और अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है।
बिल बाज़ार भारत में मुद्रा बाज़ार का एक उप-बाज़ार है। बिल दो प्रकार के होते हैं- ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक बिल। जबकि ट्रेजरी बिल या टी-बिल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं; वाणिज्यिक बिल वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं।'
टी-बिल का अन्य बिलों की तुलना में लाभ होता है जैसे कि उनके साथ शून्य जोखिम भार जुड़ा होता है। वे सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और सॉवरेन कागजात में शून्य जोखिम होता है, उच्च तरलता क्योंकि 91 दिन और 36 दिन अल्पकालिक परिपक्वता हैं।
Q17 - एक अच्छे ब्राण्ड में कौन-कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए। (कोई 3)
Ans: एक व्यापारिक नाम अच्छा या बुरा हो सकता है, वह विक्रय में वृद्धि या रुकावट कर सकता है। एक अच्छे ब्रांड में निम्न विशेषताएं होती है।
2. याद करने में सरल हो - नाम याद करने योग्य हो या याद करने में सरल हो। वह छोटा हो -छोटा व्यापारिक नाम उच्चारण और याद करने में सरल होता है। वह बड़े आकार से कम जगह में लिखा जा सकता है। जैसे टाटा, बिन्नी, सर्फ, डेट आदि।
Q18 - विपणन का महत्व लिखिए। (कोई 3)
Ans: विपणन का महत्व:
-
ग्राहकों को आकर्षित करना: विपणन ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञापन, प्रचार, और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके, व्यवसाय ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
-
बिक्री बढ़ाना: विपणन ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित करके बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। प्रभावी विपणन रणनीतियां ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, उन्हें खरीदने के लाभों को समझाती हैं, और उन्हें खरीदारी करने के लिए प्रेरित करती हैं।
-
ब्रांड प्रतिष्ठा बनाना: विपणन ब्रांड प्रतिष्ठा बनाने और उसे मजबूत करने में मदद करता है। विज्ञापन, प्रचार, और अन्य मार्केटिंग गतिविधियों का उपयोग करके, व्यवसाय अपनी ब्रांड पहचान और छवि को स्थापित कर सकते हैं, ग्राहकों का विश्वास और वफादारी प्राप्त कर सकते हैं, और प्रतिस्पर्धा से अलग खड़े हो सकते हैं।
Q19 - ब्राण्डिंग और ट्रेडमार्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। (कोई 4)
Ans:
| पैरामीटर | ब्राण्डिंग | ट्रेडमार्क |
| परिभाषा | किसी कंपनी की प्रतिष्ठा और छवि का प्रतिनिधित्व करता है | कानूनी तौर पर किसी ब्रांड के अद्वितीय पहलुओं की सुरक्षा करता है |
| उद्देश्य | कंपनी और उसके उत्पादों/सेवाओं की पहचान करता है | प्रतिस्पर्धियों को समान पहचान का उपयोग करने से रोकता है |
| दायरा | इसमें पहचान, छवि, व्यक्तित्व आदि जैसे विभिन्न तत्व शामिल हैं। | ब्रांड नाम, लोगो, पैकेजिंग इत्यादि जैसे विशिष्ट पहलू। |
| कानूनी सुरक्षा | कानून द्वारा स्वचालित रूप से संरक्षित नहीं है | अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है |
| पंजीकरण | पंजीकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन अनुशंसित है | उपयुक्त प्राधिकारी के साथ पंजीकरण की आवश्यकता है |
| दंड | अनधिकृत उपयोग के लिए कोई विशेष दंड नहीं | अनधिकृत उपयोग और उल्लंघन के लिए गंभीर दंड |
| कवरेज | किसी कंपनी के बारे में समग्र सार्वजनिक धारणा का प्रतिनिधित्व करता है | किसी ब्रांड के विशिष्ट पहलुओं को दुरुपयोग से बचाता है |
Q20 - उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए | (कोई 4)
Ans: उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाले 4 महत्वपूर्ण तत्व:
1. ग्राहक की आवश्यकताएं:
- ग्राहकों की बदलती जरूरतें और प्राथमिकताएं उत्पाद मिश्र को प्रभावित करती हैं।
- कंपनियों को ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने वाले उत्पादों की पेशकश करने की आवश्यकता होती है।
- बाजार अनुसंधान, ग्राहक सर्वेक्षण और फोकस समूह ग्राहकों की जरूरतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं।
2. प्रतिस्पर्धा:
- प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों और सेवाओं का प्रभाव उत्पाद मिश्र पर पड़ता है।
- कंपनियों को प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग दिखने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नवीन उत्पादों को विकसित करने की आवश्यकता होती है।
- प्रतिस्पर्धी विश्लेषण कंपनियों को प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को समझने और अपनी रणनीति बनाने में मदद करता है।
3. तकनीकी प्रगति:
- नई तकनीकों का आगमन उत्पाद मिश्र को बदल सकता है।
- कंपनियों को नई तकनीकों को अपनाने और ग्राहकों को बेहतर उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता होती है।
- अनुसंधान एवं विकास (R&D) कंपनियों को नवीन उत्पादों को विकसित करने में मदद करता है।
4. कंपनी की क्षमताएं:
- कंपनी की उत्पादन क्षमता, वित्तीय संसाधन और मानव संसाधन उत्पाद मिश्र को प्रभावित करते हैं।
- कंपनियों को अपनी क्षमताओं के अनुसार उत्पादों का चयन और विकास करने की आवश्यकता होती है।
- रणनीतिक योजना कंपनियों को अपनी क्षमताओं का आकलन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में मदद करती है।
लघुउत्तरीय प्रश्न (4 अंक)
Q1 - सोपान श्रृंखला एवं समतल संपर्क सिद्धांत को समझाइए ।
Ans: 'सोपान श्रृंखला' एवं 'समतल सम्पर्क सिद्धान्त'- किसी भी संगठन में उच्चतम पद से निम्नतम पद तक की औपचारिक अधिकार रेखा को 'सोपान श्रृंखला' कहते हैं। फेयोल के मतानुसार संगठन में सोपान श्रृंखला के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए। उनके इस सिद्धान्त के अनुसार संगठन में अधिकार एवं सम्पर्क की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए तथा उसी के अनुसार प्रबन्धक एवं अधीनस्थ होने चाहिए।
फेयोल का मत था कि औपचारिक सम्प्रेषण में सामान्यतः सोपान श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई आकस्मिक स्थिति है तो समतल सम्पर्क के द्वारा सम्पर्क साधा जा सकता है। यह सम्पर्क स्थापित करने का छोटा मार्ग है। इसका प्रावधान इसलिए किया गया है कि सम्प्रेषण में देरी नहीं हो। व्यवहार में कम्पनी में कोई श्रमिक सीधा मुख्य कार्यकारी से सम्पर्क नहीं कर सकता है, केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही एक श्रमिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।'
Q2 - आदेश की एकता का सिद्धांत प्रबंध के लिए किस प्रकार उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए |
Ans: 'आदेश की एकता' का सिद्धान्त यह बतलाता है कि किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश लेने चाहिए एवं उसे उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। क्योंकि यदि इस सिद्धान्त का उल्लंघन होता है तो इससे अधिकार प्रभावहीन हो जाते हैं। यदि एक से अधिक उच्चाधिकारियों से एक ही समय पर आदेश मिलेंगे तो कर्मचारी भ्रम में पड़ जायेंगे और यह निश्चित नहीं कर पायेंगे कि पहले किसका कार्य करें? साथ ही उसे अपने उत्तरदायित्व से बचने के भी अवसर मिल जायेंगे। अतः भ्रम से बचने के लिए एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार यह सिद्धान्त प्रबन्ध में विरोधाभासी आदेशों को दूर करने में सहायता करता है।
Q3 - आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में कोई चार अंतर स्पष्ट कीजिए।
Ans: आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में चार अंतर:
-
प्रकृति: आदेश एक निश्चित कार्य को करने के लिए दिया जाता है। यह कर्मचारियों को बताता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। निर्देश, दूसरी ओर, अधिक व्यापक और लचीला होता है। यह कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और रणनीति प्रदान करता है।
-
अधिकार: आदेश अधिकारपूर्ण होते हैं और इनका पालन करना कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होता है। निर्देश, दूसरी ओर, अधिक सलाहकार होते हैं और कर्मचारियों को उन्हें अपनाने की स्वतंत्रता होती है।
-
जिम्मेदारी: आदेश का पालन न करने पर कर्मचारियों को दंडित किया जा सकता है। निर्देशों का पालन न करने पर कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जाता है।
-
लक्ष्य: आदेश का उद्देश्य एक निश्चित कार्य को पूरा करना होता है। निर्देश का उद्देश्य कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना होता है।
Q4 - वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों की व्याख्या कीजिए। (कोई 4)
Ans: वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें:
-
कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन: इस तकनीक का उद्देश्य प्रत्येक कार्य को करने का सबसे कुशल और प्रभावी तरीका ढूंढना है। इसमें समय और गति अध्ययन, थकान अध्ययन, और उपकरणों और सामग्री का विश्लेषण शामिल है।
-
कार्य का मानकीकरण: इस तकनीक का उद्देश्य प्रत्येक कार्य के लिए एक मानक प्रक्रिया स्थापित करना है, जिसमें आवश्यक समय, गति, उपकरण और सामग्री शामिल हैं। यह कार्य में सुसंगतता और दक्षता सुनिश्चित करता है।
-
कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण: इस तकनीक का उद्देश्य प्रत्येक कार्य के लिए सबसे उपयुक्त कर्मचारियों का चयन करना और उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह कार्य में कुशलता और उत्पादकता में सुधार करता है।
-
विभेदात्मक वेतन प्रणाली: इस तकनीक का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर भुगतान करना है। यह कर्मचारियों को अधिक उत्पादक होने के लिए प्रेरित करता है।
Q5 - वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध श्रमिकों द्वारा क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए।
Ans: वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे अधिक विरोध श्रमिकों द्वारा किया गया, जिसके निम्न कारण हैं-
1. कार्य में वृद्धि - वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाना आवश्यक हो गया, जिससे श्रमिकों पर कार्य का बोझ बढ़ गया। कार्य का बोझ बढ़ जाने से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने से श्रमिकों ने वैज्ञानिक प्रबंध का भारी विरोध किया।
2. कठोर नियंत्रण - वैज्ञानिक प्रबंध के अन्तर्गत आठ नेता वाले संगठन को अपनाने से श्रमिकों पर एक साथ अनेक लोगों का नियंत्रण रहता है, जिसे श्रमिक पसंद नहीं करते हैं।
3. बेकारी का भय - वैज्ञानिक प्रबंध में मशीनों का कार्य बढ़ जाने से श्रमिकों में बेकारी का भय बना रहता है, अतः वे इसका विरोध करते हैं।
4. श्रमिकों का शोषण - वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य अधिक होने से उत्पादन में वृद्धि जिस मात्रा में होती है, उस मात्रा में श्रमिकों की मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती है।
Q6 - भर्ती एवं चयन में अन्तर स्पष्ट लिखिए। (कोई 4)
Ans:
भर्ती और चयन के बीच अंतर
| क्र.सं. | भर्ती | चयन |
| 1 | नौकरी की भूमिका के लिए आवेदकों को सक्रिय रूप से खोजने और नियुक्त करने की प्रक्रिया को भर्ती के रूप में जाना जाता है। | शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से उपयुक्त आवेदकों को चुनने की प्रक्रिया को चयन के रूप में जाना जाता है। |
| 2 | यह उम्मीदवार समूह को बढ़ावा देने वाली एक गतिविधि है। | यह तब तक उम्मीदवार पूल को कम करने की एक गतिविधि है जब तक हमें आदर्श उम्मीदवार नहीं मिल जाता। |
| 3 | यह उम्मीदवारों को रिक्त स्थान के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। | यह प्रक्रिया एचआर को उपयुक्त आवेदकों के साथ आगे बढ़ने और शेष को अस्वीकार करने की अनुमति देती है। |
| 4 | भर्ती में, हम नौकरी की भूमिका का विज्ञापन करते हैं और उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। | चयन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अंततः उम्मीदवार को विशिष्ट कार्य भूमिका के लिए नियुक्त करते हैं। |
| 5 | यह नियुक्ति प्रक्रिया की दिशा में पहला कदम है। | यह नियुक्ति प्रक्रिया की दिशा में दूसरा कदम है। |
| 6 | यह प्रक्रिया किफायती है. | यह प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से महंगी है। |
| 7 | भर्ती प्रक्रिया में कोई संविदात्मक संबंध नहीं है. | चयन में संगठन और कर्मचारी के बीच एक संविदात्मक संबंध शामिल होता है। |
Q7 - शिक्षण तथा प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट लिखिए। (कोई 4)
Ans: शिक्षण तथा प्रशिक्षण में अंतर:
-
उद्देश्य: शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान, समझ और कौशल का विकास करना है, जबकि प्रशिक्षण का उद्देश्य विशिष्ट कार्यों को करने के लिए योग्यता प्राप्त करना है।
-
दायरा: शिक्षण का दायरा व्यापक होता है, जिसमें कला, विज्ञान, इतिहास, साहित्य, आदि जैसे विषय शामिल होते हैं। प्रशिक्षण का दायरा सीमित होता है, और यह विशिष्ट कार्यों या व्यवसायों पर केंद्रित होता है।
-
विधि: शिक्षण में विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि व्याख्यान, प्रदर्शन, समूह चर्चा, आदि। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से व्यावहारिक शिक्षण, अनुकरण, और अभ्यास पर ध्यान दिया जाता है।
-
परिणाम: शिक्षण का परिणाम ज्ञान, समझ, और कौशल में वृद्धि होता है, जो व्यक्ति को जीवन में सफल होने में मदद करता है। प्रशिक्षण का परिणाम विशिष्ट कार्यों को करने की क्षमता में वृद्धि होता है, जो व्यक्ति को कार्यस्थल में अधिक कुशल बनाता है।
Q8 - एक कारखाने में कार्यालयीन कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया को लिखिए। (कोई 4)
Ans: कारखाने में कार्यालयीन कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया (4 चरणों में):
1. आवेदन और प्रारंभिक जांच:
- रिक्त पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है।
- आवेदकों को अपना बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव पत्र आदि जमा करना होता है।
- प्रारंभिक जांच में, योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर आवेदकों को छांटा जाता है।
2. लिखित परीक्षा:
- योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है।
- परीक्षा में सामान्य ज्ञान, भाषा, तर्कशक्ति, गणित और कंप्यूटर ज्ञान जैसे विषयों के प्रश्न शामिल होते हैं।
- न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना जाता है।
3. साक्षात्कार:
- लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।
- साक्षात्कार में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, संचार कौशल, प्रेरणा, और कार्य के प्रति समर्पण का मूल्यांकन किया जाता है।
- साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों को चयनित माना जाता है।
4. चिकित्सा परीक्षण:
- चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए फिट हैं।
- चिकित्सा परीक्षण में सफल होने के बाद, उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है।
Q9 - एक अच्छी भर्ती नीति में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? (कोई 4)
Ans: एक अच्छी भर्ती नीति में 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं:
- न्यायपूर्ण और पारदर्शी:
- भर्ती प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों के लिए समान और निष्पक्ष होनी चाहिए।
- सभी चरणों में पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसमें चयन मानदंड, परीक्षा पैटर्न, और साक्षात्कार प्रक्रिया शामिल हैं।
- योग्यता आधारित:
- योग्यता और अनुभव को ही चयन का आधार बनाया जाना चाहिए।
- सिफारिश, जाति, धर्म, या लिंग जैसे पक्षपातपूर्ण कारकों को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।
- कौशल और क्षमता पर ध्यान:
- उम्मीदवारों के पास आवश्यक कौशल, ज्ञान, और क्षमता होनी चाहिए।
- केवल शैक्षिक योग्यता पर ध्यान देने की बजाय, व्यावहारिक अनुभव और क्षमताओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
- प्रभावी और कुशल:
- भर्ती प्रक्रिया त्वरित और कुशल होनी चाहिए।
- अनावश्यक देरी और जटिलताओं से बचना चाहिए।
Q10 - "नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर है।" स्पष्ट कीजिए।
Ans: नियोजन एवं नियंत्रण: एक दूसरे पर निर्भर
नियोजन और नियंत्रण, प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एक दूसरे पर गहराई से निर्भर हैं। नियोजन, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया है। नियंत्रण, योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखने और गतिविधियों को लक्ष्य के अनुरूप रखने की प्रक्रिया है।
नियोजन और नियंत्रण के बीच संबंध निम्नलिखित हैं:
1. योजना नियंत्रण का आधार है: नियंत्रण, योजना के आधार पर ही संभव है। यदि कोई योजना नहीं है, तो यह जानना असंभव होगा कि वास्तविक प्रदर्शन अपेक्षित प्रदर्शन से मेल खाता है या नहीं।
2. नियंत्रण योजना की त्रुटियों को उजागर करता है: नियंत्रण प्रक्रिया के दौरान, यदि वास्तविक प्रदर्शन अपेक्षित प्रदर्शन से कम होता है, तो यह योजना में त्रुटियों का संकेत देता है।
3. नियंत्रण योजना में सुधार लाता है: नियंत्रण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त जानकारी का उपयोग योजना में सुधार करने के लिए किया जाता है।
4. योजना नियंत्रण को दिशा प्रदान करती है: योजना, नियंत्रण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करती है। नियंत्रण प्रक्रिया, योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
5. नियंत्रण योजना की सफलता सुनिश्चित करता है: नियंत्रण प्रक्रिया, योजना की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है।
Q11 - नियंत्रण के किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए ।
Ans: नियंत्रण की चार विशेषताएं:
-
उद्देश्यपूर्ण: नियंत्रण का उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। यह योजनाओं के अनुसार कार्य निष्पादन को मापता है और सुधारात्मक कदमों के लिए दिशा-निर्देश देता है।
-
निरंतर प्रक्रिया: नियंत्रण एक निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करती है और आवश्यक होने पर सुधार करती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होती है।
-
बहुआयामी: नियंत्रण विभिन्न पहलुओं जैसे कि वित्तीय, उत्पादन, विपणन, मानव संसाधन आदि को कवर करता है। यह संगठन के सभी स्तरों पर लागू होता है।
-
अग्रगामी: नियंत्रण भविष्यवादी होता है। यह भविष्य में योजनाओं के अनुसार कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करता है। यह भूतकाल की गलतियों से सीखता है और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाता है।
Q12 - एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक गुणों को समझाइए ।
Ans: एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक गुण:
-
स्पष्ट उद्देश्य: नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य स्पष्ट और परिभाषित होना चाहिए। यह लक्ष्य, मानक और अपेक्षित परिणामों को स्पष्ट रूप से बताता है।
-
सटीकता: नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक और विश्वसनीय होनी चाहिए। गलत जानकारी भ्रामक निर्णयों को जन्म दे सकती है।
-
समयबद्धता: नियंत्रण प्रणाली समय पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें। देर से प्राप्त जानकारी बेकार हो सकती है।
-
लचीलापन: नियंत्रण प्रणाली को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। यह विभिन्न प्रकार की जानकारी और डेटा को संभालने में सक्षम होना चाहिए।
-
स्वीकृति: नियंत्रण प्रणाली को सभी हितधारकों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यह सभी के लिए उचित और पारदर्शी होना चाहिए।
-
कम लागत: नियंत्रण प्रणाली को लागू करने और बनाए रखने के लिए लागत प्रभावी होना चाहिए। यह अनावश्यक जटिलता से बचना चाहिए।
-
सुधारात्मक: नियंत्रण प्रणाली को त्रुटियों और कमियों को पहचानने और सुधारने में सक्षम होना चाहिए। यह निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करना चाहिए।
-
सुरक्षा: नियंत्रण प्रणाली डेटा और जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह अनधिकृत पहुंच और उपयोग से बचाना चाहिए।
-
प्रतिक्रिया: नियंत्रण प्रणाली को उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यह प्रणाली को बेहतर बनाने और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है।
-
जिम्मेदारी: नियंत्रण प्रणाली में सभी कार्यों और निर्णयों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
Q13 - नियंत्रण के किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Ans: नियंत्रण की चार विशेषताएं:
-
उद्देश्यपूर्णता: नियंत्रण का उद्देश्य योजनाओं को पूरा करना और लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। यह एक निश्चित लक्ष्य के आधार पर कार्य करता है और योजना से विचलन को मापता है।
-
मापनीयता: नियंत्रण प्रक्रिया में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को मापने योग्य होना चाहिए। यदि पहलुओं को मापा नहीं जा सकता है, तो नियंत्रण प्रभावी नहीं होगा।
-
समयबद्धता: नियंत्रण समय पर होना चाहिए। यदि नियंत्रण समय पर नहीं किया जाता है, तो यह उपयोगी नहीं होगा।
-
लचीलापन: नियंत्रण प्रणाली लचीली होनी चाहिए ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसे बदला जा सके।
Q14 - सेबी के किन्ही चार कार्यों का वर्णन कीजिए।
Ans: सेबी के चार महत्वपूर्ण कार्य:
-
नियमन: सेबी प्रतिभूति बाजार के लिए नियमों और विनियमों का निर्माण, कार्यान्वयन और प्रवर्तन करता है। इसमें कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए दिशानिर्देश, लेनदेन के लिए नियम, और व्यापारिक व्यवहारों के लिए आचार संहिता शामिल हैं।
-
बाजार की निगरानी: सेबी प्रतिभूति बाजार की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल तरीके से काम कर रहा है। इसमें व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी करना, धोखाधड़ी और हेरफेर का पता लगाना और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना शामिल है।
-
निवेशक शिक्षा: सेबी निवेशकों को शिक्षित करने और जागरूक करने का काम करता है ताकि वे informed decisions ले सकें। इसमें निवेशकों को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, निवेश के जोखिमों और बाजार में लेनदेन करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल है।
-
शिकायत निवारण: सेबी निवेशकों द्वारा दायर शिकायतों का निवारण करता है। इसमें मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से विवादों को हल करना और उचित मामलों में कंपनियों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।
Q15 - पूंजी बाजार की प्रमुख चार वैध संस्थाओं अथवा उपकरणों का वर्णन कीजिए।
Ans: पूंजी बाजार की चार प्रमुख वैध संस्थाएं/उपकरण:
-
स्टॉक एक्सचेंज: यह पूंजी बाजार का मुख्य केंद्र है जहां कंपनियां अपने शेयरों को खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार के लिए लाती हैं। भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) शामिल हैं।
-
डिपॉजिटरी: डिपॉजिटरी शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने और लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्था है। भारत में दो प्रमुख डिपॉजिटरी हैं: सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)।
-
क्लीयरिंग हाउस: यह स्टॉक एक्सचेंज में किए गए लेनदेन को निपटाने के लिए एक संस्था है। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लेनदेन को सत्यापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को उनके दायित्वों को पूरा करना होगा। भारत में प्रमुख क्लियरिंग हाउस नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSCCL) है।
-
डीमैट खाता: यह एक इलेक्ट्रॉनिक खाता है जिसमें शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है। यह शेयरों के भौतिक प्रमाणपत्रों की आवश्यकता को समाप्त करता है और लेनदेन को आसान और सुविधाजनक बनाता है।
Q16 - एक अच्छे वित्तीय नियोजन के चार लक्षणों का वर्णन कीजिए
Ans: एक अच्छे वित्तीय नियोजन के चार लक्षण:
-
स्पष्ट लक्ष्य: एक अच्छे वित्तीय योजना में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित होते हैं, जैसे कि सेवानिवृत्ति के लिए बचत, घर खरीदना, या बच्चों की शिक्षा। लक्ष्य SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) होने चाहिए।
-
यथार्थवादी बजट: एक यथार्थवादी बजट आपके सभी खर्चों को ध्यान में रखता है और आपकी आय के अनुसार धन आवंटित करता है। इसमें बचत और ऋण चुकौती के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।
-
जोखिम प्रबंधन: एक अच्छे वित्तीय योजना में जोखिम प्रबंधन शामिल होता है। इसमें बीमा, विविधता, और आपातकालीन निधि के माध्यम से अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयारी शामिल है।
-
नियमित समीक्षा: आपकी वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा और अपडेट किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने लक्ष्यों पर नज़र रखें और अपनी योजना को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाएं।
Q17 - वित्तीय नियोजन की चार सीमाएं लिखिए।
Ans: वित्तीय नियोजन की चार सीमाएं:
-
अनिश्चितता: भविष्य की घटनाओं की अनिश्चितता वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करती है। अप्रत्याशित घटनाएं, जैसे कि नौकरी छूटना, स्वास्थ्य खराब होना या बाजार में उतार-चढ़ाव, योजनाओं को बाधित कर सकते हैं।
-
व्यक्तिगत भावनाएं: लोगों की जोखिम लेने की क्षमता और खर्च करने की आदतें भिन्न होती हैं। भावनाएं, जैसे कि डर या लालच, वित्तीय निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं और योजनाओं को पटरी से उतार सकती हैं।
-
बाजार में उतार-चढ़ाव: शेयर बाजार, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। निवेश पर रिटर्न अनिश्चित होता है और योजनाओं को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
-
जटिलता: वित्तीय योजनाओं में कई कारकों और विकल्पों पर विचार करना होता है। यह प्रक्रिया जटिल और भ्रमित करने वाली हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास वित्तीय ज्ञान का अभाव है।
Q18 - जिला उपभोक्ता मंच के अधिकारों का समझाइये । (कोई 4)
Ans: जिला उपभोक्ता मंच के अधिकारों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा और हित सुनिश्चित करना होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्नलिखित हैं:
-
सूचना का अधिकार (Right to Information): जिला उपभोक्ता मंच के अधिकारी उपभोक्ताओं को उनके उत्पादों और सेवाओं के बारे में सही और पूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार देते हैं।
-
शिकायत करने का अधिकार (Right to Redressal): जिला उपभोक्ता मंच उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान करने का अधिकार देते हैं।
-
सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety): जिला उपभोक्ता मंच उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पादों और सेवाओं के अधिकार की गारंटी प्रदान करने का काम करते हैं।
-
जागरूकता का अधिकार (Right to Education): जिला उपभोक्ता मंच उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के संबंध में जागरूकता और शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं।
Q19 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
Ans: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय संघ की एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
-
उपभोक्ता संरक्षा परिषद्: अधिनियम द्वारा उपभोक्ता संरक्षा परिषद् की स्थापना की गई है, जिसका कार्यक्षेत्र उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, शिकायतों का समाधान, और उनके अधिकारों की संरक्षा है।
-
उपभोक्ता के अधिकार: अधिनियम ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे उत्पादों और सेवाओं की सुरक्षा, मानक और गुणवत्ता की उम्मीद, और उचित मूल्य और पूर्ति।
-
उपभोक्ता शिकायत और संरक्षा: अधिनियम द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के लिए संरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
-
उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण: अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की संरक्षा के लिए कई प्रावधान और माध्यम प्रदान करता है।
-
उपभोक्ता संरक्षा क्षेत्र: यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षा क्षेत्र की रचना करने के लिए भी उत्तरदायी है, जिसमें उपभोक्ताओं के लिए अधिक और सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध हों।
-
उपभोक्ता शिकायत दर्जन: अधिनियम ने उपभोक्ताओं के लिए एक उपभोक्ता शिकायत दर्जन की स्थापना की है, जिसके माध्यम से उन्हें उनकी समस्याओं की शिकायत करने का माध्यम प्राप्त होता है।
-
उपभोक्ता संरक्षा अधिकारी: अधिनियम द्वारा उपभोक्ता संरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है।
Q20 - उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज कर सकता है?
Ans: उपभोक्ता न्यायालय एक महत्वपूर्ण संस्था है जो उपभोक्ताओं के हित में उच्च स्तरीय न्याय प्रदान करती है। यह एक अदालत होती है जो उपभोक्ताओं की सुनवाई करती है और उनकी शिकायतों को सुलझाती है। यहाँ बताया जा रहा है कि उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज कर सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है।
किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ता संगठन के व्यक्ति को उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का अधिकार होता है। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार की शिकायतों की सूची दी जा रही है जिनके लिए उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है:
- दुकानदार या सेवा प्रदाता के खिलाफ उपभोक्ता द्वारा शिकायत।
- दोषी उत्पाद के खिलाफ उपभोक्ता द्वारा शिकायत।
- नकली उत्पाद के खिलाफ उपभोक्ता द्वारा शिकायत।
- सेवा में दोष के खिलाफ उपभोक्ता द्वारा शिकायत।
- शिकायत करने वाले उपभोक्ता के हित में जिम्मेदारी की अवहेलना करने के खिलाफ उपभोक्ता द्वारा शिकायत।
शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता को उपभोक्ता न्यायालय के प्राधिकृत कार्यालय में एक आवेदन पत्र देना होता है। इस पत्र में शिकायत का विवरण, उपभोक्ता का नाम, पता, और संपर्क जानकारी दी जाती है। यदि शिकायत विचारणीय मानी जाती है, तो उपभोक्ता न्यायालय उस पर सुनवाई करता है और न्याय देता है।
र्दीघघउत्तरीय प्रश्न (5 अंक)
Q1 - "प्रबंध तथा प्रशासन एक-दूसरे के पर्यायवाची है।" स्पष्ट करते हुए इन दोनों में अंतर लिखिए।
Ans:
Q2 - प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध की विशेषताओं को समझाइए ?
Ans: प्रबंध: परिभाषा और विशेषताएं
प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना, आयोजन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण शामिल होता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो संगठन के सभी स्तरों पर लागू होती है।
प्रबंध की विशेषताएं:
1. उद्देश्यपूर्ण: प्रबंध का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। सभी गतिविधियां इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती हैं।
2. सार्वभौमिक: प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है, चाहे वह व्यवसायिक, सामाजिक, या राजनीतिक हो।
3. निरंतर प्रक्रिया: प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है जो योजना, आयोजन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण के चरणों में चलती रहती है।
4. समूह क्रिया: प्रबंध एक समूह क्रिया है जिसमें विभिन्न लोगों का योगदान होता है।
5. सामाजिक प्रक्रिया: प्रबंध लोगों के बीच संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
6. नेतृत्व: प्रबंध में नेतृत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेता संगठन के सदस्यों को प्रेरित करता है और उन्हें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है।
7. निर्णय लेना: प्रबंध में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, जैसे कि योजना बनाना, संसाधनों का आवंटन करना, और समस्याओं का समाधान करना।
8. संचार: प्रबंध में प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। संगठन के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने और समझने में सक्षम होना चाहिए।
9. परिवर्तनशील: प्रबंध परिवर्तनशील होता है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होता रहता है।
10. नैतिकता: प्रबंध में नैतिकता महत्वपूर्ण है। संगठन के सदस्यों को नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए।
Q3 - प्रबंध के किन्ही पांच उद्देश्यों को लिखिए ।
Ans: प्रबंध के पांच उद्देश्य:
-
उद्देश्यों की प्राप्ति: प्रबंध का मुख्य उद्देश्य संगठन के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
-
कार्यक्षमता में वृद्धि: प्रबंध कार्य को सरल बनाने, अनावश्यक गतिविधियों को कम करने, और समय और संसाधनों का सदुपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
-
कर्मचारियों की प्रेरणा: प्रबंध कर्मचारियों को प्रेरित करने, उनकी क्षमताओं का विकास करने, और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है।
-
समन्वय और सहयोग: प्रबंध विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
-
नवाचार और परिवर्तन: प्रबंध संगठन में नवाचार और परिवर्तन को प्रोत्साहित करने, नए विचारों को विकसित करने और उन्हें लागू करने में मदद करता है।
Q4 - प्रबंध के प्रमुख कार्यों को समझाइए? (कोई 5)
Ans: प्रबंध के प्रमुख कार्य:
-
नियोजन (Planning): यह प्रबंध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें संगठन के लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति और योजना बनाना शामिल है।
-
संगठन (Organizing): इसमें संगठन के संसाधनों (मानव, भौतिक, और वित्तीय) को व्यवस्थित करना शामिल है ताकि लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।
-
निर्देशन (Directing): इसमें कर्मचारियों को प्रेरित करना, मार्गदर्शन करना, और उनकी देखरेख करना शामिल है ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें।
-
नियंत्रण (Controlling): इसमें योजनाओं और लक्ष्यों की प्रगति को मॉनिटर करना और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है।
-
संचार (Communication): इसमें संगठन के सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से जानकारी का आदान-प्रदान करना शामिल है।
Q5 - “समन्वय प्रबंध का सार है। क्या आप सहमत हैं?” कारण स्पष्ट कीजिए |
Ans: हाँ, समन्वय वास्तव में प्रबंधन का सार है। समन्वय से हमारा तात्पर्य एक पथ से है जिसके माध्यम से समूह कार्य जुड़े हुए हैं। यह वह शक्ति है जो, प्रबंधन के अन्य सभी कार्यों को एक-दूसरे से बाँधती है। यह सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाता है।
निम्नलिखित बिंदु प्रबंधन में समन्वय के महत्त्व को उजागर करते हैं-
- सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है।
- कार्यवाही में एकता लाता है।
- निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
- सर्वव्यापी कार्य है।
- सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है।
- समन्वय सोचा-समझा कार्य है।
Q6 - 'प्रबंध के स्तरों ' से क्या अभिप्राय है? प्रबंध के विभिन्न स्तरों के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
Ans: प्रबंध के स्तर
प्रबंध के स्तर संगठन में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों को संदर्भित करते हैं, जो विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को विभाजित करते हैं। प्रबंधन के विभिन्न स्तरों का उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है। प्रबंधन के तीन मुख्य स्तर हैं:
1. उच्च स्तरीय प्रबंधन:
यह संगठन का शीर्ष स्तर है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आदि शामिल हैं। इस स्तर के प्रबंधक रणनीतिक योजना, नीति निर्माण, और संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
2. मध्य स्तरीय प्रबंधन:
यह प्रबंधन का मध्य स्तर है, जिसमें विभागीय प्रमुख, महाप्रबंधक, आदि शामिल हैं। इस स्तर के प्रबंधक उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा निर्धारित रणनीति और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे विभागीय कार्यों, बजट, और कर्मचारियों का प्रबंधन करते हैं।
3. निम्न स्तरीय प्रबंधन:
यह प्रबंधन का सबसे निचला स्तर है, जिसमें पर्यवेक्षक, फोरमैन, आदि शामिल हैं। इस स्तर के प्रबंधक दैनिक कार्यों, कर्मचारियों की देखरेख, और उत्पादन या सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
प्रबंध के विभिन्न स्तरों के कार्य:
उच्च स्तरीय प्रबंधन:
- संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करना
- रणनीतिक योजना बनाना
- नीति निर्माण
- संसाधनों का आवंटन
- संगठनात्मक संस्कृति को विकसित करना
- बाहरी वातावरण के साथ संबंध बनाना
मध्य स्तरीय प्रबंधन:
- उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा निर्धारित रणनीति और नीतियों को लागू करना
- विभागीय कार्यों का प्रबंधन
- बजट का प्रबंधन
- कर्मचारियों का प्रबंधन
- प्रदर्शन मूल्यांकन
- समस्या निवारण
निम्न स्तरीय प्रबंधन:
- दैनिक कार्यों की योजना बनाना और उनका निर्देशन करना
- कर्मचारियों की देखरेख
- उत्पादन या सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन
- कर्मचारियों को प्रेरित करना और उनका मनोबल बनाए रखना
Q7 - "एक सफल उद्यमी अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करता है"। स्पष्ट कीजिए |
Ans: एक सफल उद्यमी वही होता है जो अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक सफल प्रबन्धक होना अति आवश्यक है क्योंकि एक प्रबन्धक ही प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में सन्तुलन स्थापित कर सकता है।
प्रबन्ध के महत्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट कर सकते हैं –
(i) प्रबन्ध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है – संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबन्ध की आवश्यकता होती है। प्रबन्ध का कार्य संगठन के सम्पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों को समान दिशा देना है।
(ii) प्रबन्ध क्षमता में वृद्धि करता है – प्रबन्ध का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं के श्रेष्ठ नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियन्त्रण के माध्यम से लागत को कम करना एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। अतः इससे संगठन की क्षमता में वृद्धि होती है।
(iii) प्रबन्ध गतिशील संगठन का निर्माण करता है – प्रत्येक संगठन का प्रबन्ध निरन्तर बदल रहे पर्यावरण के अन्र्तगत करना होता है। सामान्यत: यह देखा जाता है कि किसी भी संगठन में कार्यरत लोग अपरिचित, कम सुरक्षित एवं अधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण की ओर जाना पसन्द नहीं करते हैं। लेकिन संगठन की प्रतियोगी श्रेष्ठता को बनाये रखने के लिए प्रबन्ध लोगों को इन परिवर्तनों को अपनाने में सहायता करता है।
(iv) प्रबन्ध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है – प्रबन्धक अपनी टीम को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता हैं एवं उसका नेतृत्व करता है जिससे कि प्रत्येक सदस्य संगठन के सामूहिक उद्देश्यों में योगदान देते हुए व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करता है।
(v) प्रबन्ध समाज के विकास में सहायक होता है – संगठन के विभिन्न घटकों के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में प्रबन्ध संगठन के विकास में सहायक होता है तथा इसके माध्यम से ही समाज के विकास में सहायक होता है। यह श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने, रोजगार के अवसर पैदा करने, नयी तकनीकों को अपनाने, बुद्धि एवं विकास के रास्ते पर चलने में सहायक होता है।
Q8 - एक उपक्रम की सफलता में प्रबंध कैसे सहयोगी होता है? स्पष्ट कीजिए।
Ans: प्रबंध की भूमिका:
एक उपक्रम की सफलता में प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो योजना, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और प्रेरणा के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है।
प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो एक उपक्रम की सफलता में योगदान करते हैं:
1. योजना:
प्रबंधन का पहला कदम योजना बनाना है। इसमें उद्देश्यों को निर्धारित करना, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ बनाना और कार्यों को आवंटित करना शामिल है। एक अच्छी योजना उपक्रम को सही दिशा में ले जाने और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करती है।
2. संगठन:
प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू संगठन है। इसमें विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को विभिन्न व्यक्तियों और समूहों को सौंपना शामिल है। एक प्रभावी संगठनात्मक संरचना उपक्रम के सभी सदस्यों को एकजुट होकर काम करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है।
3. निर्देशन:
प्रबंधन का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू निर्देशन है। इसमें कर्मचारियों को उनके कार्यों को करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना शामिल है। एक अच्छा प्रबंधक कर्मचारियों को उनके काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें उचित प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करता है।
4. नियंत्रण:
प्रबंधन का चौथा महत्वपूर्ण पहलू नियंत्रण है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी कार्य योजना के अनुसार किए जा रहे हैं और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। नियंत्रण प्रक्रिया में प्रदर्शन की निगरानी करना, समस्याओं की पहचान करना और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करना शामिल है।
5. प्रेरणा:
प्रबंधन का पांचवां महत्वपूर्ण पहलू प्रेरणा है। इसमें कर्मचारियों को उनके काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। एक अच्छा प्रबंधक कर्मचारियों को उनके काम में अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है और उन्हें पुरस्कार और मान्यता प्रदान करके उनके काम को स्वीकार करता है।
Q9 - पर्यवक्षक के कार्य लिखिए | (कोई 5)
Ans: पर्यवेक्षक के कार्य:
-
निरीक्षण: पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य कार्यस्थल का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना है कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है।
-
मार्गदर्शन: पर्यवेक्षक कर्मचारियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ताकि वे अपने कार्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सकें।
-
प्रशिक्षण: पर्यवेक्षक कर्मचारियों को नए कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
-
मूल्यांकन: पर्यवेक्षक कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।
-
समस्या समाधान: पर्यवेक्षक कार्यस्थल में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाते हैं।
Q10 - प्रबंध के निर्देशन कार्य के एक तत्व के रूप में पर्यवेक्षण का महत्व लिखिए।
Ans: प्रबंध के निर्देशन कार्य के एक तत्व के रूप में पर्यवेक्षण का महत्व:-
प्रबंधन में निर्देशन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। निर्देशन के कई तत्व हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण तत्व है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का अर्थ है कर्मचारियों के कार्य को देखना और उनका मूल्यांकन करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे योजना के अनुसार काम कर रहे हैं और लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं।
पर्यवेक्षण प्रबंधन के निर्देशन कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:
1. कार्य में सुधार:
- पर्यवेक्षण कर्मचारियों को उनकी गलतियों को सुधारने और कार्य में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है।
- पर्यवेक्षक कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, ताकि वे कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें।
2. उत्पादकता में वृद्धि:
- जब कर्मचारियों को लगता है कि उनका काम देखा जा रहा है, तो वे अधिक प्रेरित होते हैं और अधिक कुशलता से काम करते हैं।
- पर्यवेक्षण कार्य में अनावश्यक देरी और रुकावटों को कम करने में मदद करता है।
3. गुणवत्ता में सुधार:
- पर्यवेक्षण कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है।
- पर्यवेक्षक त्रुटियों और कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद कर सकते हैं।
4. अनुशासन में सुधार:
- पर्यवेक्षण कार्यस्थल में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है।
- पर्यवेक्षक कर्मचारियों को नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
5. कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि:
- जब कर्मचारियों को लगता है कि उनका काम देखा जा रहा है और उनकी सराहना की जा रही है, तो वे अधिक संतुष्ट होते हैं।
- पर्यवेक्षण कर्मचारियों को अपनी समस्याओं और चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
Q11 - अभिप्रेरण की आवश्यकता क्यो होती है? (कोई 5)
Ans: 1. लक्ष्य प्राप्ति के लिए: अभिप्रेरण हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी काम करने और चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है।
2. बेहतर प्रदर्शन के लिए: जब हम प्रेरित होते हैं, तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। हम अधिक ऊर्जावान, उत्साही और रचनात्मक होते हैं।
3. सफलता के लिए: अभिप्रेरण सफलता की कुंजी है। यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करती है।
4. खुशी और संतुष्टि के लिए: जब हम प्रेरित होते हैं, तो हम अपने काम में अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं। यह हमारे जीवन में खुशी और अर्थ लाता है।
5. आत्म-विकास के लिए: अभिप्रेरण हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें नई चीजें सीखने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में मदद करती है।
Q12 - निर्देशन के कार्य लिखिए। (कोई 5)
Ans: निर्देशन के 5 प्रमुख कार्य :
-
आत्म-ज्ञान: निर्देशन का पहला कार्य व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, रुचियों, मूल्यों और व्यक्तित्व के बारे में जागरूक करना है। यह जानकारी उन्हें अपनी शिक्षा, करियर और जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है।
-
समस्या समाधान: निर्देशन व्यक्तियों को अपनी समस्याओं को पहचानने, समझने और उनका समाधान करने में मदद करता है। यह उन्हें विभिन्न समस्या-समाधान रणनीतियाँ सिखाता है और उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास देता है।
-
निर्णय लेना: निर्देशन व्यक्तियों को शिक्षा, करियर, रिश्ते और अन्य महत्वपूर्ण जीवन निर्णय लेने में मदद करता है। यह उन्हें विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने, उनके परिणामों पर विचार करने और उनके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने में सहायता करता है।
-
शैक्षिक योजना: निर्देशन छात्रों को अपनी शैक्षिक क्षमताओं के अनुसार अपनी शिक्षा की योजना बनाने में मदद करता है। यह उन्हें अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम और संस्थान चुनने में सहायता करता है।
-
व्यावसायिक विकास: निर्देशन व्यक्तियों को अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त करियर चुनने में मदद करता है। यह उन्हें आवश्यक कौशल विकसित करने, नौकरी खोजने और कार्यस्थल में सफल होने में सहायता करता है।
Q13 - संप्रेषण प्रक्रिया में निम्न तत्वों का आशय स्पष्ट कीजिए ।
1. प्रेषक 2. माध्यम 3. डिकोडिंग 4. प्रतिपुष्टि 5. कोलाट्रल
Ans: संप्रेषण प्रक्रिया में तत्वों का आशय:
1. प्रेषक:
- संदेश भेजने वाला व्यक्ति या संस्था।
- विचारों, भावनाओं, या सूचनाओं को साझा करने की इच्छा रखता है।
- प्रेषक का ज्ञान, अनुभव, और भाषा का प्रयोग संदेश को प्रभावित करते हैं।
2. माध्यम:
- वह तरीका जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है।
- मौखिक (बोलना), लिखित (पढ़ना), या दृश्य (प्रतीक) माध्यम हो सकते हैं।
- माध्यम का चुनाव संदेश की प्रकृति, प्राप्तकर्ता, और स्थिति पर निर्भर करता है।
3. डिकोडिंग:
- प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की प्रक्रिया।
- प्राप्तकर्ता के ज्ञान, अनुभव, और भाषा का प्रयोग डिकोडिंग को प्रभावित करते हैं।
- डिकोडिंग में अर्थ की व्याख्या और संदेश का विश्लेषण शामिल है।
4. प्रतिपुष्टि:
- प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को संदेश के बारे में प्रतिक्रिया।
- मौखिक या अमौखिक रूप में हो सकती है।
- प्रतिपुष्टि संचार की प्रभावशीलता को मापने में मदद करती है।
5. कोलाट्रल:
- संदेश के साथ भेजी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी।
- तस्वीरें, वीडियो, या दस्तावेज हो सकते हैं।
- कोलाट्रल संदेश को समझने और संवाद को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं।
Q14 - मैसलो के आवश्यकता क्रमबद्धता अभिप्रेरणा सिद्धांत को समझाइए ।
Ans: मैसलो का आवश्यकता क्रमबद्धता अभिप्रेरणा सिद्धांत:-
अब्राहम मैसलो द्वारा 1943 में प्रस्तुत आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत मानव प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि मानव ज़रूरतें एक क्रम में व्यवस्थित होती हैं और एक स्तर की ज़रूरत पूरी होने के बाद ही अगले स्तर की ज़रूरत प्रेरक बनती है।
इस सिद्धांत के अनुसार, मानवीय ज़रूरतों को पांच स्तरों में बांटा गया है:
- शारीरिक ज़रूरतें: ये ज़रूरतें अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं और इनमें भोजन, पानी, हवा, आश्रय, नींद आदि शामिल हैं। जब तक इन ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति अन्य ज़रूरतों के लिए प्रेरित नहीं होता है।
- सुरक्षा ज़रूरतें: इन ज़रूरतों में सुरक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, और स्थिरता शामिल हैं। जब व्यक्ति को भोजन, पानी, और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब वह सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है।
- सामाजिक ज़रूरतें: इन ज़रूरतों में प्यार, स्नेह, दोस्ती, सामाजिक स्वीकृति, और सम्मान शामिल हैं। जब व्यक्ति को सुरक्षा ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब वह सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है।
- सम्मान ज़रूरतें: इन ज़रूरतों में आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास, उपलब्धि, और मान्यता शामिल हैं। जब व्यक्ति को सामाजिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब वह सम्मान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है।
- आत्म-बोध ज़रूरतें: इन ज़रूरतों में व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता, और जीवन में अर्थ खोजने की इच्छा शामिल हैं। जब व्यक्ति को सम्मान ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब वह आत्म-बोध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है।
Q15 - प्रबंधन के निर्देशन कार्य के महत्व की पांच बिंदुओं की व्याख्या कीजिए।
Ans: प्रबंधन के निर्देशन कार्य के महत्व के पांच बिंदु:
-
कार्य को प्रेरित करना: निर्देशन कर्मचारियों को उनके कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए प्रेरित करता है। प्रबंधक कर्मचारियों को उनके कार्यों के महत्व, लक्ष्यों और अपेक्षाओं को समझाकर उन्हें प्रेरित करते हैं।
-
प्रभावी संचार: निर्देशन संगठन में प्रभावी संचार को बढ़ावा देता है। प्रबंधक कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे गलतफहमी और भ्रम कम होता है।
-
कार्य में समन्वय: निर्देशन संगठन में विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के बीच कार्य में समन्वय स्थापित करता है। प्रबंधक यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कर्मचारी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं।
-
कार्यक्षमता में वृद्धि: निर्देशन संगठन की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंधक कर्मचारियों को उनके कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
-
नैतिकता और अनुशासन: निर्देशन संगठन में नैतिकता और अनुशासन को बढ़ावा देता है। प्रबंधक कर्मचारियों को संगठन के नैतिकता और आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
Q16 - निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। (कोई 5)
Ans: निर्देशन के 5 सिद्धांत:
-
व्यक्तिगत भिन्नता: प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और उसकी अपनी क्षमताएं, रुचियां और योग्यताएं होती हैं। निर्देशन व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को समझने और उनका उपयोग करने में मदद करता है।
-
स्वयं की समझ: निर्देशन व्यक्ति को उसकी क्षमताओं, रुचियों, मूल्यों और लक्ष्यों को समझने में मदद करता है। यह आत्म-जागरूकता व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने और जीवन में सफल होने में सक्षम बनाता है।
-
विकासात्मक दृष्टिकोण: निर्देशन व्यक्ति को उसकी विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को जीवन के विभिन्न चरणों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है।
-
निर्णय लेने की प्रक्रिया: निर्देशन व्यक्ति को प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करता है। यह व्यक्ति को विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने और उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है।
-
समस्या समाधान: निर्देशन व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। यह व्यक्ति को समस्याओं की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और उनके लिए प्रभावी समाधान खोजने में सक्षम बनाता है।
Q17 - औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में पांच अंतर लिखिए।
Ans: औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में पांच अंतर:
-
भाषा:
- औपचारिक: मानक भाषा, व्याकरण का पालन, औपचारिक शब्दावली, और शिष्टाचार का प्रयोग।
- अनौपचारिक: बोलचाल की भाषा, व्याकरण में लचीलापन, सरल शब्दावली, और अनौपचारिक शिष्टाचार।
-
शैली:
- औपचारिक: गंभीर, संक्षिप्त, और व्यावसायिक शैली।
- अनौपचारिक: हल्का-फुल्का, विस्तृत, और व्यक्तिगत शैली।
-
संबंध:
- औपचारिक: वरिष्ठ-कनिष्ठ, व्यावसायिक, या अजनबी के बीच।
- अनौपचारिक: मित्रों, परिवार, या करीबी लोगों के बीच।
-
उदाहरण:
- औपचारिक: व्यावसायिक पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, या प्रस्तुति।
- अनौपचारिक: टेक्स्ट संदेश, सोशल मीडिया पोस्ट, या फोन कॉल।
-
माध्यम:
- औपचारिक: पत्र, ईमेल, या प्रस्तुति।
- अनौपचारिक: टेक्स्ट संदेश, फोन कॉल, या आमने-सामने बातचीत।
Q18 - धनात्मक प्रेरणा और ऋणात्मक प्रेरणा में पांच अंतर लिखिए।
Ans: धनात्मक प्रेरणा और ऋणात्मक प्रेरणा में पांच अंतर:
1. भावना:
- धनात्मक प्रेरणा खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास जैसी सकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होती है।
- ऋणात्मक प्रेरणा भय, चिंता और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होती है।
2. लक्ष्य:
- धनात्मक प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति और सफलता पर केंद्रित होती है।
- ऋणात्मक प्रेरणा विफलता से बचने और दंड से दूर रहने पर केंद्रित होती है।
3. दीर्घकालिक प्रभाव:
- धनात्मक प्रेरणा दीर्घकालिक सफलता और आत्म-विकास को बढ़ावा देती है।
- ऋणात्मक प्रेरणा अल्पकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती है और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है।
4. रचनात्मकता:
- धनात्मक प्रेरणा रचनात्मकता, नवीनता और समस्या-समाधान को बढ़ावा देती है।
- ऋणात्मक प्रेरणा डर और चिंता के कारण रचनात्मकता को बाधित कर सकती है।
5. सामाजिक संबंध:
- धनात्मक प्रेरणा सहयोग, टीम वर्क और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देती है।
- ऋणात्मक प्रेरणा प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और नकारात्मक संबंधों को जन्म दे सकती है।
र्दीघघउत्तरीय प्रश्न (6 अंक)
Q1. नियोजन की तकनीक या प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
Ans: नियोजन की तकनीक या प्रक्रिया
नियोजन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में विभाजित है:
1. उद्देश्यों का निर्धारण: सबसे पहले, योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। उद्देश्य विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध (SMART) होने चाहिए।
2. डेटा का संग्रह: योजना बनाने के लिए, संगठन के बारे में जानकारी, जैसे कि उसके संसाधन, क्षमताएं, कमजोरियां, अवसर और खतरे, इकट्ठा करना आवश्यक है।
3. पर्यावरणीय विश्लेषण: योजना बनाते समय, बाहरी वातावरण का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रतियोगी, बाजार की स्थिति, तकनीकी प्रगति, और सरकारी नीतियां शामिल हैं।
4. विकल्पों का मूल्यांकन: विभिन्न विकल्पों पर विचार करना और उनका मूल्यांकन करना आवश्यक है जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
5. योजना का चयन: मूल्यांकन के आधार पर, सबसे उपयुक्त योजना का चयन करना आवश्यक है।
6. कार्यान्वयन: योजना को क्रियान्वित करना, इसे व्यवहार में लाना है।
7. नियंत्रण और मूल्यांकन: योजना को ट्रैक करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है। यदि आवश्यक हो तो योजना में बदलाव किया जा सकता है।
नियोजन की तकनीकें:
- SWOT विश्लेषण: यह तकनीक संगठन की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का विश्लेषण करने में मदद करती है।
- पोर्टफोलियो विश्लेषण: यह तकनीक संगठन के विभिन्न व्यवसायों या उत्पादों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करती है।
- बजट: यह योजना का एक वित्तीय विवरण है जो संगठन के संसाधनों के आवंटन को दर्शाता है।
- समयसीमा: यह योजना के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित करने में मदद करता है।
Q2. कभी-कभी प्रबंध के सर्वोच्च प्रयत्नों के बावजूद भी नियोजन क्यों असफल होता है? स्पष्ट कीजिए।
Ans: नियोजन की असफलता के कारण
प्रबंधन के सर्वोच्च प्रयत्नों के बावजूद भी नियोजन कई कारणों से असफल हो सकता है। यहां कुछ प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला गया है:
1. अपूर्ण जानकारी: योजना बनाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। भविष्य की अनिश्चितता, बाजार में बदलाव, प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियां, और तकनीकी प्रगति जैसी अनिश्चितताओं के कारण योजनाएं अप्रभावी हो सकती हैं।
2. गलत धारणाएँ: योजनाकारों द्वारा बाजार, प्रतिस्पर्धियों, या ग्राहकों के बारे में गलत धारणाएं बनाई जा सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप गलत योजनाएँ बन सकती हैं।
3. अवास्तविक लक्ष्य: योजना में निर्धारित लक्ष्य अवास्तविक या अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका क्रियान्वयन असंभव हो जाता है।
4. अपर्याप्त संसाधन: योजना में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों (जैसे, धन, कर्मचारी, समय) की कमी हो सकती है।
5. खराब क्रियान्वयन: योजना का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है, यदि कर्मचारियों को योजना की जानकारी नहीं है, वे प्रशिक्षित नहीं हैं, या वे प्रेरित नहीं हैं।
6. अप्रत्याशित घटनाएं: प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक अस्थिरता, या आर्थिक मंदी जैसी अप्रत्याशित घटनाएं योजनाओं को बाधित कर सकती हैं।
7. परिवर्तन का अभाव: बदलते बाजार, प्रतिस्पर्धियों, या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को अपडेट नहीं किया जा सकता है।
8. संचार की कमी: योजना के विभिन्न हितधारकों (जैसे, प्रबंधन, कर्मचारी, ग्राहक) के बीच प्रभावी संचार की कमी योजना की सफलता को बाधित कर सकती है।
9. प्रतिक्रिया का अभाव: योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्रगति की निगरानी नहीं की जा सकती है और आवश्यक बदलाव नहीं किए जा सकते हैं।
10. अस्पष्ट जिम्मेदारी: योजना में निर्धारित कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप काम में ढिलाई हो सकती है।
Q3. आदर्श नियोजन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (कोई 6)
Ans: आदर्श नियोजन की 6 विशेषताएं:
- स्पष्ट लक्ष्य: आदर्श नियोजन में, लक्ष्य स्पष्ट और परिभाषित होते हैं। लक्ष्य SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) होने चाहिए।
- कार्य योजना: लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है। योजना में कार्यों का क्रम, समयसीमा, जिम्मेदारियां और संसाधनों का उल्लेख होता है।
- लचीलापन: आदर्श नियोजन में अप्रत्याशित घटनाओं के लिए लचीलापन होता है। योजना में बदलाव करने की व्यवस्था होती है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
- सहभागिता: आदर्श नियोजन में सभी हितधारकों की भागीदारी होती है। योजना बनाने और क्रियान्वित करने में सभी की राय और योगदान महत्वपूर्ण होता है।
- निरंतर मूल्यांकन: आदर्श नियोजन में प्रगति का निरंतर मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के आधार पर योजना में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं।
- संसाधनों का कुशल उपयोग: आदर्श नियोजन में संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। योजना में संसाधनों का आवंटन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
Q4. नीति तथा कार्यविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। (कोई 6)
Ans: नीति और कार्यविधि में अंतर:
-
परिभाषा:
- नीति: नीति मार्गदर्शक सिद्धांतों का समूह है जो किसी संगठन, व्यक्ति या समूह के निर्णयों और कार्यों को निर्देशित करते हैं। नीतियां व्यापक और लचीली होती हैं, और वे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- कार्यविधि: कार्यविधि एक निश्चित क्रम में किए जाने वाले कार्यों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। कार्यविधियां नीतियां को लागू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट चरणों का वर्णन करती हैं।
-
उद्देश्य:
- नीति: नीतियां संगठन के मूल्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करती हैं। वे एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, और वे संगठन के सदस्यों को निर्णय लेने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं।
- कार्यविधि: कार्यविधियां दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। वे यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि कार्य एक सुसंगत और मानकीकृत तरीके से किए जाते हैं, और वे त्रुटियों और भिन्नता को कम करते हैं।
-
लचीलापन:
- नीति: नीतियां लचीली होती हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती हैं। उन्हें समय-समय पर समीक्षा और अपडेट किया जाना चाहिए ताकि वे प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें।
- कार्यविधि: कार्यविधियां आमतौर पर नीतियां की तुलना में अधिक कठोर होती हैं। उन्हें अक्सर विस्तृत रूप से दस्तावेज किया जाता है और उन्हें बदलने के लिए औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
-
स्तर:
- नीति: नीतियां आमतौर पर संगठनात्मक स्तर पर निर्धारित की जाती हैं और सभी सदस्यों पर लागू होती हैं।
- कार्यविधि: कार्यविधियां विशिष्ट विभागों, टीमों या व्यक्तियों के लिए विकसित की जा सकती हैं।
-
उदाहरण:
- नीति: एक कंपनी की नैतिकता नीति कर्मचारियों के लिए व्यवहार के मानकों को परिभाषित कर सकती है।
- कार्यविधि: एक कंपनी की बिक्री प्रक्रिया में संभावनाओं को पहचानने, योग्य बनाने और बंद करने के लिए आवश्यक चरणों का वर्णन किया जा सकता है।
Q5. संगठन से क्या अभिप्राय है? संगठन के महत्व की व्याख्या कीजिए ।
Ans: संगठन: परिभाषा और महत्व
संगठन एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करता है। यह समूह लोगों, विचारों, संसाधनों और प्रक्रियाओं को एक व्यवस्थित तरीके से जोड़ता है ताकि वे एक साथ मिलकर काम कर सकें और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
संगठन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
1. लक्ष्य प्राप्ति: संगठन लोगों को एक साथ लाकर लक्ष्य प्राप्ति को आसान बनाता है। जब लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो वे अकेले काम करने की तुलना में अधिक हासिल कर सकते हैं।
2. संसाधनों का कुशल उपयोग: संगठन संसाधनों का कुशल उपयोग करता है। जब लोग एक साथ काम करते हैं, तो वे संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और उन्हें बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
3. विशेषज्ञता का लाभ: संगठन विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इससे संगठन को विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में मदद मिलती है।
4. निर्णय लेने में सुधार: संगठन में विभिन्न लोगों के विचारों और अनुभवों का उपयोग करके बेहतर निर्णय लिए जाते हैं।
5. प्रेरणा और सहयोग: संगठन लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
6. विकास और नवाचार: संगठन लोगों को सीखने और विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे संगठन में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
7. सामाजिक परिवर्तन: संगठन सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे लोगों को शिक्षित करके, जागरूकता फैलाकर और सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए काम करके सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं।
8. स्थायित्व: संगठन पर्यावरण की रक्षा करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।







 Profile
Profile Signout
Signout












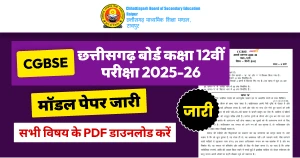

 Quiz
Quiz
 Get latest Exam Updates
Get latest Exam Updates 










